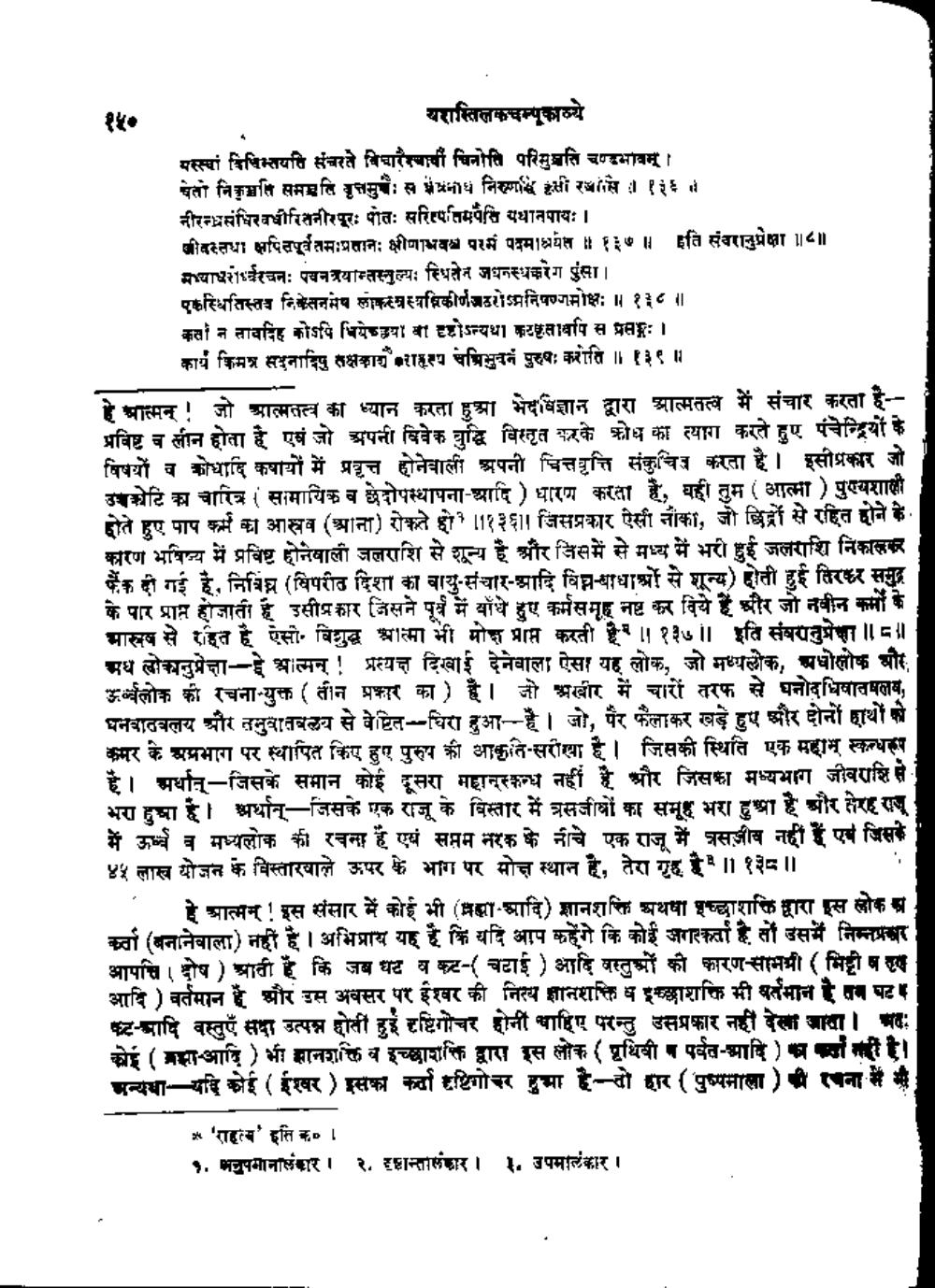________________
१५.
यरास्तिलकपम्पकाव्ये परस्पां विनिम्तयति संचरते विचारचाची चिनोति परिमुवति चण्डभावम् । चेता निकाति समयति वृत्तमु समावं निरुणाय सी खास १३६ नीरन्ध्रसंघिरवधीरितनीरपूरः पोतः सरित्पत्तिमपैति यथानपायः । जीवस्तथा क्षपितपूर्वतमःप्रतानः क्षीणाभव परमं पदमाश्रयत ॥ १६ ॥ इति संवरानुप्रेक्षा ॥८॥ मन्याधरचनः पयनत्रयान्तस्तुल्यः स्थितेन जधनस्थकरेग पुंसा। एकस्थितिस्तत्र निकेतनमेष लोकत्यस्वत्रिकीर्णजठरोऽमनिषग्गमोक्षः ॥ १३८ । का न तावविह कोऽपि थियेच्छया वा दृष्टोऽन्यथा कस्कृतावपि स प्रसः ।
कार्य किमत्र सदनादिपु तक्षकाय राहत्य पत्रिभुवनं पुरुषः करोति ॥ १३९ ॥ हे आत्मन् ! जो आत्मतत्व का ध्यान करता हुआ भेदविज्ञान द्वारा आत्मतत्व में संचार करता है- प्रविष्ट च लीन होता है एवं जो अपनी विवेक बुद्धि विस्तृत करके क्रोध का त्याग करते हुए पंचेन्द्रियों के . विषयों व कोधादि कषायों में प्रवृत्त होनेवाली अपनी चित्तवृत्ति संकुचित्र करता है। इसीप्रकार जो उचोटि का चारित्र ( सामायिक व छेदोपस्थापना-श्रादि ) धारण करता है, यही तुम ( आत्मा) पुण्यशाली । होते हुए पाप कर्म का आस्तव (आना) रोकते हो। ११३६|| जिसप्रकार ऐसी नौका, जो छिद्रों से रहित होने के कारण भविष्य में प्रविष्ट होनेवाली जलराशि से शून्य है और जिसमें से मध्य में भरी हुई जलराशि निकालकर फैंक दी गई है. निर्विघ्न (विपरीत दिशा का वायु-संचार-आदि विघ्न-बाधाओं से शून्य) होती हुई तिरकर समुद्र के पार प्राप्त होजाती है उसीप्रकार जिसने पूर्व में याँधे हुए कर्मसमूह नष्ट कर दिये हैं और जो नवीन कमों के भारष से रहित है ऐसी. विशुद्ध श्रात्मा भी मोक्ष प्राप्त करती है ।। १३७ ।। इति संघयनुप्रेक्षा ।।८।। मध लोक्यनुप्रेक्षा-ई श्रात्मन ! प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला ऐसा यह लोक, जो मध्यलोक, अधोलोक औरः । अवलोक की रचना-युक्त ( तीन प्रकार का) है। जो खीर में चारों तरफ से घनोदधिवावपलब, धनवातबलय और तनुवातबलय से वेष्टित-घिरा हुआ है। जो, पैर फैलाकर खड़े हुए और दोनों हाथों को कमर के अप्रभाग पर स्थापित किए हुए पुरुष की आकृति-सरीया है। जिसकी स्थिति एक महान स्कन्धरूप है। अर्थात्-जिसके समान कोई दूसरा महानस्कन्ध नहीं है और जिसका मध्यभाग जीवराशि से भरा हुआ है। अर्थात्-जिसके एक राजू के विस्तार में त्रसजीवों का समूह भरा हुआ है और तेरह राजू में ऊर्ध्व व मध्यलोक की रचना है एवं सप्तम नरक के नीचे एक राजू में त्रसजीव नहीं है एवं जिसके ४५ लाख योजन के विस्तारवाने ऊपर के भाग पर मोक्ष स्थान है, तेरा गृह है। ॥ १३८ ।।
आत्मम् ! इस संसार में कोई भी (ब्रह्मा-आदि) ज्ञानशक्ति अथषा इच्छाशक्ति द्वारा इस लोकन कर्ता (बनानेवाला) नहीं है। अभिप्राय यह है कि यदि आप कहेंगे कि कोई अगरकर्ता है, तो उसमें निम्नप्रकार आपत्ति दोष ) आती हैं कि जब घट व कट-( चटाई ) आदि वस्तुओं को कारण सामग्री (मिट्टी पहन आदि ) वर्तमान हैं और उस अवसर पर ईश्वर की नित्य ज्ञानशक्ति व इच्छाशक्ति भी वर्तमान सब घट कट-आदि वस्तुएँ सथा उत्पन्न होती हुई दृष्टिगोचर होनी चाहिए परन्तु उसप्रकार नहीं देखा जाता। भदः | कोई ( प्रमा-आदि) भी ज्ञानशक्ति व इच्छाशक्ति द्वारा इस लोक (पृथिवीप पर्वत-आदि ) कामही है। अन्यथा-यदि कोई ( ईश्वर ) इसका कर्ता दृष्टिगोचर हुमा है-तो हार (पुष्पमाला)ी सपना में है।
* 'राहत्य' इसिक। १.भनुपमानालंकार । २. शान्तालंकार। 1. उपमालंकार ।