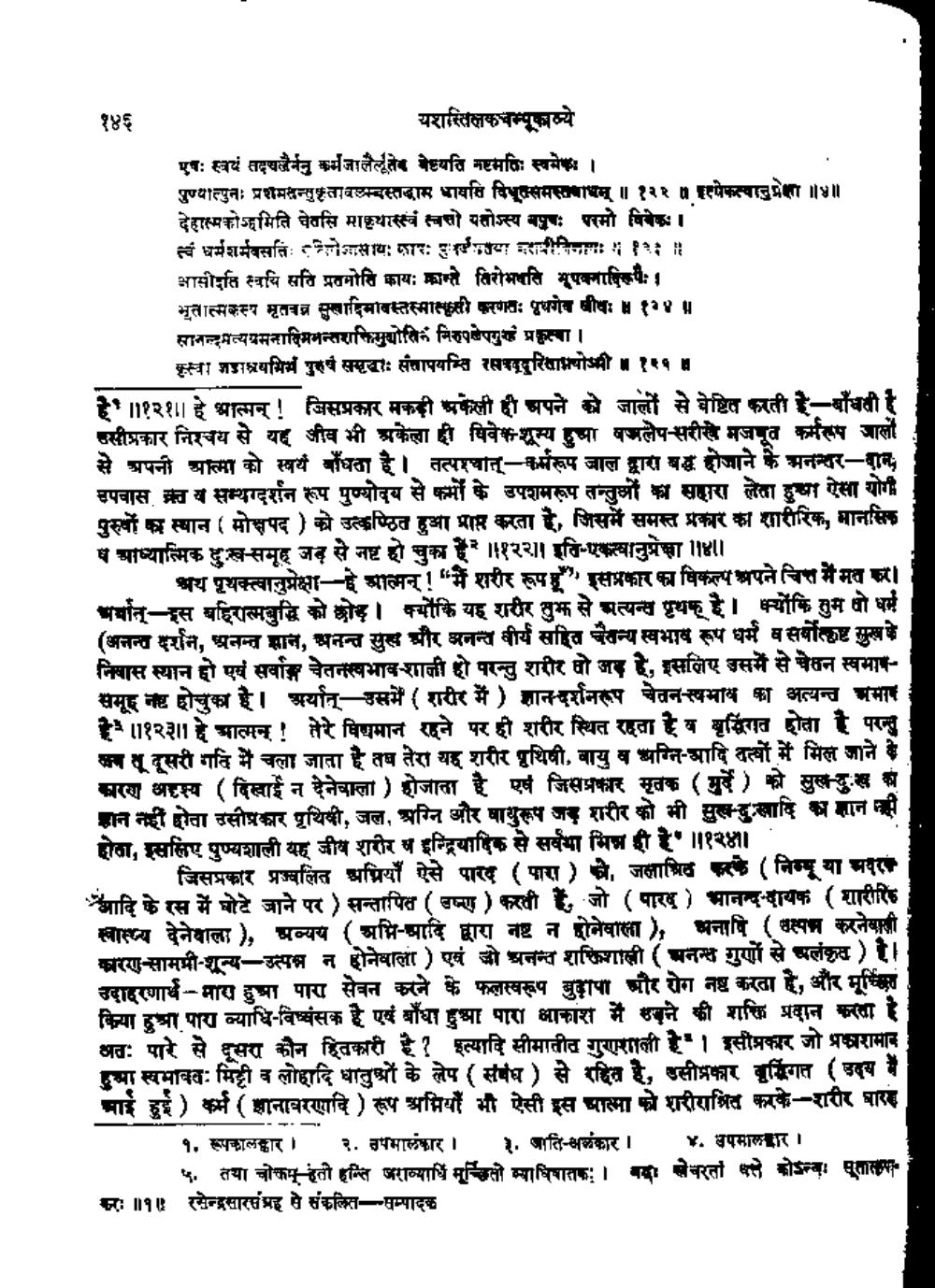________________
१४६
यशस्तिलकचम्पूकाव्ये एष: स्वयं सदशलैननु कर्मजालेलते वेष्टयति मष्टमतिः स्वमेका । पुण्यात्पुनः प्रशमतन्तुक्तावलम्बस्तद्धाम पायसि विभूतसमस्तवायम् ॥ १२१ पेकस्वानुप्रेक्षा ॥४॥ देहास्मकोऽहमिति चेतसि मायास्वं स्वसो यतोऽस्य वपुषः परमो विवेकः । स्वं धर्मशर्मवसतिः किशासाय: मारः जया महानि ११॥ आसीदति स्वयि सति प्रतमोति कायः माते तिरोभवति भूपकमाविकपः । भुतात्मकस्य मृतबन्न सुखादिमावस्तस्मास्कसी करणतः पृथगेव बीयः ॥ १॥ सानन्दमत्ययमनादिममन्सशक्तिमयोति मिरुपलेपगुरू प्रकृत्वा ।
कृत्वा जडानयमिमं पुरुष समृद्धाः संतापयन्ति रसरिताप्रयोऽमी ॥ ११ ॥ है ॥१२१|| हे आत्मन् ! जिसप्रकार मकड़ी अकेली ही अपने को जालों से बेष्टित करती है-बाँधती है। उसीप्रकार निश्चय से यह जीव भी अकेला ही विवेकशून्य हुआ वमलेप-सरीखे मजबूत कर्मस्प जालो से अपनी आत्मा को स्वयं बाँधता है। तत्पश्चात्-कर्मरूप जाल द्वारा बद्ध होजाने के अनन्धर-पान । उपवास त व सम्यग्दर्शन रूप पुण्योदय से कमों के उपशमरूप तन्तुओं का सहारा लेता हुया ऐसा योगी पुरुषों का स्थान ( मोक्षपद ) को उत्कण्ठित हुआ प्राप्त करता है, जिसमें समस्त प्रकार का शारीरिक, मानसिक प आध्यात्मिक दुःख-समूह जद से नष्ट हो चुका है ॥१२२|| इति-एकत्यानुप्रेशा ॥४॥
श्रय पृथक्त्वानुप्रेक्षा हे आत्मन् ! "मैं शरीर रूप हूँ इसप्रकार का विकल्प अपने चित्त में मत कर अर्थात्-इस बहिरात्मबुद्धि को छोड़। क्योंकि यह शरीर तुझ से अत्यन्त पृथक् है। क्योंकि तुम धो धर्म | (अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य सहित चैतन्य स्वभाव रूप धर्म व सर्वोत्कृष्ट मुख के निवास स्थान हो एवं सर्वाङ्ग चेतनस्वभाव-शानी हो परन्तु शरीर वो जड़ है, इसलिए उसमें से पेसन स्वमारसमूह ना होचुका है। अर्यात्-उसमें ( शरीर में ) ज्ञानदर्शनरूप चेतन-स्वभाव का अत्यन्त ममा । है ॥१२शा हे आत्मन् ! तेरे विद्यमान रहने पर ही शरीर स्थित रहता है व वृद्धिंगत होता है परन्तु अन तू दूसरी गति में चला जाता है तब तेरा यह शरीर पृथिवी, वायु व अग्नि-आदि तत्वों में मिल जाने के। कारण अदृश्य ( दिखाई न देनेवाला) होजाता है एवं जिसप्रकार मृतक (मुर्दै) को सुख-दुःख का डान नहीं होता उसीप्रकार पृथिवी, जल, अग्नि और षायुरूप जड़श होता, इसलिए पुण्यशाली यह जीव शरीर ष इन्द्रियादिक से सर्वथा भिन्न हीरे ॥१२॥
जिसप्रकार प्रज्वलित अप्रियाँ ऐसे पारद (पारा)चे, जलाश्रित करके (निम्मू या भवरल आदि के रस में घोटे जाने पर ) सन्तापित ( उष्ण) करती है, जो (पारद ) भानन्द-दायक (शारीरिक स्वास्थ्य देनेवाला), अव्यय (अमि-आदि द्वारा नष्ट न होनेवाला), अनापि (सत्पन्न करनेवाली कारण-सामग्री-शून्य-उत्पन्न न होनेवाला) एवं जो अनन्त शक्तिशाली (अनन्त गुणों से अलंकृत) है। उदाहरणार्थ-मारा हुआ पारा सेवन करने के फलस्वरूप बुढ़ापा और रोग नष्ट करता है, और भूमि ! किया हुआ पारा व्याधि-विध्वंसक है एवं बाँधा हुआ पारा भाकाश में सबने की शक्ति प्रदान करता है। अतः पारे से दूसरा कौन हितकारी है? इत्यादि सीमातीत गुणशाली है। इसीप्रकार जो प्रकाशमान हुमा स्वमाक्यः मिट्टी व लोहादि धातुओं के लेप ( संबंध) से रहित है, उसीप्रकार वृद्धिंगत (उदय में माई हुई ) कर्म (ज्ञानावरादि ) रूप अमियों भी ऐसी इस पात्मा को शरीराश्रित करके-शरीर धारह
१. रूपकालकार। २. तपमालंकार। ३. जाति-मर्मकार । ४. अपमालबार ।
५. तया चोक्का-हतो हन्ति अराव्याधि मूच्छितो म्याधिषातकः। बा खेचरतो पते कोऽन्तः सुतार करः ॥१॥ रमेन्द्रसारसंग्रह से संकलित-सम्पादक