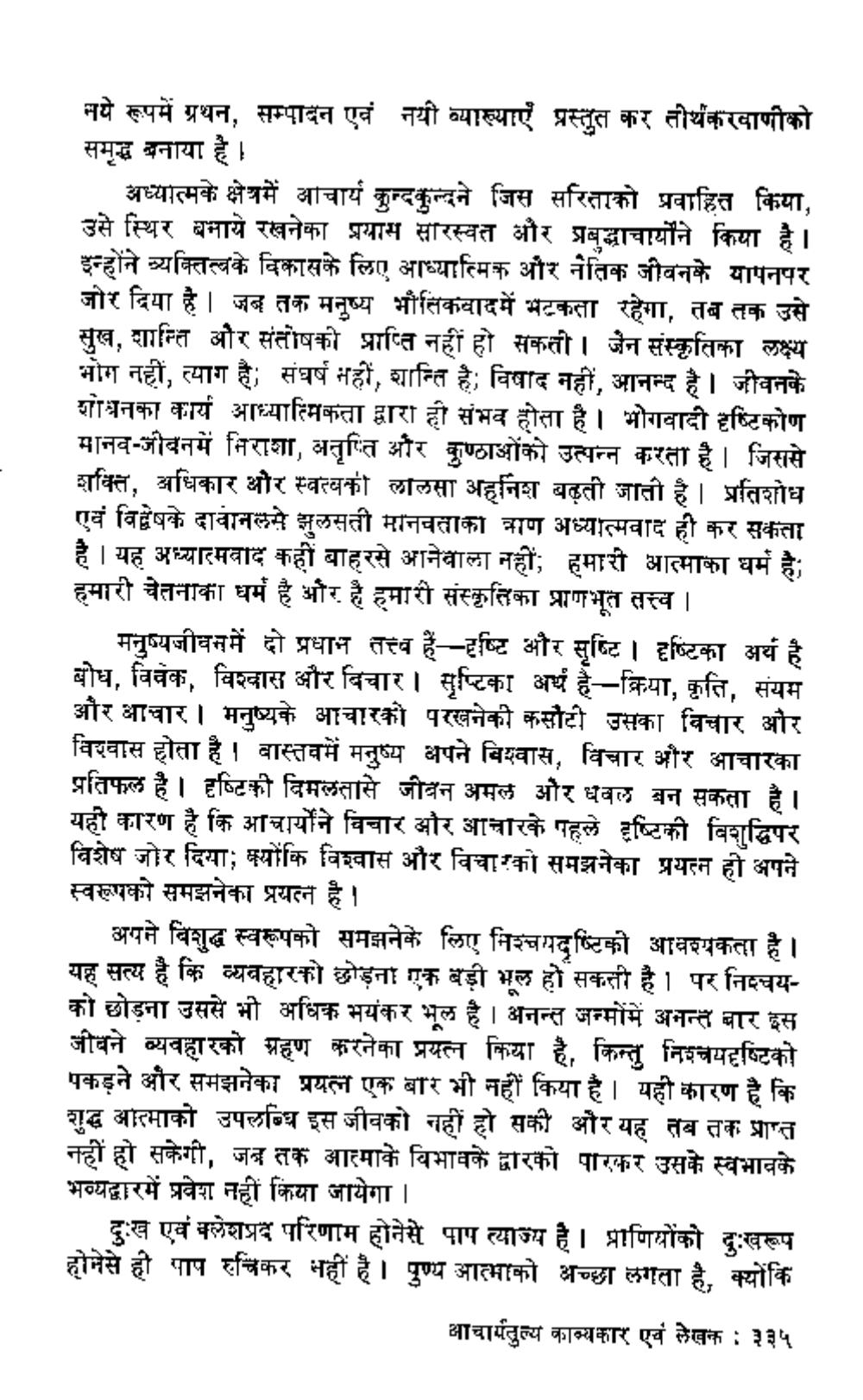________________
नये रूप में प्रथन, सम्पादन एवं नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत कर तीर्थकरवाणीको समृद्ध बनाया है। ___ अध्यात्मके क्षेत्रमें आचार्य कुन्दकुन्दने जिस सरिताको प्रवाहित किया, उसे स्थिर बनाये रखनेका प्रयास सारस्वत और प्रबुद्धाचार्योने किया है। इन्होंने व्यक्तित्व के विकासके लिए आध्यात्मिक और नैतिक जीवनके यापनपर जोर दिया है | जब तक मनुष्य भौतिकवादमें भटकता रहेगा, तब तक उसे सुख, शान्ति और संतोषको प्राप्ति नहीं हो सकती। जैन संस्कृतिका लक्ष्य भोग नहीं, त्याग है; संघर्ष नहीं, शान्ति है; विषाद नहीं, आनन्द है। जीवनके शोधनका कार्य आध्यात्मिकता द्वारा ही संभव होता है। भोगवादी दृष्टिकोण मानव-जीवनमें निराशा, अतृप्ति और कुण्ठाओंको उत्पन्न करता है। जिससे शक्ति. अधिकार और स्वत्वकी लालसा अहर्निश बढ़ती जाती है। प्रतिशोध एवं विद्वेषके दावानलसे झुलसती मानवताका वाण अध्यात्मवाद ही कर सकता है । यह अध्यात्मवाद कहीं बाहरसे आनेवाला नहीं; हमारी आत्माका धर्म है। हमारी चेतनाका धर्म है और है हमारी संस्कृतिका प्राणभूत तत्त्व ।
मनुष्यजीवन में दो प्रधान तत्त्व हैं-दृष्टि और सृष्टि । दृष्टिका अर्थ है बोध, विवेक, विश्वास और विचार । सुप्टिका अर्थ है-क्रिया, कृति, संयम और आचार। मनुष्यके आचारको परखनेकी कसौटी उसका विचार और विश्वास होता है। वास्तवमें मनुष्य अपने विश्वास, विचार और आचारका प्रतिफल है। दृष्टिकी विमलतासे जीवन अमल और धवल बन सकता है। यही कारण है कि आचार्योने विचार और आचारके पहले दृष्टिकी विशुद्धिपर विशेष जोर दिया; क्योंकि विश्वास और विचारको समझनेका प्रयत्न ही अपने स्वरूपको समझनेका प्रयत्न है। __ अपने विशुद्ध स्वरूपको समझनेके लिए निश्च यदष्टिको आवश्यकता है। यह सत्य है कि व्यवहारको छोड़ना एक बड़ी भल हो सकती है। पर निश्चयको छोड़ना उससे भी अधिक भयंकर भल है । अनन्त जन्मों में अनन्त बार इस जीवने व्यवहारको ग्रहण करनेका प्रयत्न किया है, किन्तु निश्चयदृष्टिको पकड़ने और समझनेका प्रयल एक बार भी नहीं किया है। यही कारण है कि शुद्ध आत्माको उपलब्धि इस जीवको नहीं हो सकी और यह तब तक प्राप्त नहीं हो सकेगी, जब तक आत्माके विभावके द्वारको पारकर उसके स्वभावके भव्यद्वारमें प्रवेश नहीं किया जायेगा।
दुःख एवं क्लेशप्रद परिणाम होनेसे पाप त्याज्य है । प्राणियोंको दुःखरूप होनेसे ही पाप रुचिकर नहीं है । पुण्य आत्माको अच्छा लगता है, क्योंकि
आचार्यतुल्य कान्यकार एवं लेखक : ३३५