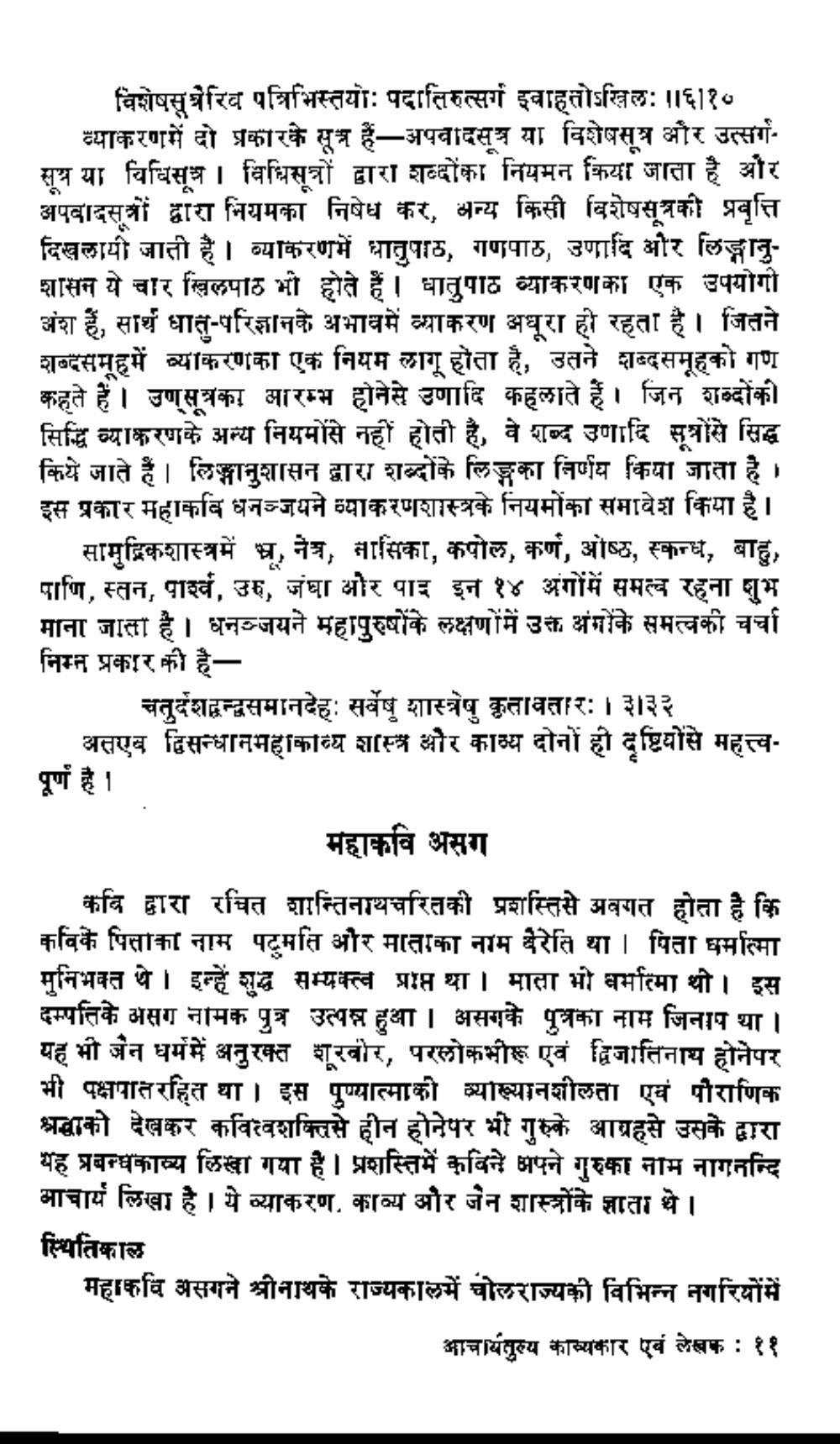________________
विशेषसूत्रेरिव पत्रिभिस्तयोः पदातिरुत्सर्ग इवाह्तोऽखिलः ।। ६।१० व्याकरण में दो प्रकारके सूत्र हैं- अपवादसूत्र या विशेषसूत्र और उत्सर्गसूत्र या विधिसूत्र | विधिसूत्रों द्वारा शब्दोंका नियमन किया जाता है और अपवादसूत्रों द्वारा नियमका निषेध कर, अन्य किसी विशेषसूत्रकी प्रवृत्ति दिखलायी जाती है । व्याकरणमें धातुपाठ, गणपाठ, उणादि और लिङ्गानुशासन ये चार ख़िलपाठ भी होते हैं। धातुपाठ व्याकरणका एक उपयोगी अंश हैं, सार्थ धातु-परिज्ञानके अभाव में व्याकरण अधूरा ही रहता है। जितने शब्दसमूहमें व्याकरणका एक नियम लागू होता है, उतने शब्दसमूहको गण कहते हैं । उणसूत्रका आरम्भ होनेसे उणादि कहलाते हैं। जिन शब्दोंकी सिद्धि व्याकरण के अन्य नियमोंसे नहीं होती है, वे शब्द उणादि सूत्रोंसे सिद्ध किये जाते हैं । लिङ्गानुशासन द्वारा शब्दों के लिङ्गका निर्णय किया जाता है । इस प्रकार महाकवि धनजयने व्याकरणशास्त्र के नियमों का समावेश किया है ।
सामुद्रिकशास्त्र में, नेत्र, नासिका, कपोल, कर्ण, ओष्ठ, स्कन्ध, बाहु, पाणि, स्तन, पार्श्व, उरु, जंघा और पाइ इन १४ अंगों में समत्व रहना शुभ माना जाता है । धनञ्जयने महापुरुषोंके लक्षणों में उक्त अंगों के समत्वकी चर्चा निम्न प्रकार की है
चतुर्दशद्वन्द्वसमानदेहः सर्वेषु शास्त्रेषु कृतावतारः । ३।३३
अतएव द्विसन्धानमहाकाव्य शास्त्र और काव्य दोनों ही दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है ।
महाकवि असग
कवि द्वारा रचित शान्तिनाथचरितकी प्रशस्तिसे अवगत होता है कि कविके पिताका नाम पटुमति और माताका नाम बेरेति था। पिता धर्मात्मा मुनिभक्त थे । इन्हें शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त था । माता भी वर्मात्मा थी । इस दम्पत्तिके असग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । असगके पुत्रका नाम जिनाप था । यह भी जैन धर्म में अनुरक्त शूरवीर, परलोकभीरू एवं द्विजातिनाथ होनेपर भी पक्षपातरहित था । इस पुण्यात्माको व्याख्यानशीलता एवं पौराणिक श्रद्धाको देखकर कविश्वशक्तिसे हीन होनेपर भी गुरुके आग्रहसे उसके द्वारा यह प्रबन्धकाव्य लिखा गया है। प्रशस्ति में कविने अपने गुरुका नाम नागतन्दि आचार्य लिखा है । ये व्याकरण. काव्य और जेन शास्त्रोंके ज्ञाता थे ।
स्थितिकाल
महाकवि असमने श्रीनाथके राज्यकालमें चोलराज्यकी विभिन्न नगरियों में आचार्य तुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११