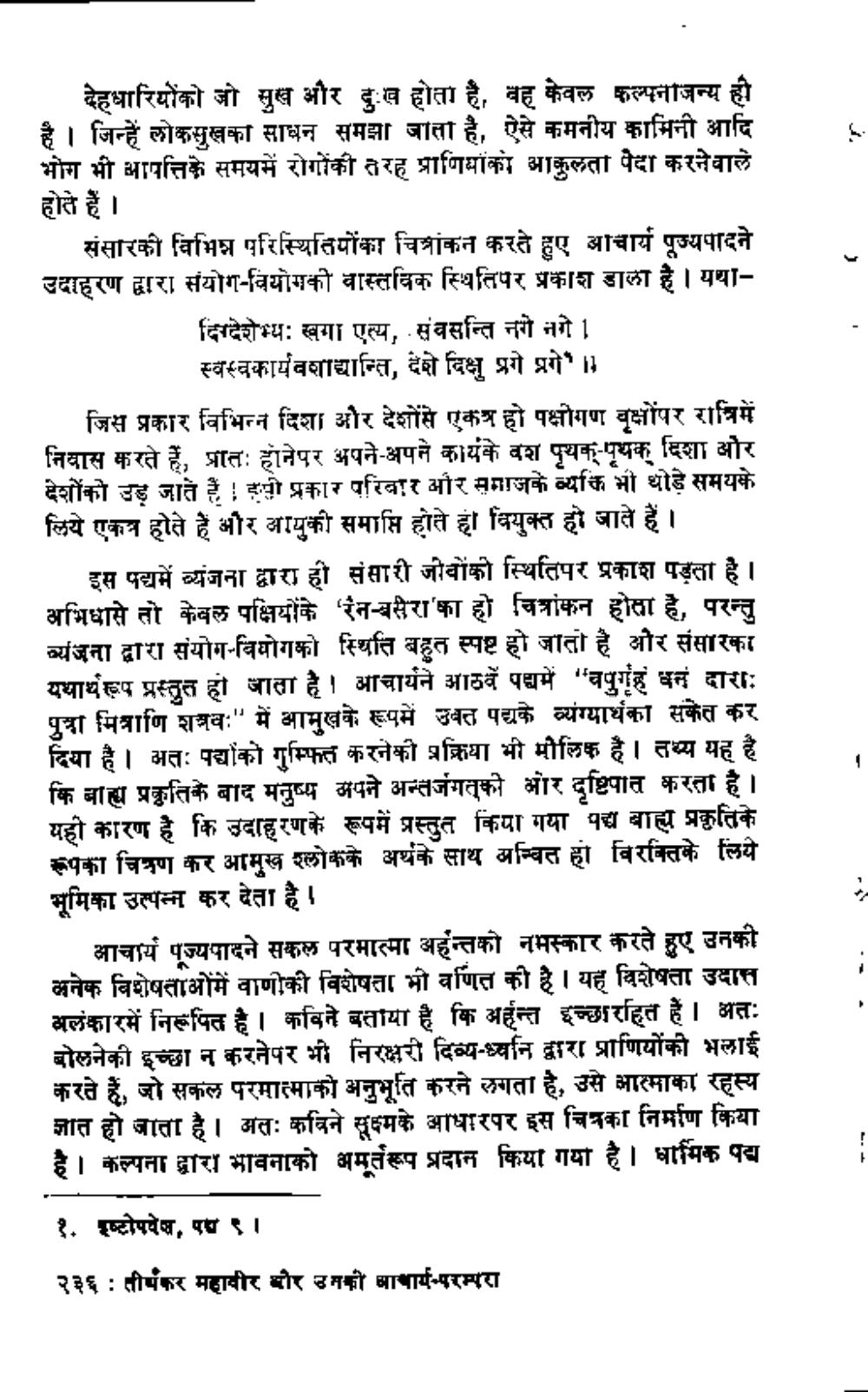________________
देहधारियोंको जो सुख और दुःख होता है, वह केवल कल्पनाजन्य ही है । जिन्हें लोकसुखका साधन समझा जाता है, ऐसे कमनीय कामिनी आदि भोग भी आपत्ति के समय में रोगोंकी तरह प्राणिमांको आकुलता पैदा करनेवाले होते हैं ।
संसारकी विभिन्न परिस्थितियोंका चित्रांकन करते हुए आचार्य पूज्यपादने उदाहरण द्वारा संयोग-वियोगको वास्तविक स्थितिपर प्रकाश डाला है । यथादिग्देशेभ्यः स्वगा एत्य, संवसन्ति नगे नगे 1 स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे' ||
जिस प्रकार विभिन्न दिशा और देशोंसे एकत्र हो पक्षीगण वृक्षोंपर रात्रि में निवास करते हैं, प्रातः होनेपर अपने-अपने कार्यके वश पृथक-पृथक दिशा और देशों को उड़ जाते हैं । इसी प्रकार परिवार और समाजके व्यक्ति भी थोड़े समय के लिये एकत्र होते हैं और आयुकी समाप्ति होते ही वियुक्त हो जाते हैं ।
इस पद्यमें व्यंजना द्वारा ही संसारी जीवों की स्थितिपर प्रकाश पड़ता है । अभिधासे तो केवल पक्षियों के 'रैन बसेरा' का हो चित्रांकन होता है, परन्तु व्यंजना द्वारा संयोग-वियोगको स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है और संसारका यथार्थरूप प्रस्तुत हो जाता है। आचार्यने आठवें पद्यमें "चपुगृहं वनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः" में आमुख के रूप में उक्त पद्यके व्यंग्यार्थंका संकेत कर दिया है। अतः पद्योंको गुम्फित करनेकी प्रक्रिया भी मौलिक हैं। तथ्य यह है कि बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तर्जगत्को ओर दृष्टिपात करता है । यही कारण है कि उदाहरण के रूपमें प्रस्तुत किया गया पद्य बाह्य प्रकृतिके रूपका चित्रण कर आमुख श्लोकके अर्थके साथ अन्वित हो विरक्तिके लिये भूमिका उत्पन्न कर देता है ।
आचार्य पूज्यपादने सकल परमात्मा अर्हन्तको नमस्कार करते हुए उनकी अनेक विशेषताओंमें वाणीकी विशेषता भी वर्णित की है। यह विशेषता उदास अलंकारमें निरूपित है । कविने बताया है कि अर्हन्त इच्छा रहित हैं । अतः बोलनेकी इच्छा न करनेपर भी निरक्षरी दिव्य-ध्वनि द्वारा प्राणियोंकी भलाई करते हैं, जो सकल परमात्माको अनुभूति करने लगता है, उसे आत्माका रहस्य ज्ञात हो जाता है | अतः कविने सूक्ष्मके आधारपर इस चित्रका निर्माण किया है । कल्पना द्वारा भावनाको अमूर्तरूप प्रदान किया गया है। धार्मिक पद्म
१. इष्टोपवेश पद्म ९ ।
.
२३६ : तीर्थंकर महावीर बोर उनको आचार्य-परम्परा
1
F