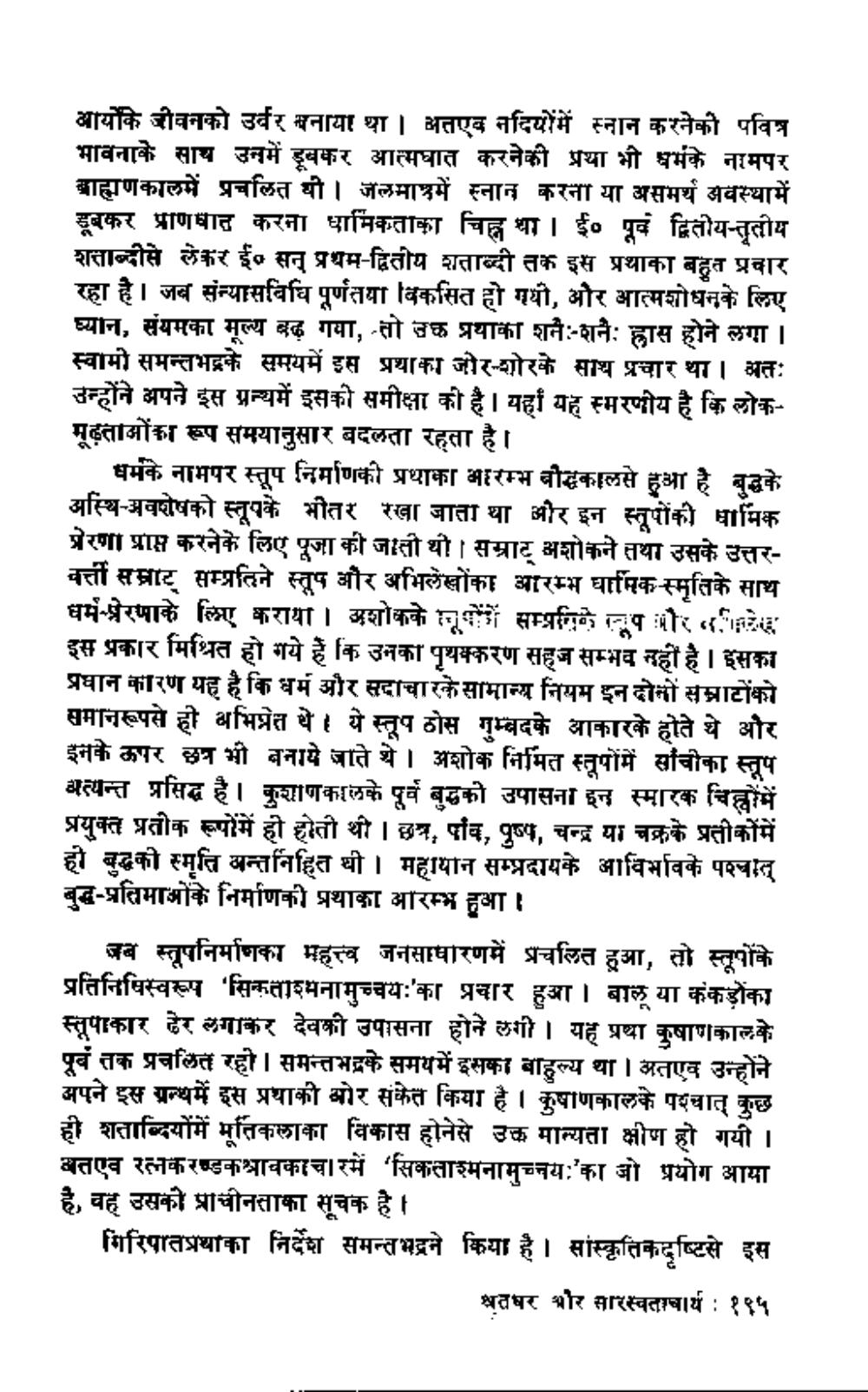________________
आर्योंके जीवनको उर्वर बनाया था। अतएव नदियों में स्नान करनेकी पवित्र भावनाके साथ उनमें डूबकर आत्मघात करनेकी प्रथा भी धर्मके नामपर ब्राह्मणकालमें प्रचलित थी । जलमाश्रमें स्नान करना या असमर्थ अवस्थामें डूबकर प्राणघात करना धार्मिकताका चिह्न था । ई० पूर्व द्वितीय तृतीय शताब्दीसे लेकर ई० सन् प्रथम- द्वितीय शताब्दी तक इस प्रथाका बहुत प्रचार रहा है । जब संन्यासविधि पूर्णतया विकसित हो गयी, और आत्मशोधन के लिए ध्यान, संयमका मूल्य बढ़ गया, तो उक प्रथाका शनैः-शनैः ह्रास होने लगा । स्वामी समन्तभद्रके समयमें इस प्रथाका जोर-शोर के साथ प्रचार था । अतः उन्होंने अपने इस ग्रन्थ में इसकी समीक्षा की है । यहाँ यह स्मरणीय है कि लोकमूढ़ताओं का रूप समयानुसार बदलता रहता है ।
धर्मके नामपर स्तूप निर्माणको प्रथाका आरम्भ बौद्धकालसे हुआ है बुद्धके अस्थि-अवशेषको स्तूपके भीतर रखा जाता था और इन स्तूपोंकी धार्मिक प्रेरणा प्राप्त करनेके लिए पूजा की जाती थी । सम्राट् अशोकने तथा उसके उत्तरचत्तीं सम्राट् सम्प्रतिने स्तुप और अभिलेखोंका आरम्भ धार्मिक स्मृतिके साथ धर्म-प्रेरणाके लिए कराया । अशोक सम्प्रति सूप और लेख इस प्रकार मिश्रित हो गये हैं कि उनका पृथक्करण सहज सम्भव नहीं है । इसका प्रधान कारण यह है कि धर्म और सदाचारके सामान्य नियम इन दोनों सम्राटों को समानरूपसे ही अभिप्रेत थे । ये स्तूप ठोस गुम्बदके आकारके होते थे और इनके ऊपर छत्र भी बनाये जाते थे। अशोक निर्मित स्तूपों में सांचीका स्तूप अत्यन्त प्रसिद्ध है । कुशाणकालके पूर्व बुद्धको उपासना इन स्मारक चिल्लोंमें प्रयुक्त प्रतीक रूपों में ही होती थी । छत्र, पांव, पुष्प, चन्द्र या चक्रके प्रतीकों में हो बुद्धकी स्मृति अन्तर्निहित थी । महायान सम्प्रदाय के आविर्भावके पश्चात् बुद्ध प्रतिमाओं के निर्माणकी प्रथाका आरम्भ हुआ ।
जब स्तूपनिर्माणका महत्त्व जनसाधारण में प्रचलित हुआ, तो स्तूपोंके प्रतिनिषिस्वरूप 'सिकताश्मनामुच्चयः का प्रचार हुआ। बालू या कंकड़ोंका स्तूपाकार ढेर लगाकर देवकी उपासना होने लगी । यह प्रथा कुषाणकाल के पूर्व तक प्रचलित रहो । समन्तभद्रके समय में इसका बाहुल्य था । अतएव उन्होंने अपने इस ग्रन्थ में इस प्रथाकी ओर संकेत किया है । कुषाणकालके पश्चात् कुछ ही शताब्दियों में मूर्तिकलाका विकास होनेसे उक्त मान्यता क्षीण हो गयी | बत्तएव रत्नकरण्डक श्रावकाच । रमें 'सिकतारमनामुच्नयः का जो प्रयोग आया है, वह उसको प्राचीनताका सूचक है ।
गिरिपातप्रथाका निर्देश समन्तभद्रने किया है। सांस्कृतिकदृष्टिसे इस
श्रवर श्रीर सारस्वताचार्य १९५