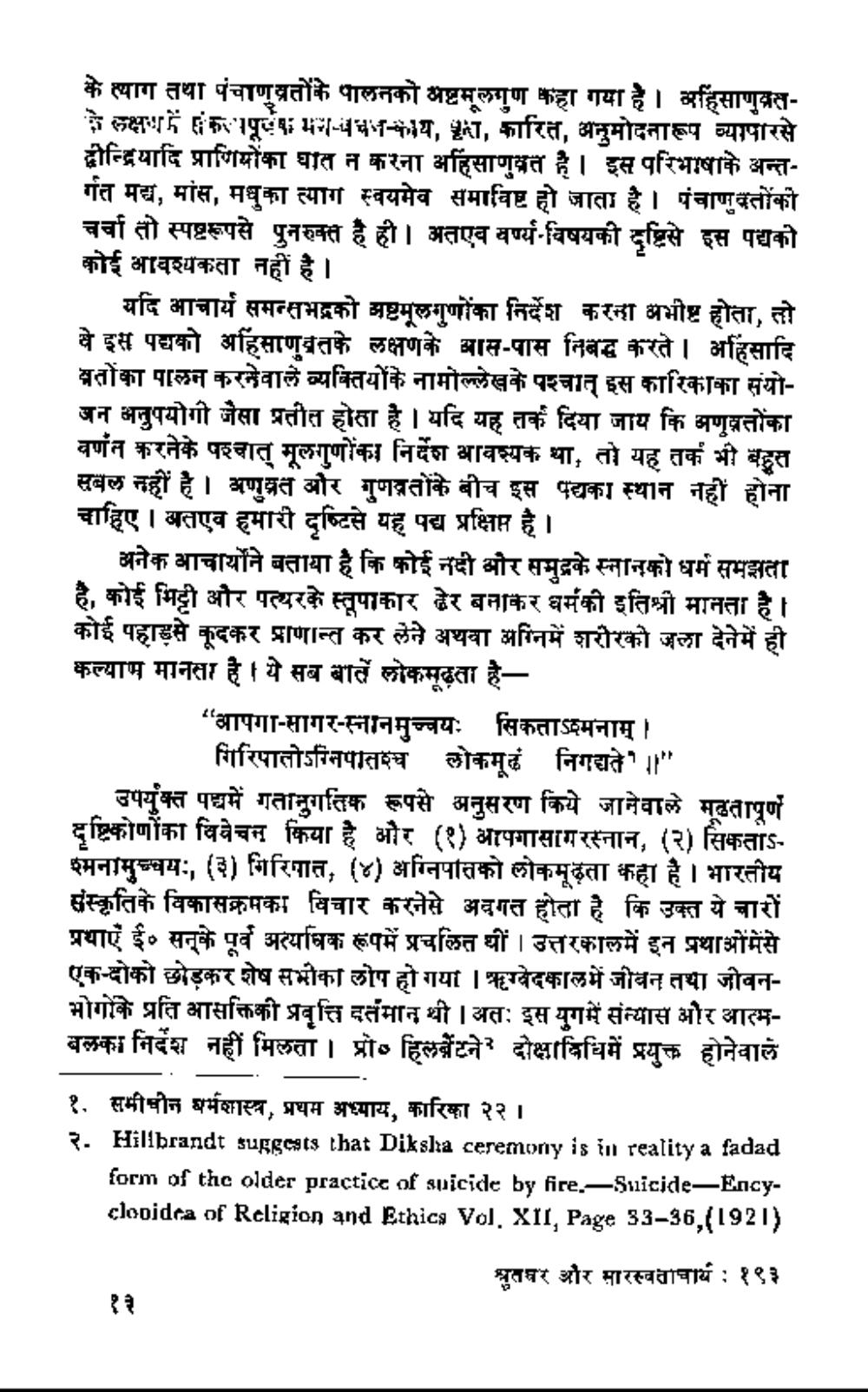________________
के त्याग तथा पंचाणुव्रतोंके पालनको अष्टमूलगुण कहा गया है। अहिंसाणुव्रतके लक्षण कापूर मन-धमकाय, मा, कारित, अनुमोदनारूप व्यापारसे द्वीन्द्रियादि प्राणियोंका घात न करना अहिंसाणुवत है। इस परिभाषाके अन्तर्गत मद्य, मांस, मधुका त्याग स्वयमेव समाविष्ट हो जाता है। पंचाणुक्तोंको चर्चा तो स्पष्टरूपसे पुनरुक्त है ही। अतएव वर्ण्य विषयकी दृष्टिसे इस पद्यको कोई आवश्यकता नहीं है। ___ यदि आचार्य समन्तभद्रको अष्टमूलगुणोंका निर्देश करना अभीष्ट होता, तो वे इस पद्यको अहिंसाणुव्रतके लक्षणके आस-पास निबद्ध करते । अहिंसादि बतोंका पालन करनेवाले व्यक्तियोंके नामोल्लेखके पश्चात् इस कारिकाका संयोजन अनुपयोगी जैसा प्रतीत होता है । यदि यह तर्क दिया जाय कि अणुव्रतोंका वर्णन करनेके पश्चात् मूलगुणोंका निर्देश आवश्यक था, तो यह तर्क भी बहुत सबल नहीं है । अणुव्रत और गुणवतोंके बीच इस पद्यका स्थान नहीं होना चाहिए । अतएव हमारी दृष्टिसे यह पद्य प्रक्षिप्त है। ___ अनेक आचार्योंने बताया है कि कोई नदी और समुद्रके स्नानको धर्म समझता है, कोई भिटी और पत्थरके स्तुपाकार ढेर बनाकर धमकी इतिश्री मानता है। कोई पहाड़से कूदकर प्राणान्त कर लेने अथवा अग्निमें शरीरको जला देनेमें ही कल्याम मानता है । ये सब बातें लोकमूढ़ता है
"आपगा-सागर-स्नानमुच्चयः सिकताऽश्मनाम् ।
गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ।।" उपर्युक्त पद्यमें गतानुगतिक रूपसे अनुसरण किये जानेवाले मूढतापूर्ण दृष्टिकोणोंका विवेचन किया है और (१) आपगासागरस्नान, (२) सिकताsश्मनामुच्चयः, (३) गिरिपात, (४) अग्निपातको लोकमूढ़ता कहा है । भारतीय संस्कृतिक विकासक्रमका विचार करनेसे अवगत होता है कि उक्त ये चारों प्रथाएँ ई. सन्के पूर्व अत्यधिक रूपमें प्रचलित थीं । उत्तरकालमें इन प्रथाओंमेंसे एक-दोको छोड़कर शेष सभीका लोप हो गया | ऋग्वेदकालमें जीवन तथा जीवनभोगोंके प्रति आसक्तिकी प्रवृत्ति दर्तमान थी । अतः इस युगमें संन्यास और आत्मबलका निर्देश नहीं मिलता। प्रो० हिलनेटने दोक्षाविधिमें प्रयुक्त होनेवाले
१. समीचीन धर्मशास्त्र, प्रथम अध्याय, कारिका २२ । 3. Hillbrandt suggests that Diksha ceremony is in reality a fadad
form of the older practice of suicide by fire.-Suicide-Encyclooidea of Religion and Ethics Vol. XII, Page 33-36,(1921)
श्रुतघर और मारस्वताचार्य : १९३