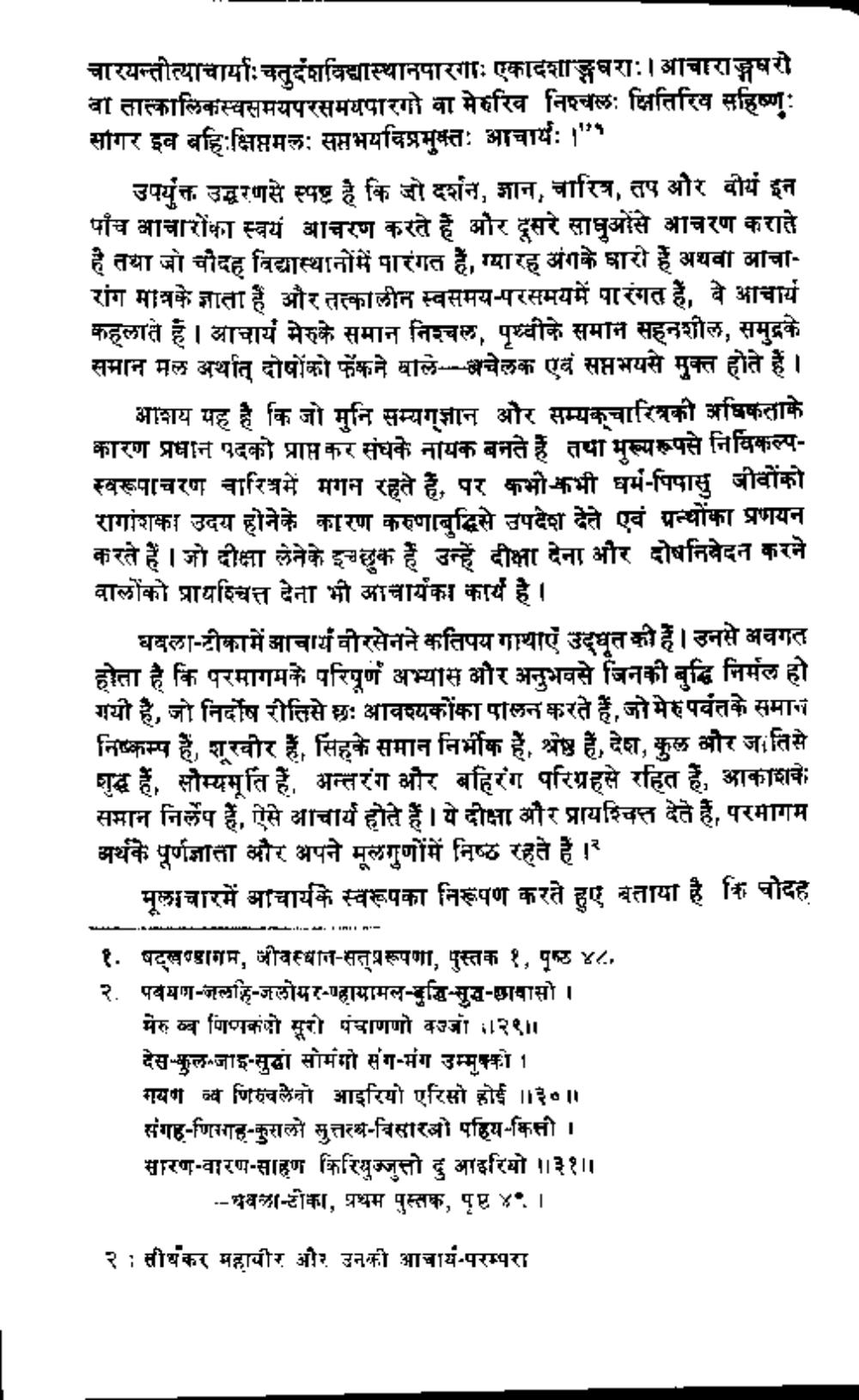________________
चारयन्तीत्याचार्याः चतुर्दशविद्यास्थानपारगाः एकादशाङ्गधराः । आचाराङ्गषरो वा तात्कालिक स्वसमयपरसमयपारगो वा मेरुरिव निश्चलः क्षितिरिव सहिष्णुः सांगर इव बहिः क्षिप्तमलः सप्तभयविप्रमुक्तः आचार्यः |""
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीयं इन पाँच आचारोंका स्वयं आचरण करते हैं और दूसरे साधुओंसे आचरण कराते है तथा जो चौदह विद्यास्थानों में पारंगत हैं, ग्यारह अंगके घारी है अथवा याचारांग मात्रके ज्ञाता हैं और तत्कालीन स्वसमय-परसमय में पारंगत हैं, वे आचार्य कहलाते हैं | आचार्यं मेरुके समान निश्चल, पृथ्वीके समान सहनशील, समुद्रके समान मल अर्थात् दोषोंको फेंकने वाले अचेलक एवं सप्तभयसे मुक्त होते हैं ।
आशय यह है कि जो मुनि सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी अधिकता के कारण प्रधान पदको प्राप्त कर संघके नायक बनते हैं तथा मुख्यरूपसे निर्विकल्पस्वरूपाचरण चारित्र में मगन रहते हैं, पर कभी-कभी धर्म-पिपासु जीवोंको रागांशका उदय होनेके कारण करुणाबुद्धिसे उपदेश देते एवं प्रत्थोंका प्रणयन करते हैं । जो दीक्षा लेने के इच्छुक हैं उन्हें दीक्षा देना और दोषनिवेदन करने वालोंको प्रायश्चित्त देना भी आचार्यका कार्य है ।
घवला
का टीका में आचार्यं वीरसेनने कतिपय गाथाएँ उद्धृत की हैं। उनसे अवगत होता है कि परमागम के परिपूर्ण अभ्यास और अनुभवसे जिनकी बुद्धि निर्मल हो गयी है, जो निर्दोष रीतिसे छः आवश्यकों का पालन करते हैं, जो मेरु पर्वत के समान निष्कम्प हैं, शूरवीर हैं, सिहके समान निर्भीक है, श्रेष्ठ हैं, देश, कुल और जाति से शुद्ध हैं, सोम्यमूर्ति हैं, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहसे रहित हैं, आकाशके समान निर्लेप हैं, ऐसे आचार्य होते हैं । ये दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं, परमागम अर्थके पूर्णज्ञाता और अपने मूलगुणों में निष्ठ रहते हैं ।
मूलाचारमें आचार्य के स्वरूपका निरूपण करते हुए बताया है कि चौदह
१. षट्खण्डागम, जीवस्थान-सत्प्ररूपणा, पुस्तक १, पृष्ठ ४८.
२. पण जलहि-जलोय र पहायामल - बुद्धि-सुद्ध - छावासो | मेरु व णिकंदो सूरो पंचाणणो वजी ॥ २९ ॥ देस -कुल- जाइ सुद्धा सोमंगो संग-संग उम्मुको गयण व णिश्वलेनो आइरियो एरिसो होई ॥३०॥ संगह णिमाह- कुराको सुत्तत्य-विसार पहिय- किती । सारण-वारण साहृण किरियुज्जुतो दु आइरियो ||३१|| - पवाटीका, प्रथम पुस्तक, पृष्ठ ४९ ।
२ : सीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा