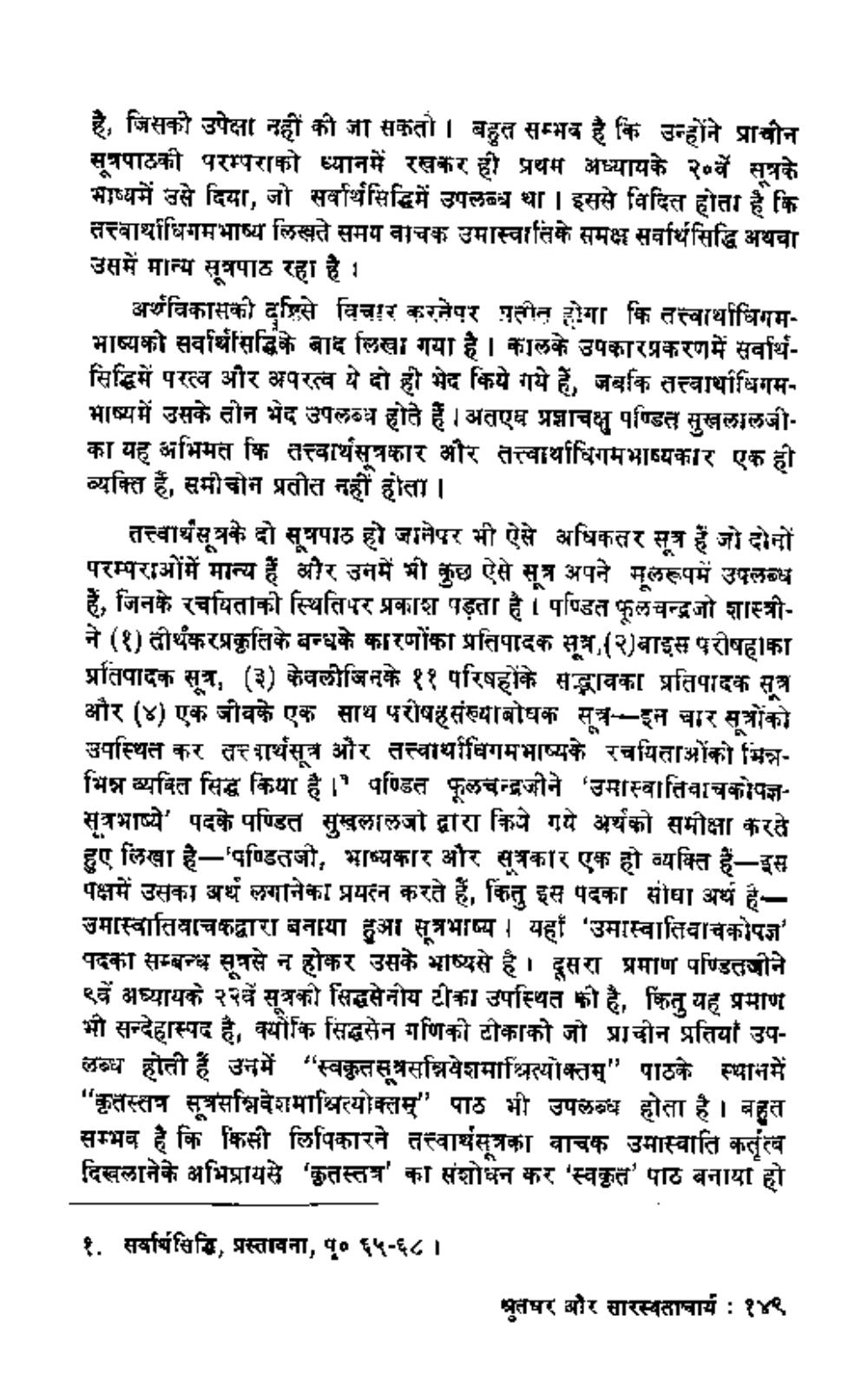________________
है, जिसको उपेक्षा नहीं की जा सकतो। बहुत सम्भव है कि उन्होंने प्राचीन सूत्रपाठकी परम्पराको ध्यानमें रखकर ही प्रथम अध्यायके २०वें सूत्रके भाष्यमें उसे दिया, जो सर्वार्थसिद्धिमें उपलब्ध था। इससे विदित होता है कि तत्त्वार्थाधिगमभाष्य लिखते समय वाचक उमास्वातिके समक्ष सर्वार्थसिद्धि अथवा उसमें मान्य सूत्रपाठ रहा है । ___ अर्थविकासको दृष्सेि विचार करने पर प्रतीत होगा कि तत्त्वार्थाधिगमभाष्यको सर्वार्थसिद्धिके बाद लिखा गया है । कालके उपकारप्रकरण में सर्वार्थसिद्धिमें परत्व और अपरत्व ये दो ही भेद किये गये हैं, जबकि तत्त्वार्थाधिगमभाष्यमें उसके तीन भेद उपलब्ध होते हैं । अतएप प्रज्ञाचक्षु पण्डित सुखलालजीका यह अभिमत कि तत्त्वार्थसूत्रकार और तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकार एक ही व्यक्ति हैं, समोचोन प्रतीत नहीं होता। __ तत्वार्थ सूत्रके दो सूत्रपाठ हो जानेपर भी ऐसे अधिकतर सूत्र हैं जो दोनों परम्पराओंमें मान्य हैं और उनमें भी कुछ ऐसे सूत्र अपने मूलरूपमें उपलब्ध हैं, जिनके रचयिताको स्थितिपर प्रकाश पड़ता है । पण्डित फूलचन्द्रजो शास्त्रीने (१) तीर्थंकरप्रकृतिके बन्धके कारणोंका प्रतिपादक सत्र (२)बाइस परीषहाका प्रतिपादक सूत्र, (३) केवलीजिनके ११ परिषहोंके सद्भावका प्रतिपादक सूत्र और (४) एक जीवके एक साथ परीषहसंख्याबोधक सूत्र-इन चार सूत्रोंको उपस्थित कर तत्त्वार्थसूत्र और तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके रचयिताओंको मिन्नभिन्न व्यक्ति सिद्ध किया है।' पण्डित फूलचन्द्रजीने 'उमास्वातिवाचकोपज्ञसवभाष्ये' पदके पण्डित सुखलालजो द्वारा किये गये अर्थको समीक्षा करते हुए लिखा है-'पण्डितजी, भाष्यकार और सूत्रकार एक हो व्यक्ति हैं-इस पक्षमें उसका अर्थ लगानेका प्रयत्न करते हैं, किंतु इस पदका सीधा अर्थ हैउमास्वातिवाचकद्वारा बनाया हुआ सूत्रभाष्य । यहाँ 'उमास्वातिवाचकोपज्ञ' पदका सम्बन्ध सबसे न होकर उसके भाष्यसे है। दूसरा प्रमाण पण्डितजीने ९वें अध्यायके २२वें सूत्रको सिद्धसेनीय टीका उपस्थित की है, किंतु यह प्रमाण भी सन्देहास्पद है, क्योंकि सिद्धसेन गणिको टोकाको जो प्राचीन प्रतियां उपलब्ध होती हैं उनमें "स्वकृतसूत्रसन्निवेशमाश्रियोक्तम्" पाठके स्थानमें "कृतस्तत्र सूत्रसन्निवेशमाश्रित्योक्तम्" पाठ भी उपलब्ध होता है। बहुत सम्भव है कि किसी लिपिकारने तत्त्वार्थसूत्रका वाचक उमास्वाति कर्तृत्व दिखलानेके अभिप्रायसे 'कुतस्तत्र' का संशोधन कर 'स्वकृत' पाठ बनाया हो
१. सर्वार्थसिडि, प्रस्तावना, पृ० ६५-६८ ।
श्रुतघर और सारस्वताचार्य : १४९