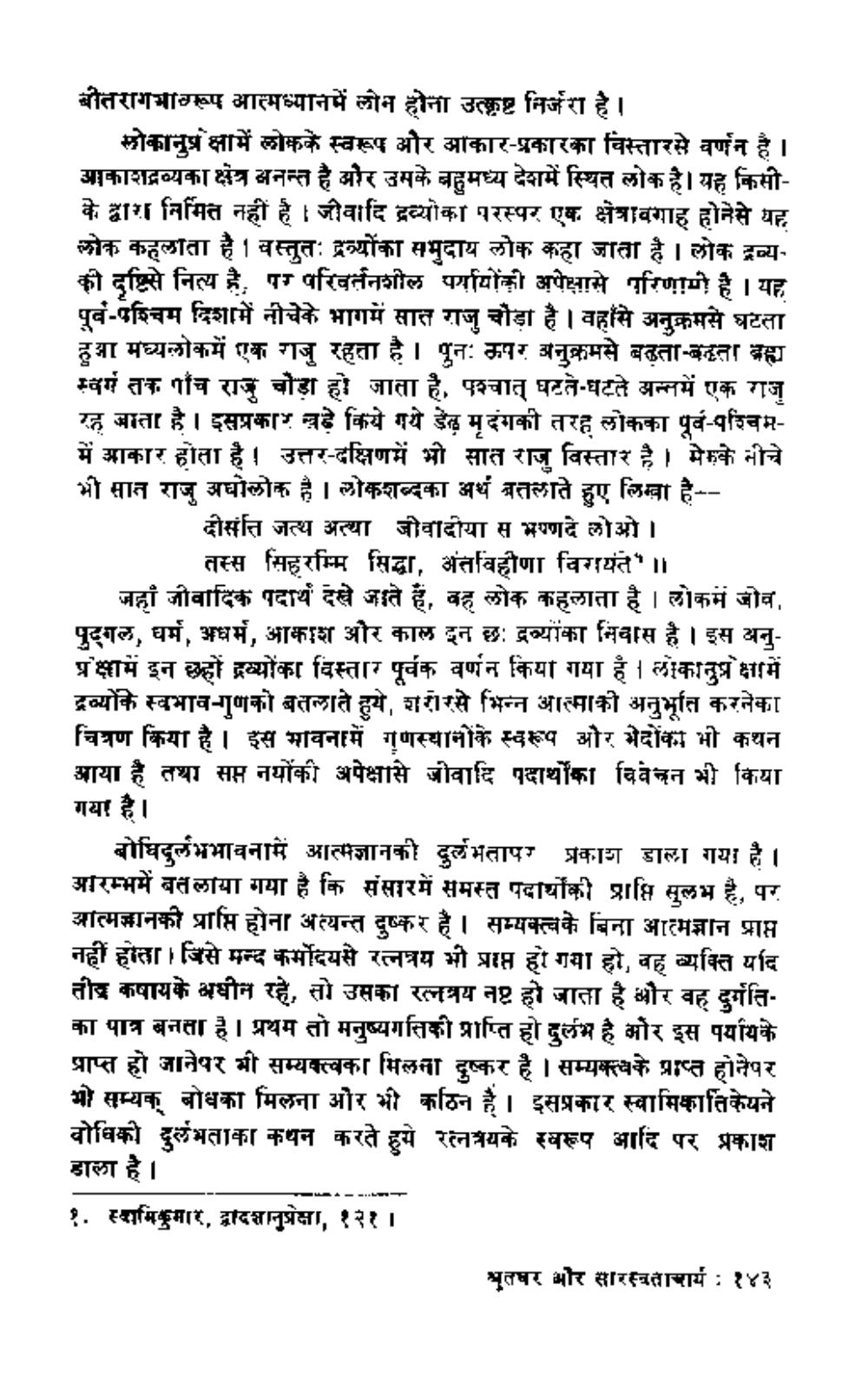________________
बीतराग भावरूप आत्मध्यानमें लोन होना उत्कृष्ट निर्जरा है ।
I
लोकानुत्रं क्षा में लोकके स्वरूप और आकार-प्रकारका विस्तारसे वर्णन है । आकाशद्रव्यका क्षेत्र अनन्त है और उसके बहुमध्य देशमें स्थित लोक है। यह किसीके द्वारा निर्मित नहीं है। जीवादि द्रव्योका परस्पर एक क्षेत्रावगाह होने से यह लोक कहलाता है । वस्तुतः द्रव्यों का समुदाय लोक कहा जाता है । लोक द्रव्यकी दृष्टिसे नित्य है, पर परिवर्तनशील पर्यायोंकी अपेक्षा परिणामी है । यह पूर्व-पश्चिम दिशामें नीचेके भागमें सात राजु चौड़ा है। वहाँ अनुक्रमसे घटता हुआ मध्यलोकमें एक राजु रहता है। पुनः ऊपर अनुक्रमसे बढ़ता बहता ब्रह्म स्वर्ग तक पांच राजु चौड़ा हो जाता है, पश्चात् घटते घटते अन्तमें एक राज रह जाता है । इसप्रकार बड़े किये गये डेढ़ मृदंगकी तरह लोकका पूर्व-पश्चिममें आकार होता है। उत्तर-दक्षिण में भी सात राजु विस्तार है। मैकके नीचे भी सात राजु अधोलोक है । लोकशब्दका अर्थ बतलाते हुए लिखा हैदीति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ । तस्स सिहरम्मि सिद्धा, अंत्तविहीणा विरायंते ॥
जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक कहलाता है । लोकमं जोव. पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छः द्रव्यांका निवास है । इस अनुप्रक्षा इन छहों द्रव्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लोकानुप्रक्षा में द्रव्योंके स्वभाव-गुणको बतलाते हुये, शरीर से भिन्न आत्माकी अनुभूति करनेका चित्रण किया है । इस भावना में गुणस्थानोंके स्वरूप और भेदोंका भी कथन आया है तथा सप्त नयोंकी अपेक्षासे जोवादि पदार्थोंका विवेन्द्रन भी किया गया है ।
बोधिदुर्लभ भावनाएं आत्मज्ञानकी दुर्लभतापर प्रकाश डाला गया है । आरम्भमें बतलाया गया है कि संसार में समस्त पदार्थोंकी प्राप्ति सुलभ है, पर आत्मज्ञानकी प्राप्ति होना अत्यन्त दुष्कर है। सम्यक्त्वके बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिसे मन्द कर्मोदयसे रत्नत्रय भी प्राप्त हो गया हो, वह व्यक्ति यदि तीव्र कषाय के अधीन रहे, तो उसका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है और वह दुर्गतिका पात्र बनता है | प्रथम तो मनुष्यगतिकी प्राप्ति हो दुर्लभ है और इस पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी सम्यक्त्वका मिलना दुष्कर है । सम्यक्त्व के प्राप्त होनेपर भो सम्यक् बोधका मिलना और भी कठिन है। इसप्रकार स्वामिकार्तिकेयने वोधिकी दुर्लभताका कथन करते हुये रत्नत्रयके स्वरूप आदि पर प्रकाश डाला है ।
१. स्वामिकुमार, द्वादशानुप्रेक्षा, १२१ ।
श्रुतवर और सारस्वताचार्य १४३