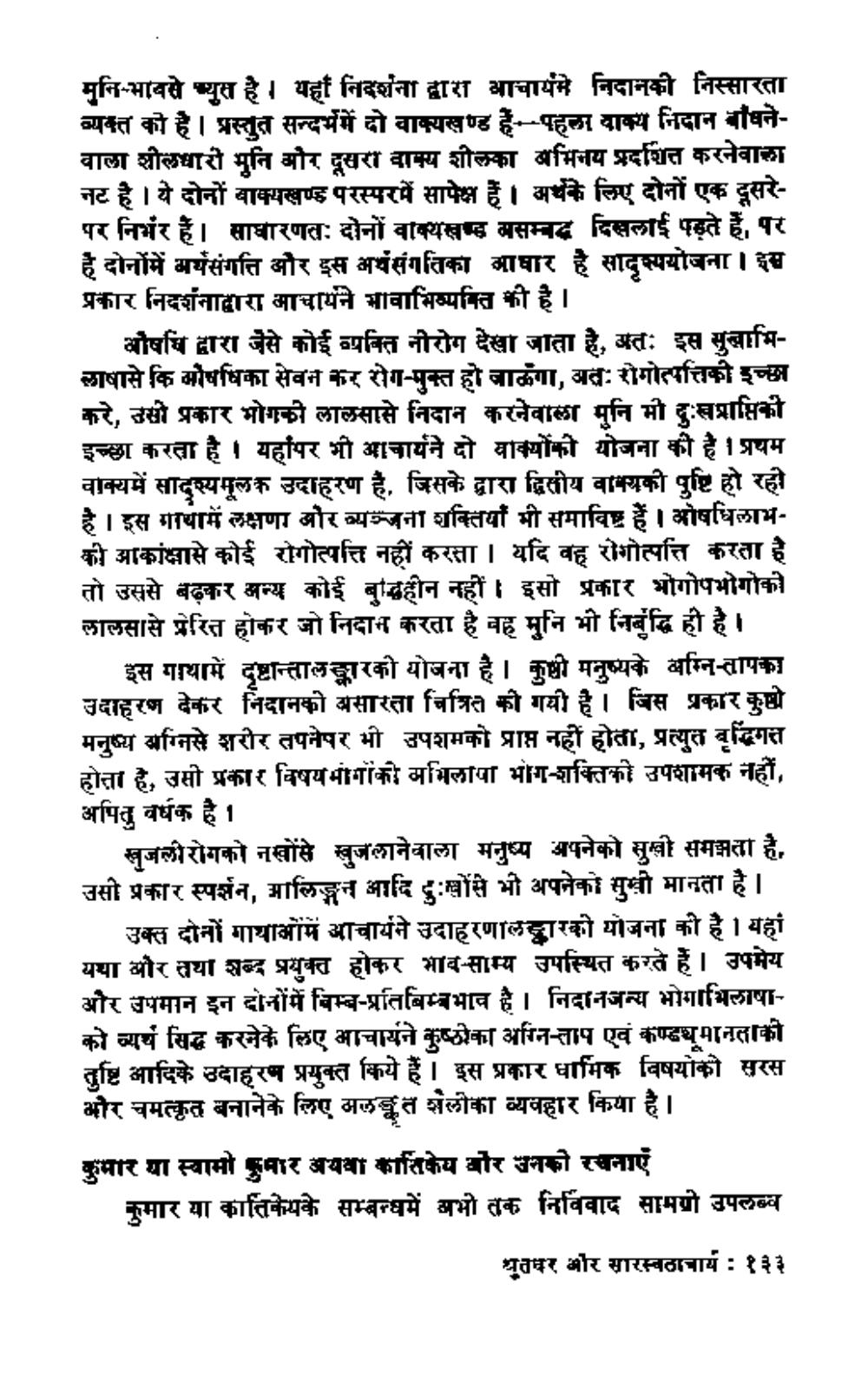________________
मुनि-भावसे व्युत है। यहां निदर्शना द्वारा आचार्यमे निदानकी निस्सारता व्यक्त को है । प्रस्तुत सन्दर्भ में दो वाक्यखण्ड हैं--पहला वाक्य निदान बाँधनेवाला शीलधारी मुनि और दूसरा वास्य शीलका अभिनय प्रदर्शित करनेवाला नट है । ये दोनों वाक्यखण्ड परस्परमें सापेक्ष हैं। अर्थके लिए दोनों एक दूसरेपर निर्भर हैं। साधारणतः दोनों वाक्यखण्ड असम्बद दिखलाई पड़ते हैं, पर है दोनोंमें अर्यसंगत्ति और इस अर्थसंगतिका आधार है सादृश्ययोजना । इस प्रकार निदर्शनाद्वारा आचार्यने भावाभिव्यक्ति की है।
बौषधि द्वारा जैसे कोई व्यक्ति नोरोग देखा जाता है, अतः इस सुखाभिलाषासे कि मौषधिका सेवन कर रोग-मुक्त हो जाऊंगा, अतः रोगोत्पत्तिको इच्छा करे, उसी प्रकार भोगको लालसासे निदान करनेवाला मुनि मी दुःखप्राप्तिको इच्छा करता है । यहाँपर भी आचार्यने दो याक्योंकी योजना की है। प्रथम वाक्यमें सादृश्यमूलक उदाहरण है, जिसके द्वारा द्वितीय वायकी पुष्टि हो रही है । इस गाथामें लक्षणा और व्यन्जना शक्तियां भी समाविष्ट हैं । ओषधिलाभकी आकांक्षासे कोई रोगोत्पत्ति नहीं करता। यदि वह रोगोत्पत्ति करता है तो उससे बढ़कर अन्य कोई बुद्धिहीन नहीं। इसो प्रकार भोगोपभोगोको लालसासे प्रेरित होकर जो निदान करता है वह मुनि भी निर्बुद्धि ही है।
इस गाथामें दृष्टान्तालङ्कारको योजना है। कुछी मनुष्यके अग्नि-तापका उदाहरण देकर निदानको असारता चित्रित की गयी है। जिस प्रकार कुछ मनुष्य अग्निसे शरीर तपनेपर भी उपशमको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वृद्धिंगत होता है, उसी प्रकार विषयमांगोंको अभिलाषा भोग-शक्तिको उपशामक नहीं, अपितु वधक है।
खुजलीरोगको नखोंसे खुजलानेवाला मनुष्य अपनेको सुम्बी समझता है, उसी प्रकार स्पर्शन, आलिङ्गन आदि दु:खोंसे भी अपनेको सुखी मानता है।
उक्त दोनों गाथाओंमें आचार्यने उदाहरणालद्वारको योजना की है। यहां यथा ओर तथा शब्द प्रयुक्त होकर भाव-साम्य उपस्थित करते हैं। उपमेय और उपमान इन दोनों में विम्ब-प्रतिबिम्बभाव है। निदानजन्य भोगाभिलाषाको व्यर्थ सिद्ध करनेके लिए आचार्यने कुष्ठीका अग्नि-ताप एवं कण्डमानताको तुष्टि आदिके उदाहरण प्रयुक्त किये हैं। इस प्रकार धार्मिक विषयोको सरस और चमत्कृत बनानेके लिए अलङ्कृत शैलीका व्यवहार किया है। कुमार या स्वामी कुमार अथवा कार्तिकेय बोर उनको रचनाएं
कुमार या कार्तिकेयके सम्बन्धमें अभी तक निर्विवाद सामग्री उपलब्ध
धृतधर और सारस्वताचार्य : १३३