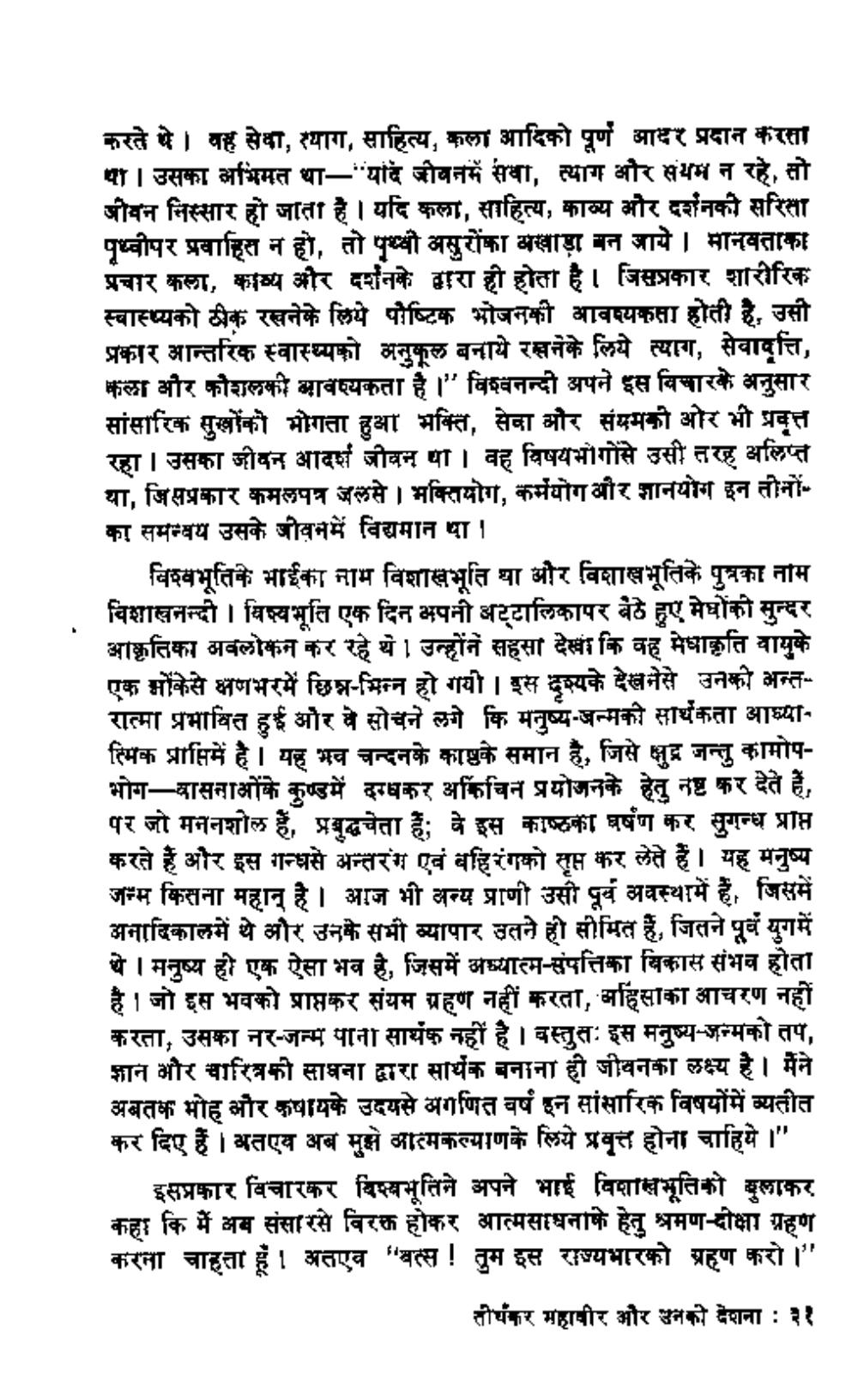________________
करते थे। वह सेवा, त्याग, साहित्य, कला आदिको पूर्ण आदर प्रदान करता था। उसका अभिमत था-"यदि जीवन में सवा, त्याग और संयम न रहे, सो जीवन निस्सार हो जाता है। यदि कला, साहित्य, काव्य और दर्शनकी सरिता पृथ्वीपर प्रवाहित न हो, तो पृथ्वी असुरोंका अखाड़ा बन जाये | मानवताका प्रचार कला, काव्य और दर्शनके द्वारा ही होता है। जिसप्रकार शारीरिक स्वास्थ्यको ठीक रखने के लिये पौष्टिक भोजनकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आन्तरिक स्वास्थ्यको अनुकूल बनाये रखने के लिये त्याग, सेवावृत्ति, कला और कौशलकी आवश्यकता है।" विश्वनन्दी अपने इस विचारके अनुसार सांसारिक सुखोंको भोगता हुआ भक्ति, सेवा और संयमकी ओर भी प्रवृत्त रहा । उसका जीवन आदर्श जीवन था। वह विषयभोगोंसे उसी तरह अलिप्त था, जिसप्रकार कमलपत्र जलसे । भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग इन तीनों का समन्वय उसके जीवन में विद्यमान था ।
विश्वभूतिके भाईका नाम विशाखभूति था और विशाखभूतिके पुत्रका नाम विशाखनन्दी । विश्वभूति एक दिन अपनी अट्टालिकापर बैठे हुए मेघोंको सुन्दर आकृतिका अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने सहसा देखा कि वह मेधाकृति वायुके एक मोंकेसे क्षणभरमें छिन्न-भिन्न हो गयी । इस दृश्यके देखनेसे उनको अन्तरात्मा प्रभावित हुई और वे सोचने लगे कि मनुष्य-जन्मको सार्थकता आध्यात्मिक प्राप्तिमें है। यह भव चन्दनके काष्ठके समान है, जिसे क्षर जन्तु कामोपभोग-वासनाओंके कण्डमें दग्धकर अकिचिन प्रयोजनके हेतु नष्ट कर देते हैं, पर जो मननशील हैं, प्रबद्धचेता है; वे इस काष्ठका घर्षण कर सुगन्ध प्राप्त करते हैं और इस गन्धसे अन्तरंग एवं बहिरंगको सप्त कर लेते हैं। यह मनुष्य जन्म किसना महान् है। आज भी अन्य प्राणी उसी पूर्व अवस्थामें हैं, जिसमें अनादिकालमें थे और उनके सभी व्यापार उतने ही सीमित है, जितने पूर्व युगमें थे । मनुष्य ही एक ऐसा भव है, जिसमें अध्यात्म-संपत्तिका विकास संभव होता है । जो इस भवको प्राप्तकर संयम ग्रहण नहीं करता, अहिंसाका आचरण नहीं करता, उसका नर-जन्म पाना सार्थक नहीं है। वस्तुतः इस मनुष्य-जन्मको तप, ज्ञान और चारित्रकी साधना द्वारा सार्थक बनाना ही जीवनका लक्ष्य है। मैंने अबतक मोह और कषायके उदयसे अगणित वर्ष इन सांसारिक विषयोंमें व्यतीत कर दिए हैं । अतएव अब मुझे आत्मकल्याणके लिये प्रवृत्त होना चाहिये ।"
इसप्रकार विचारकर विश्वभूतिने अपने भाई विशाखभूतिको बुलाकर कहा कि मैं अब संसारसे विरत होकर आत्मसाधनाके हेतु श्रमण-दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। अतएव "वत्स ! तुम इस राज्यभारको ग्रहण करो।"
तीर्थकर महावीर और उनको देशना : ३१