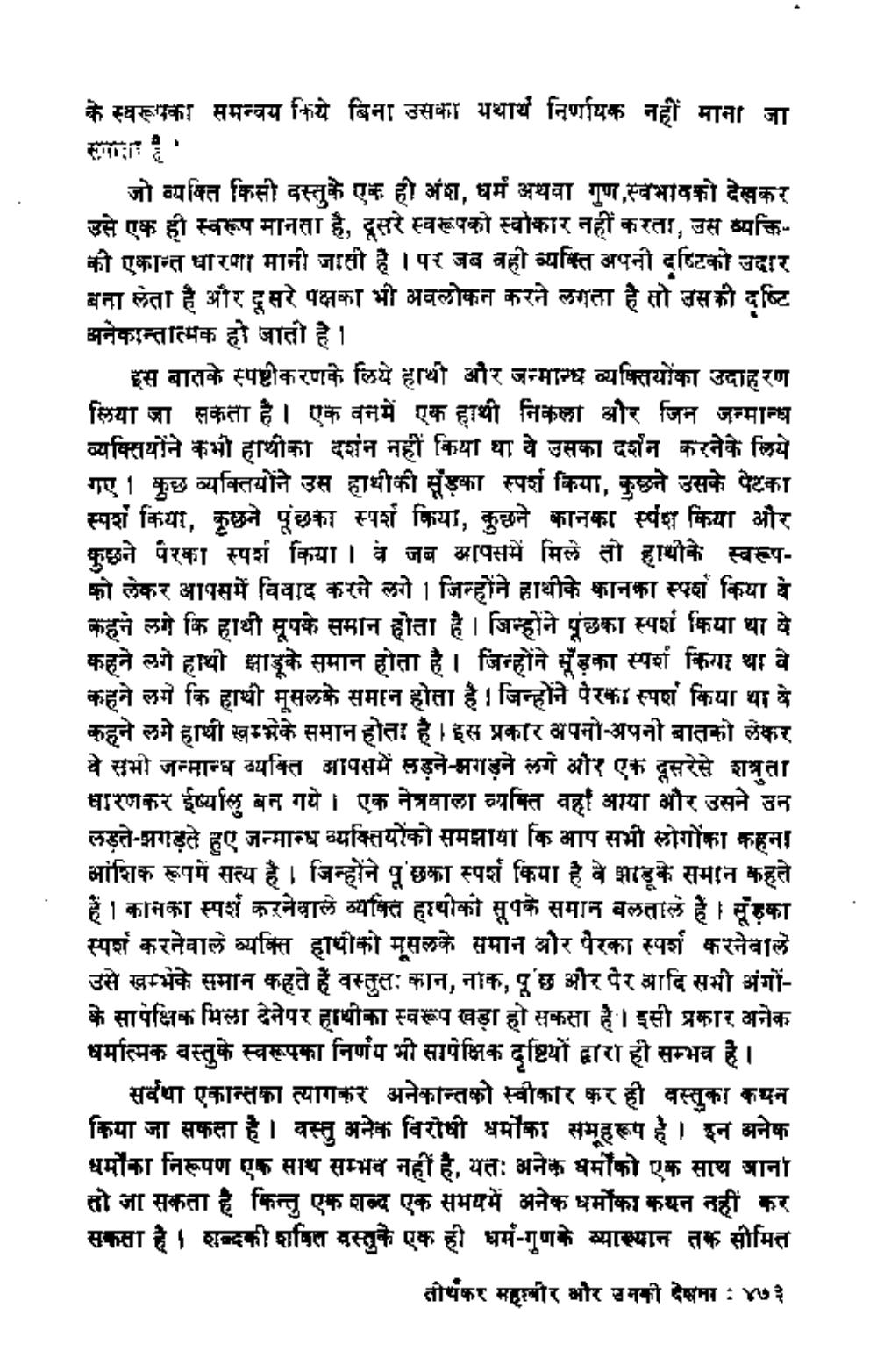________________
के स्वरूपका समन्वय किये बिना उसका यथार्थ निर्णायक नहीं माना जा
है
.
जो व्यक्ति किसी वस्तुके एक ही अंश, धर्म अथवा गुण, स्वभावको देखकर उसे एक ही स्वरूप मानता है, दूसरे स्वरूपको स्वोकार नहीं करता, उस व्यक्तिकी एकान्त धारणा मानी जाती है । पर जब वही व्यक्ति अपनी दृष्टिको उदार बना लेता है और दूसरे पक्षका भी अवलोकन करने लगता है तो उसकी दृष्टि अनेकान्तात्मक हो जाती है ।
1
इस बातके स्पष्टीकरण के लिये हाथी और जन्मान्ध व्यक्तियोंका उदाहरण लिया जा सकता है। एक वनमें एक हाथी निकला और जिन जन्मान्ध व्यक्तियोंने कभी हाथीका दर्शन नहीं किया था वे उसका दर्शन करनेके लिये गए । कुछ व्यक्तियोंने उस हाथी की सूँड़का स्पर्श किया, कुछने उसके पेटका स्पर्श किया, कुछने पूंछका स्पर्श किया, कुछने कानका पेश किया और कुछने परका स्पर्श किया। वे जब आपस में मिले तो हाथोंके स्वरूपको लेकर आपस में विवाद करने लगे । जिन्होंने हाथीके कानका स्पर्श किया ये कहने लगे कि हाथी सूपके समान होता है । जिन्होंने पूछका स्पर्श किया था ये कहने लगे हाथी झाडूके समान होता है। जिन्होंने सूँड़का स्पर्श किया था वे कहने लगे कि हाथी मूसलके समान होता है । जिन्होंने पेरका स्पर्श किया था के कहने लगे हाथी खम्भे के समान होता है। इस प्रकार अपनी-अपनी बातको लेकर वे सभी जन्मान्ध व्यक्ति आपसमें लड़ने अगड़ने लगे और एक दूसरेसे शत्रुता धारणकर ईर्ष्यालु बन गये । एक नेत्रवाला व्यक्ति वहीं आया और उसने उन लड़ते-झगड़ते हुए जन्मान्ध व्यक्तियोंको समझाया कि आप सभी लोगों का कहना आंशिक रूपमें सत्य है । जिन्होंने पूछका स्पर्श किया है वे शाके समान कहते हैं । कानका स्पर्श करनेवाले व्यक्ति हाथीको सूपके समान बलताले हैं। सूँड़का स्पर्श करनेवाले व्यक्ति हाथीको मूसलके समान और पैरका स्पर्श करनेवाले उसे खम्भे के समान कहते हैं वस्तुतः कान, नाक, पूछ और पैर आदि सभी अंगोंके सापेक्षिक मिला देनेपर हाथीका स्वरूप खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार अनेक धर्मात्मक वस्तुके स्वरूपका निर्णय भी सापेक्षिक दृष्टियों द्वारा ही सम्भव है ।
सर्वथा एकान्तका त्यागकर अनेकान्तको स्वीकार कर ही वस्तुका कथन किया जा सकता है । वस्तु अनेक विरोधी धर्मोका समूहरूप है । इन अनेक धर्मोका निरूपण एक साथ सम्भव नहीं है, यतः अनेक धर्मोंको एक साथ जाना सो जा सकता है किन्तु एक शब्द एक समय में अनेक धर्मोका कथन नहीं कर सकता है । शब्दकी शक्ति वस्तुके एक ही धर्म-गुणके व्याख्यान तक सीमित
तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४७३