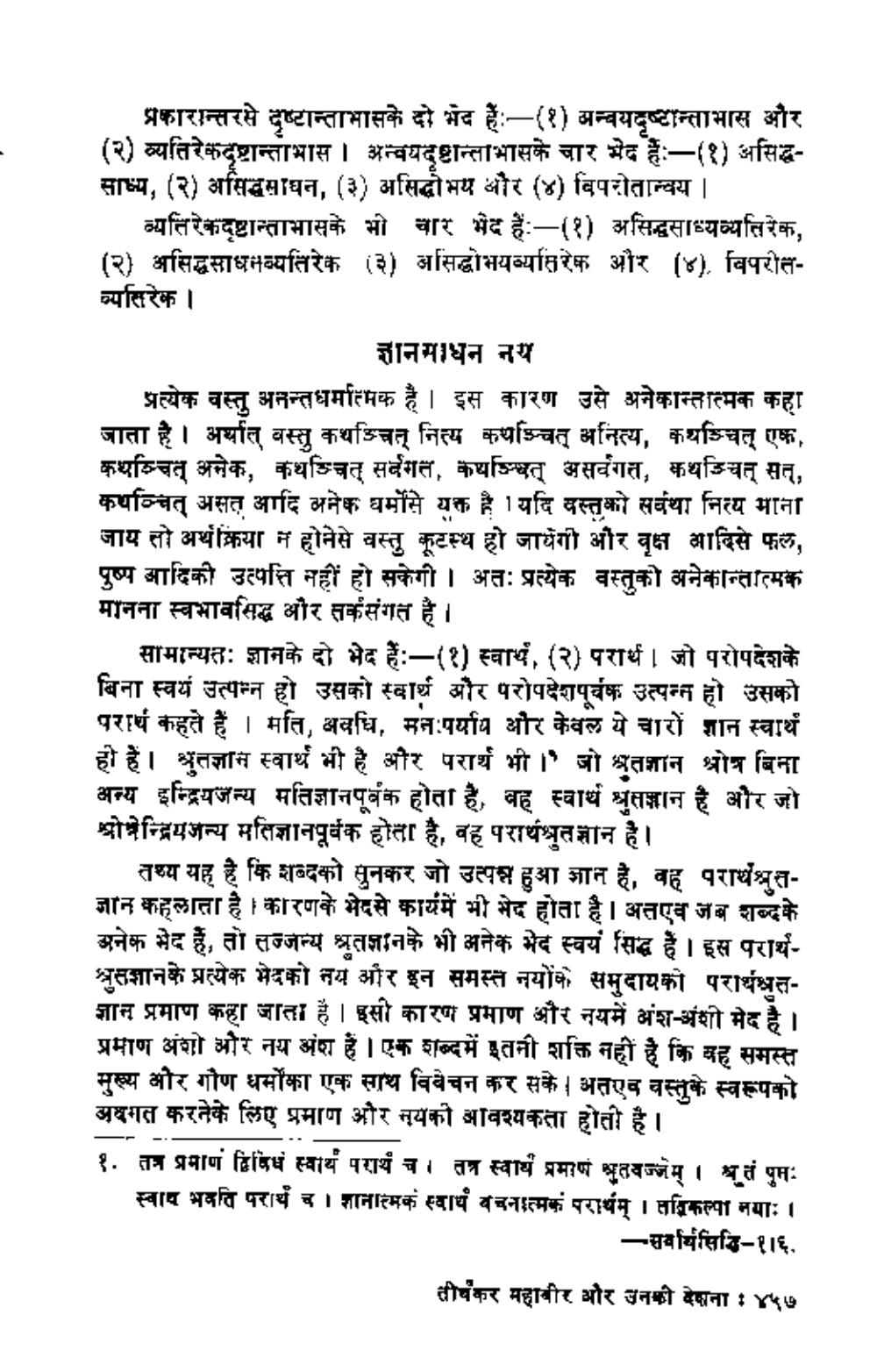________________
प्रकारान्तरसे दृष्टान्ताभासके दो भेद हैं: - (१) अन्वयदृष्टान्ताभास और (२) व्यतिरेकदृष्टान्ताभास । अन्वयदृष्टान्ताभासके चार भेद है: - (१) असिद्धसाध्य, (२) असिद्धसाधन, (३) असिद्धो भय और ( ४ ) विपरीतान्वय |
व्यतिरेकदृष्टान्ताभासके भो चार भेद हैं: - ( १ ) असिद्धसाध्यव्यतिरेक, (२) असिद्धसाधनव्यतिरेक (३) असिद्धोभयव्यतिरेक और ( ४ ) विपरीतव्यतिरेक ।
ज्ञानसाधन नय
+
प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। इस कारण उसे अनेकान्तात्मक कहा जाता है । अर्थात् वस्तु कथञ्चित् नित्य कथञ्चत् अनित्य, कथञ्चित् एक, कथञ्चित् अनेक, कथञ्चित् सर्वगत कथञ्चित् असवंगत कथञ्चित् सत् कथञ्चित् असत् आदि अनेक धर्मोसे युक्त है । यदि वस्तुको सर्वथा नित्य माना जाय तो अर्थक्रिया न होनेसे वस्तु कूटस्थ हो जायेंगी और वृक्ष आदिसे फल, पुष्प आदिकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। अतः प्रत्येक वस्तुको अनेकान्तात्मक मानना स्वभावसिद्ध और तर्कसंगत है।
सामान्यतः ज्ञानके दो भेद हैं: - ( १ ) स्वार्थ, (२) परार्थ । जो परोपदेश के बिना स्वयं उत्पन्न हो उसको स्वार्थ और परोपदेशपूर्वक उत्पन्न हो उसको परार्थं कहते हैं । मति, अवधि, मनःपर्याय और केवल ये चारों ज्ञान स्वार्थ ही हैं । श्रुतज्ञान स्वार्थ भी है और परार्थ भी ।" जो श्रुतज्ञान श्रोत्र बिना अन्य इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक होता है, वह स्वार्थ श्रुतज्ञान है और जो श्रीरेन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक होता है, वह परार्थश्रुतज्ञान है।
तथ्य यह है कि शब्दको सुनकर जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है, वह परार्थश्रुतज्ञान कहलाता है। कारणके भेद से कार्यमें भी भेद होता है। अतएव जब शब्द के अनेक भेद है, तो तज्जन्य श्रुतज्ञानके भी अनेक भेद स्वयं सिद्ध हैं । इस परार्थश्रुतज्ञान के प्रत्येक भेदको नय और इन समस्त नयोंके समुदायको परार्थश्रुतज्ञान प्रमाण कहा जाता है । इसी कारण प्रमाण और नयमें अंश अंशी मेद है । प्रमाण अंशो और नय अंश हैं । एक शब्दमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह समस्त मुख्य और गौण धर्मोका एक साथ विवेचन कर सके। अतएव वस्तुके स्वरूपको अवगत करनेके लिए प्रमाण और नयको आवश्यकता होती है ।
१. तत्र प्रमाणं द्विविधं स्वायं परार्थं च । तत्र स्वायं प्रमाणं श्रुतवज्जेम् । श्रुतं पुमः स्वाय भवति परार्थं च । ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम् । तद्विकल्पा नयाः । - सर्वार्थसिद्धि - १६.
तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना : ४५७