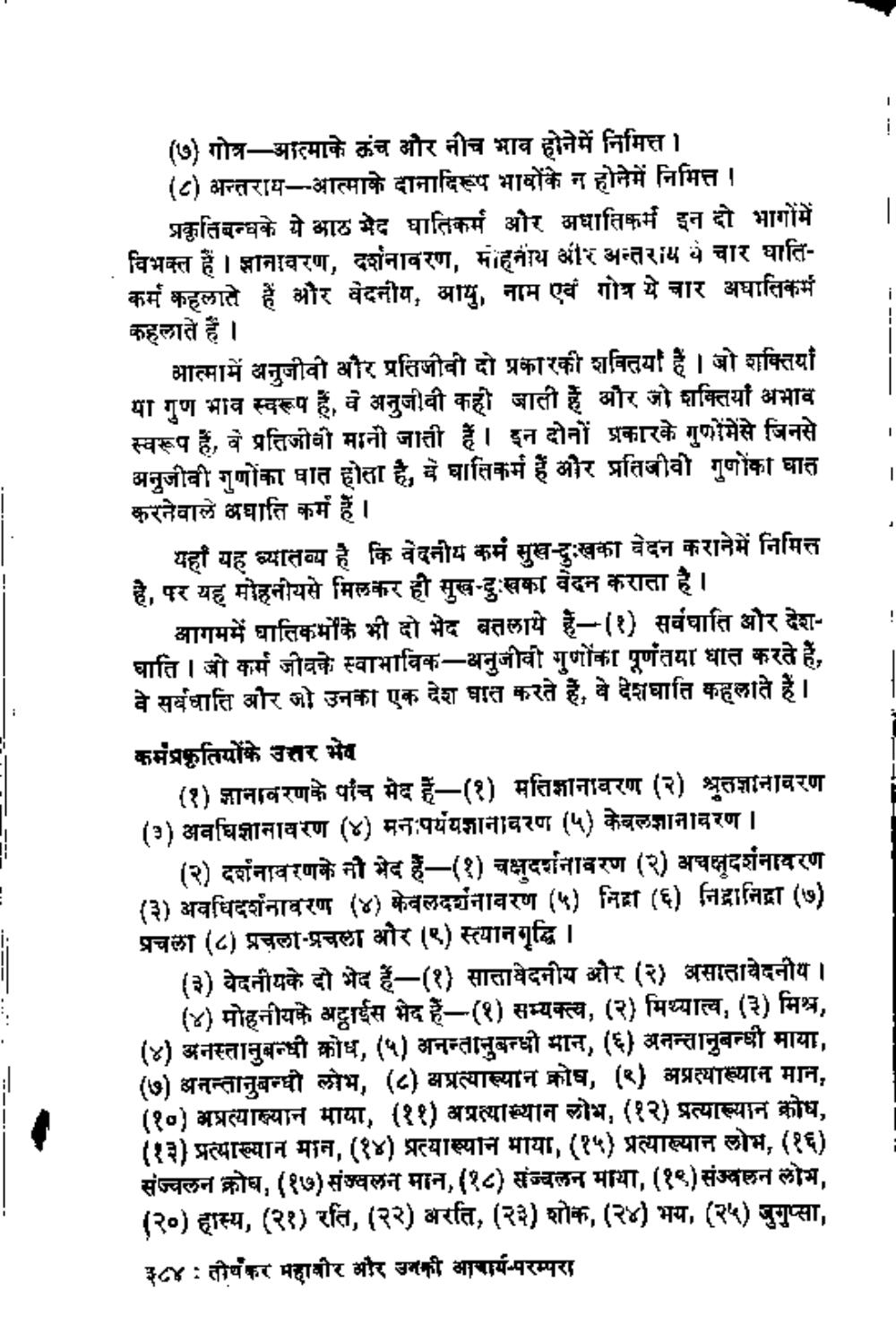________________
(७) गोत्र – आत्माके ऊंच और नीच भाव होने में निमित्त । (८) अन्तराय - आत्माके दानादिरूप भावोंके न होनेमें निमित्त ।
प्रकृतिबन्धके ये आठ भेद घातिकर्म और अधातिकर्म इन दो भागों में विभक्त हैं । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय के चार घातिकर्म कहलाते हैं और वेदनीय, आयु, नाम एवं गोत्र ये चार अघातिकर्म कहलाते हैं ।
आत्मामें अनुजीवी और प्रतिजीवी दो प्रकारकी शक्तियाँ हैं । जो शक्तियाँ या गुण भाव स्वरूप हैं, वे अनुजीवी कही जाती है और जो शक्तियाँ अभाव स्वरूप हैं, वे प्रतिजीवी मानी जाती हैं। इन दोनों प्रकारके गुणोंमेंसे जिनसे अनुजीवी गुणोंका घात होता है, वे घातिकर्म हैं और प्रतिजीवी गुणोंका घात करनेवाले अघाति कर्म हैं ।
यहाँ यह व्यातव्य है कि वेदनीय कर्म सुख-दुःखका वेदन कराने में निमित्त है, पर यह मोहनीयसे मिलकर ही सुख-दुःखका वेदन कराता है ।
I
आगममें घातिकर्मो के भी दो भेद बतलाये है - (१) सर्वघाति और देशघाति । जो कर्म जीवके स्वाभाविक - अनुजीवी गुणोंका पूर्णतया घात करते हैं, वे सर्वधाति और जो उनका एक देश घात करते हैं, वे देशघाति कहलाते हैं । कर्मप्रकृतियोंके उत्तर भेव
(१) ज्ञानावरण के पांच मेद हैं- (१) मतिज्ञानावरण (२) श्रुतज्ञानावरण ( 3 ) अवधिज्ञानावरण (४) मन:पर्ययज्ञानावरण (५) केवलज्ञानावरण |
(२) दर्शनावरणके नौ भेद हैं- (१) चक्षुदर्शनावरण (२) अचक्षुदर्शनावरण (३) अवधिदर्शनावरण (४) केवलदर्शनावरण (५) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (८) प्रचलाप्रचला और ( ९ ) स्त्यानगृद्धि ।
(३) वेदनीयके दो भेद हैं- (१) सातावेदनीय और (२) असातावेदनीय |
(४) मोहनीय अट्ठाईस भेद हैं- ( १ ) सम्यक्त्य, (२) मिथ्यात्व (३) मिश्र, (४) अनस्तानुबन्धी क्रोध, (५) अनन्तानुबन्धी मान, (६) अनन्तानुबन्धी माया, (७) अनन्तानुबन्धी लोभ, (८) अप्रत्याख्यान क्रोध, (९) अप्रत्याख्यान मान, (१०) अप्रत्याख्यान माया, (११) अप्रत्याख्यान लोभ, (१२) प्रत्याख्यान क्रोध, (१३) प्रत्याख्यान मान, (१४) प्रत्याख्यान माया, (१५) प्रत्याख्यान लोभ, (१६) संज्वलन क्रोध, (१७) संज्वलन मान, (१८) संञ्चलन माया, (१९) संज्वलन लोभ, (२०) हास्य, (२१) रति, (२२) अरति, (२३) शोक, (२४) भय, (२५) जुगुप्सा, ३८४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा
1
T
i
1
+