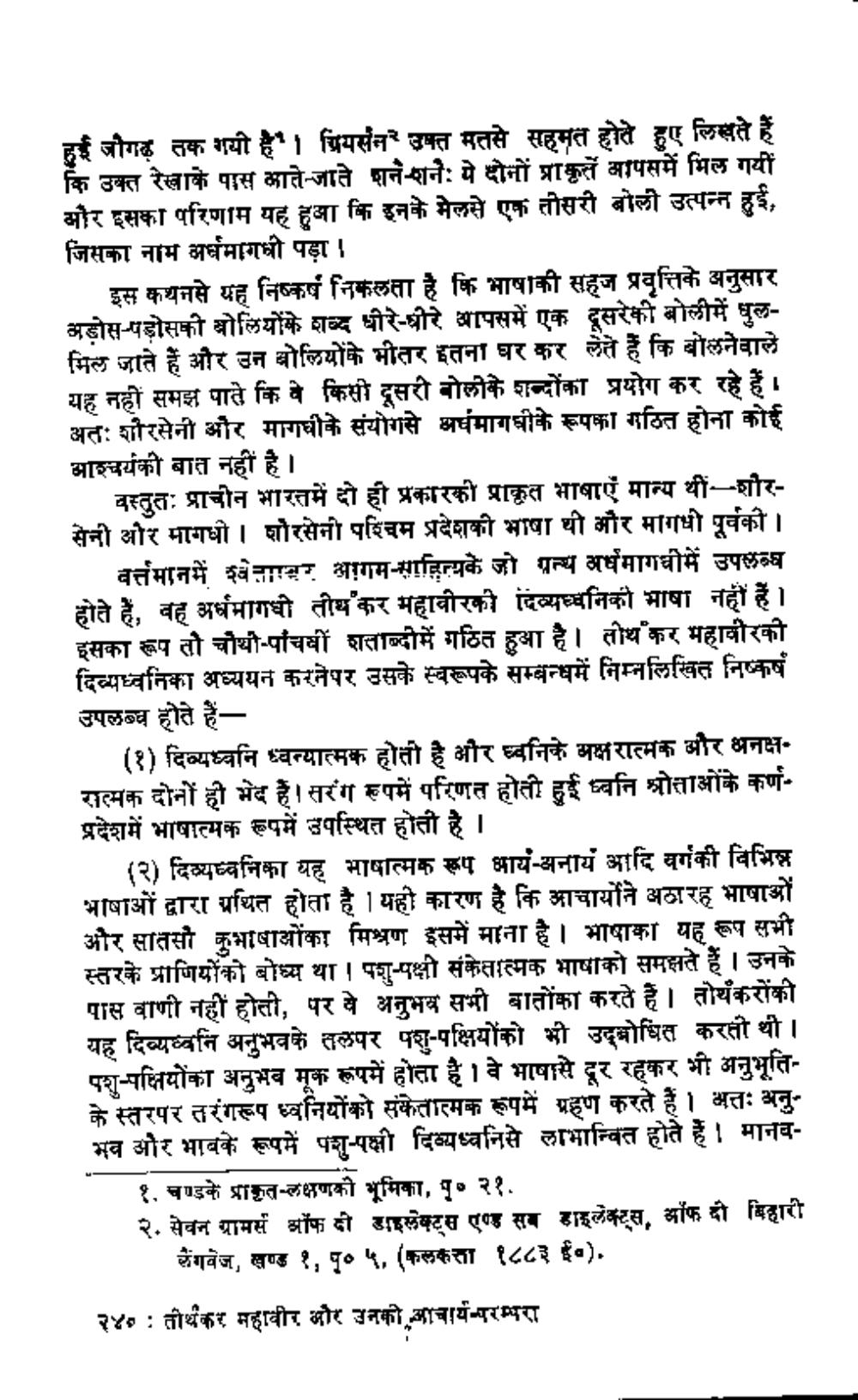________________
हुई जोगढ़ तक गयी है। ग्रियर्सन उक्त मतसे सहमत होते हुए लिखते हैं कि उक्त रेखाके पास आते-जाते शन-शनैः ये दोनों प्राकृतें आपसमें मिल गयीं और इसका परिणाम यह हुआ कि इनके मेलसे एक तीसरी बोली उत्पन्न हुई, जिसका नाम अर्धमागधी पड़ा।
इस कथनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषाकी सहज प्रवृत्तिके अनुसार अड़ोस-पड़ोसकी बोलियोंके शब्द धीरे-धीरे आपसमें एक दूसरेकी बोलीमें धुलमिल जाते हैं और उन बोलियों के भीतर इतना घर कर लेते हैं कि बोलनेवाले यह नहीं समझ पाते कि वे किसी दूसरी बोलीके शन्दोंका प्रयोग कर रहे हैं। अतः शौरसेनी और मागधी के संयोगसे अर्धमागधीके रूपका गठित होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।
वस्तुतः प्राचीन भारतमें दो ही प्रकारको प्राकृत भाषाएं मान्य थीं-शौरसेनी और मागधी । शौरसेनी पश्चिम प्रदेशको भाषा थी और मागधी पूर्वको।
वर्तमानमें श्वेताकर आगम-साहित्यके जो ग्रन्थ अर्धमागधीमें उपलब्ध होते हैं, वह अर्धमागधी तीर्थकर महावीरकी दिव्यध्वनिकी भाषा नहीं हैं। इसका रूप तो चौथी-पांचवीं शताब्दीमें गठित हुआ है। तीर्थ कर महावीरकी दिव्यध्वनिका अध्ययन करनेपर उसके स्वरूपके सम्बन्धमें निम्नलिखित निष्कर्ष उपलब्ध होते हैं
(१) दिव्यध्वनि ध्वन्यात्मक होती है और ध्वनिके अक्षरात्मक और अनक्ष. रात्मक दोनों ही भेद हैं। सरंग रूपमें परिणत होती हुई ध्वनि श्रोताओंके कर्णप्रदेशमें भाषात्मक रूपमें उपस्थित होती है ।
(२) दिव्यध्वनिका यह भाषात्मक रूप आर्य-अनार्य आदि वर्गकी विभिन्न भाषाओं द्वारा ग्रथित होता है । यही कारण है कि आचार्योने अठारह भाषाओं और सातसो कुभाषाओंका मिश्रण इसमें माना है। भाषाका यह रूप सभी स्तरके प्राणियोंको बोध्य था । पशु-पक्षी संकेतात्मक भाषाको समझते हैं । उनके पास वाणी नहीं होती, पर वे अनुभव सभी बातोंका करते हैं। तोर्थंकरोंकी यह दिव्यध्वनि अनुभवके तलपर पशु-पक्षियोंको भी उद्बोधित करती थी । पशु-पक्षियोंका अनुभव मूक रूपमें होता है। वे भाषासे दूर रहकर भी अनुभूतिके स्तरपर तरंगरूप ध्वनियोंको संकेतात्मक रूपमें ग्रहण करते हैं। अतः अनुभव और भाबके रूपमें पशु-पक्षी दिव्यध्वनिसे लाभान्वित होते हैं। मानव
१. चण्डके प्राकृत-लक्षणको भूमिका, पु. २१. २. सेवन ग्रामर्स ऑफ दी इलेक्ट्स एण्ड सब हाइलेक्ट्स, ऑफ दी बिहारी
लैंगवेज, खण्ड १, पृ० ५, (कलकत्ता १८८३ ई०). २४० : तीर्थकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा