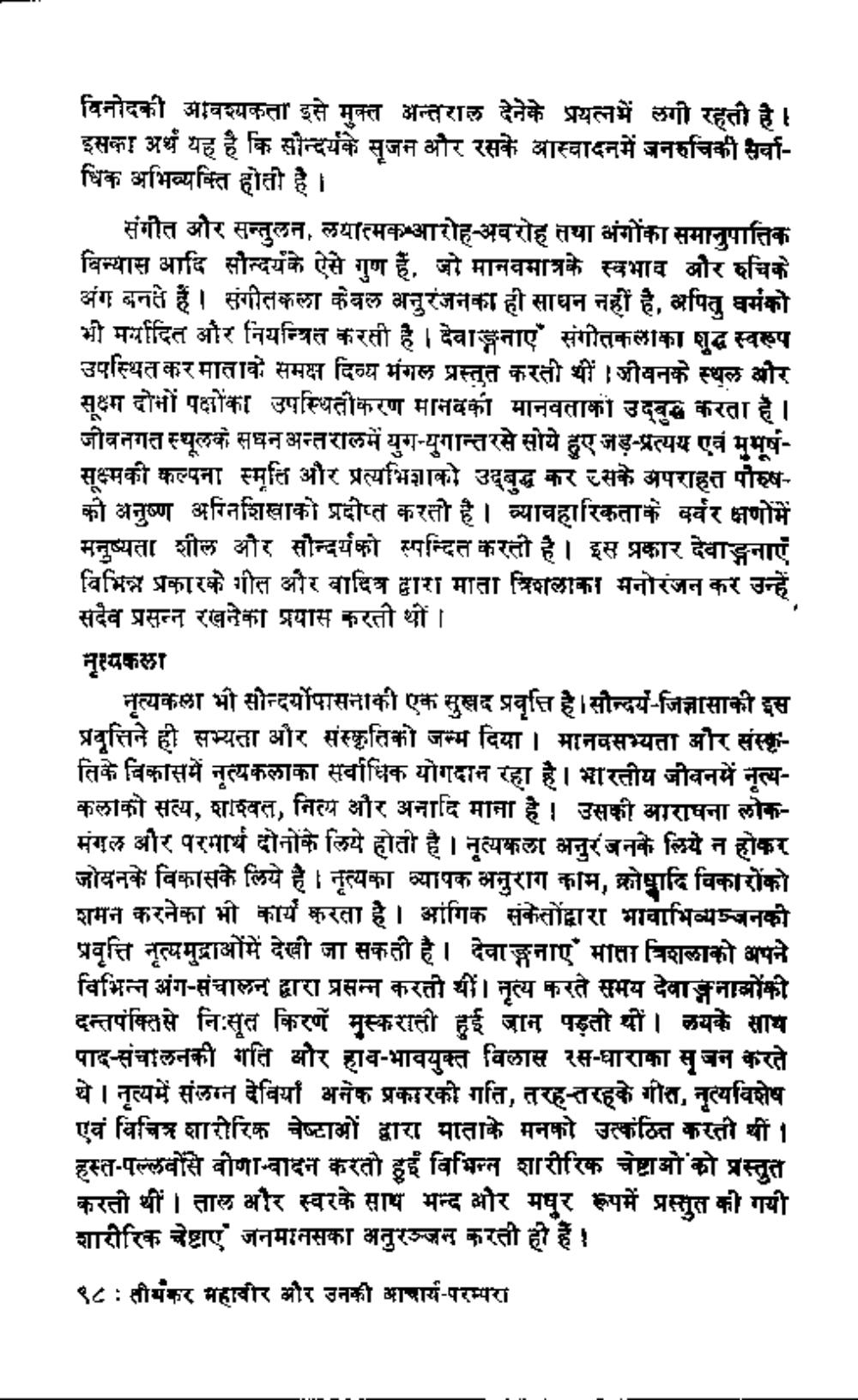________________
विनोदकी आवश्यकता इसे मुक्त अन्तराल देनेके प्रयत्नमें लगी रहती है। इसका अर्थ यह है कि सौन्दर्यके सृजन और रसके आस्वादनमें जनरुचिकी सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है।
संगीत और सन्तुलन, लयात्मक आरोह-अवरोह तथा अंगोंका समानुपातिक विन्यास आदि सौन्दर्यके ऐसे गुण हैं, जो मानवमात्रके स्वभाव और चिके अंग बनते हैं। संगीतकला केवल अनुरंजनका ही साधन नहीं है, अपितु धर्मको भी मर्यादित और नियन्त्रित करती है । देवाङ्गनाएँ संगीतकलाका शुद्ध स्वरूप उपस्थित कर माताके समक्ष दिव्य मंगल प्रस्तुत करती थीं । जीवनके स्थल और सूक्ष्म दोनों पक्षोंका उपस्थितीकरण मानवकी मानवताका उबुर करता है । जीवनगत स्थूलको सघन अन्तरालमें युग-युगान्तरसे सोये हुए जड़-प्रत्यय एवं मुमूर्षसूक्ष्मकी कल्पना स्मृत्ति और प्रत्यभिशाको उद्बद्ध कर उसके अपराहत पौरुषको अनुष्ण अग्निशिखाको प्रदीप्त करती है। व्यावहारिकताके वर्वर क्षणोंमें मनुष्यता शील और सौन्दर्यको स्पन्दित करती है। इस प्रकार देवाङ्गनाएं विभिन्न प्रकारके गीत और वादित्र द्वारा माता त्रिशलाका मनोरंजन कर उन्हें सदैव प्रसन्न रखनेका प्रयास करती थीं। नृत्यकला
नृत्यकला भी सौन्दर्योपासनाकी एक सुखद प्रवृत्ति है। सौन्दर्य-जिज्ञासाकी इस प्रवृत्तिने ही सभ्यता और संस्कृतिको जन्म दिया। मानवसभ्यता और संस्कृतिके विकासमें नृत्यकलाका सर्वाधिक योगदान रहा है। भारतीय जीवनमें नृत्यकलाको सत्य, शाश्वत, नित्य और अनादि माना है। उसकी आराधना लोकमंगल और परमार्थ दोनोंके लिये होती है। नत्यकला अनुरंजनके लिये न होकर जोबनके विकासके लिये है । नृत्यका व्यापक अनुराग काम, क्रोधादि विकारोंको शमन करनेका भी कार्य करता है। आंगिक संकेतोंद्वारा भावाभिव्यजनकी प्रवृत्ति नृत्यमुद्राओंमें देखी जा सकती है। देवाङ्गनाएं माता त्रिशलाको अपने विभिन्न अंग-संचालन द्वारा प्रसन्न करती थीं। नृत्य करते समय देवाङ्गनाओंकी दन्तपंक्तिसे नि:सूत किरणें मुस्कराती हुई जान पड़ती थीं। लयके साथ पाद-संचालनकी गति और हाव-भावयुक्त विलास रस-धाराका सृजन करते थे । नृत्यमें संलग्न देवियाँ अनेक प्रकारको गति, तरह-तरहके गीत, नृत्यविशेष एवं विचित्र शारीरिक चेष्टाओं द्वारा माताके मनको उत्कंठित करती थीं। हस्त-पल्लवोंसे वीणा-वादन करतो हुई विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं को प्रस्तुत करती थीं । ताल और स्वरके साथ मन्द और मधुर रूपमें प्रस्तुत की गयी शारीरिक चेष्टाएं जनमानसका अनुरञ्जन करती ही हैं। ९८ : तीयंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा