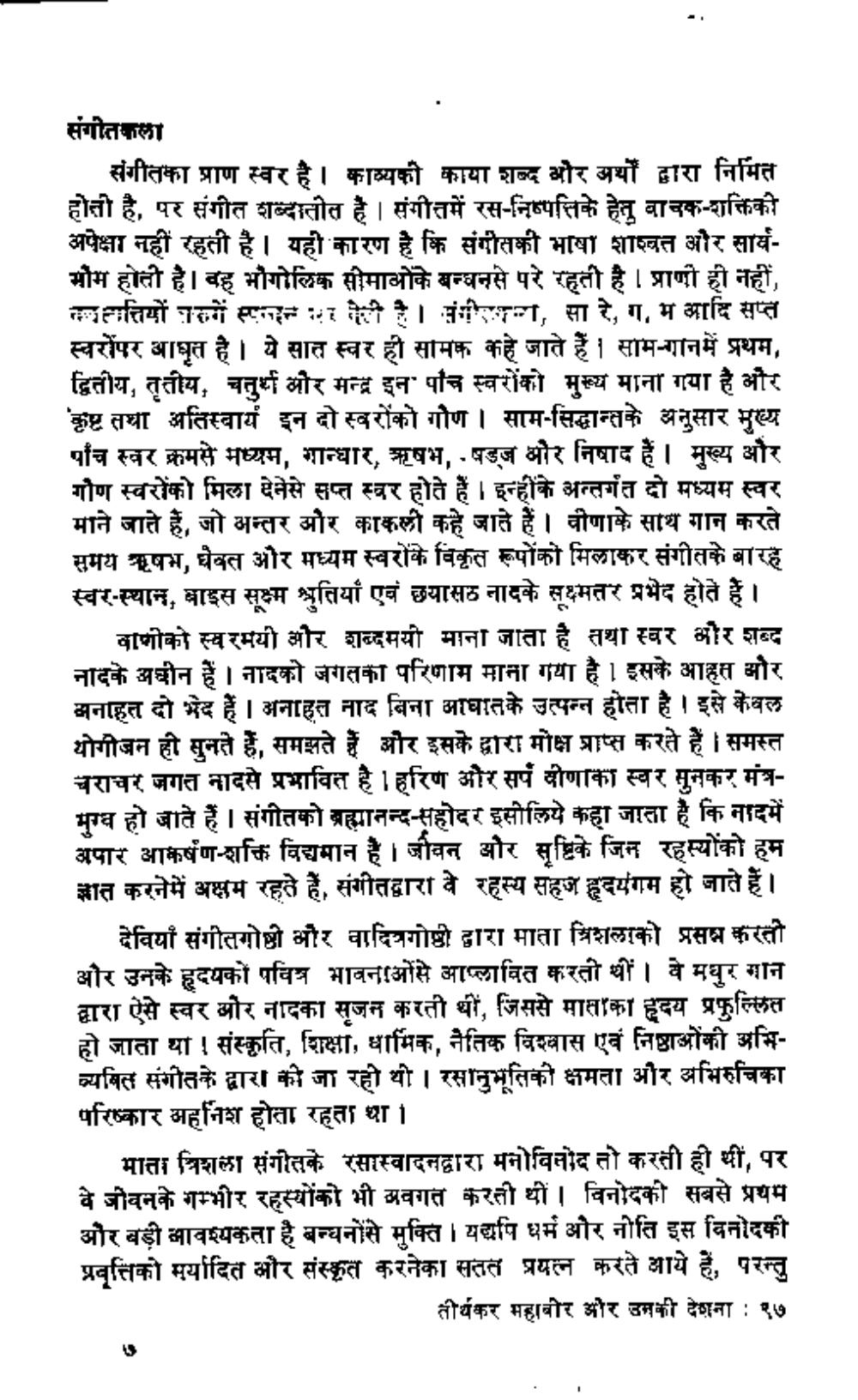________________
संगीतकला
I
संगीतका प्राण स्वर है । काव्यकी काया शब्द और अर्थों द्वारा निर्मित होती है, पर संगीत शब्दातीत है । संगीतमें रस - निष्पत्तिके हेतु वाचक-शक्तिकी अपेक्षा नहीं रहती है । यही कारण है कि संगीतकी भाषा शास्त्रत और सार्वम होती है । वह भौगोलिक सीमाओंके बन्धनसे परे रहती है । प्राणी ही नहीं, पत्तियों में भी है। सा रे, ग, म आदि सप्त स्वरोंपर आधृत है । ये सात स्वर ही सामक कहे जाते हैं । साम-गान में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ओर मन्द्र इन पाँच स्वरोंको मुख्य माना गया है और 'कृष्ट तथा अतिस्वायं इन दो स्वरोंको गौण । साम - सिद्धान्त के अनुसार मुख्य पाँच स्वर क्रमसे मध्यम, गान्धार, ऋषभ - षड्ज और निषाद हैं। मुख्य और गौण स्वरोंको मिला देनेसे सप्त स्वर होते हैं । इन्होंके अन्तर्गत दो मध्यम स्वर माने जाते हैं, जो अन्तर और काकली कहे जाते हैं । वीणाके साथ गान करते समय ऋषभ, धैवत और मध्यम स्वरोंके विकृत रूपों को मिलाकर संगीतके बारह स्वर- स्थान, बाइस सूक्ष्म श्रुतियाँ एवं छयासठ नादके सूक्ष्मतर प्रभेद होते हैं ।
वाणीको स्वरमयी और शब्दमयी माना जाता है तथा स्वर और शब्द नादके अधीन हैं। नादको जगतका परिणाम माना गया है। इसके आहत और मनात दो भेद हैं । अनाहत नाद बिना आघात के उत्पन्न होता है। इसे केवल योगीजन ही सुनते हैं, समझते है और इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं । समस्त चराचर जगत नादसे प्रभावित है । हरिण और सर्प वीणाका स्वर सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं । संगीतको ब्रह्मानन्द-सहोदर इसीलिये कहा जाता है कि नादमें अपार आकर्षण शक्ति विद्यमान है। जीवन और सृष्टिके जिन रहस्योंको हम ज्ञात करनेमें अक्षम रहते हैं, संगीतद्वारा वे रहस्य सहज हृदयंगम हो जाते हैं ।
देवियां संगीतगोष्ठी और वादित्रगोष्ठी द्वारा माता त्रिशलाको प्रसन्न करती और उनके हृदयको पवित्र भावनाओंसे आप्लावित करती थीं। वे मधुर मान द्वारा ऐसे स्वर और नादका सृजन करती थीं, जिससे माताका हृदय प्रफुल्लित हो जाता था ! संस्कृति, शिक्षा, धार्मिक, नैतिक विश्वास एवं निष्ठाओं की अभिव्यक्ति संगीत के द्वारा की जा रही थी । रसानुभूतिको क्षमता और अभिरुचिका परिष्कार अनेश होता रहता था ।
माता त्रिशला संगीतके रसास्वादनद्वारा मनोविनोद तो करती ही थीं, पर वे जीवन के गम्भीर रहस्यों को भी अवगत करती थीं। विनोदकी सबसे प्रथम और बड़ी आवश्यकता है बन्धनों से मुक्ति । यद्यपि धर्म और नीति इस विनोदकी प्रवृत्तिको मर्यादित और संस्कृत करनेका सतत प्रयत्न करते आये हैं, परन्तु तीर्थंकर महावीर और उनकी देशना ९७
७