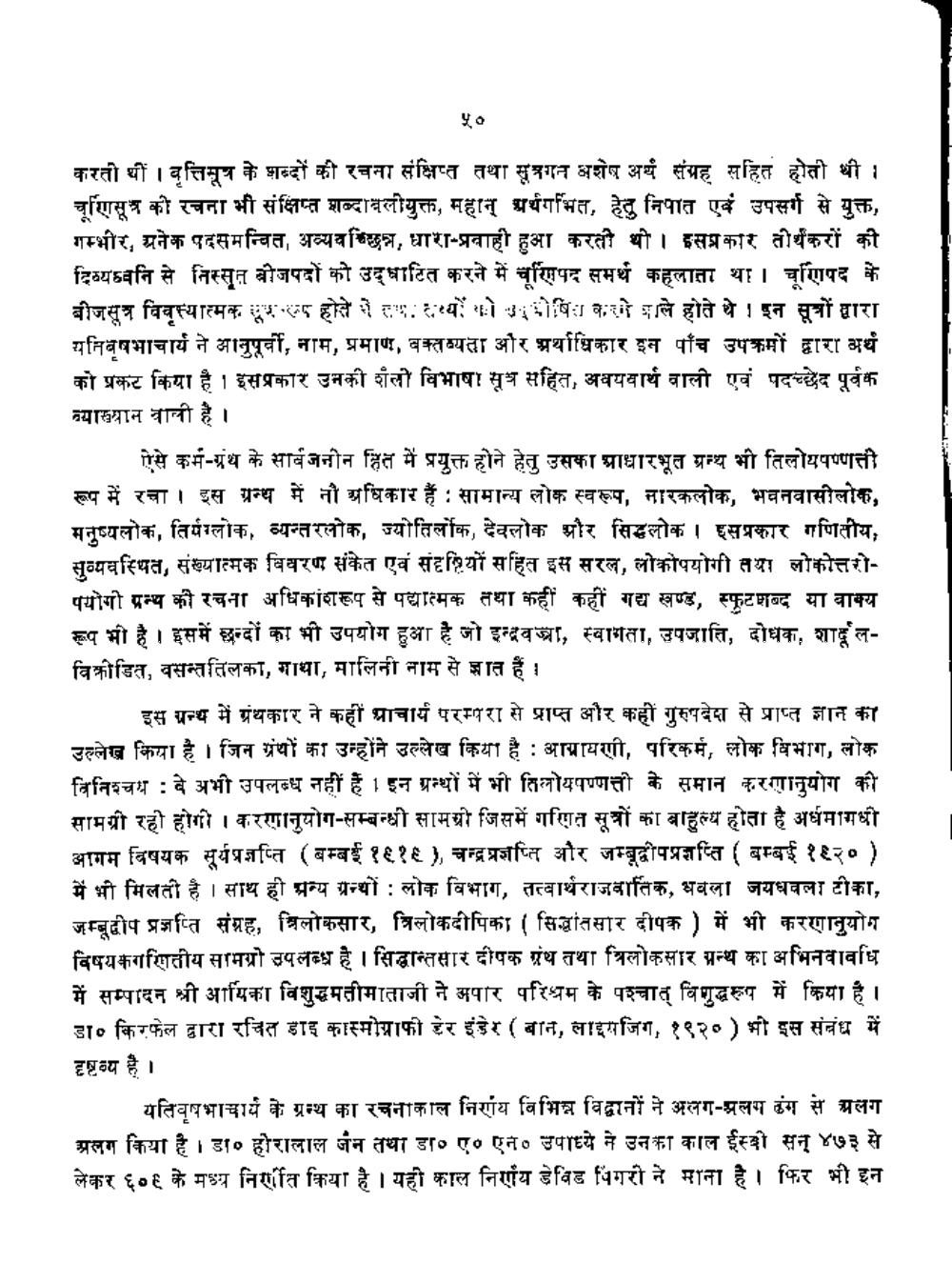________________
करती थीं । वृत्तिमूत्र के शब्दों की रचना संक्षिप्त तथा सूत्रगत अशेष अर्थ संग्रह सहित होती थी। चूणिसूत्र की रचना भी संक्षिप्त शब्दाबलीयुक्त, महान् अर्थभित, हेतु निपात एवं उपसर्ग से युक्त, गम्भीर, अनेक पदसमन्वित, अव्यवच्छिन्न, धारा-प्रवाही हुआ करती थी। इसप्रकार तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि से निस्सृत बीजपदों को उद्घाटित करने में चूणिपद समर्थ कहलाता था। चूणिपद के बीजसूत्र विवृत्यात्मक सुबह होते में रण. श्यों को कोषिः। कालो भाले होते थे । इन सूत्रों द्वारा यनिवृषभाचार्य ने आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार इन पाँच उपक्रमों द्वारा अर्थ को प्रकट किया है । इसप्रकार उनकी शैली विभाषा सूत्र सहित, अवययार्थ वाली एवं पदच्छेद पूर्वक व्याख्यान वाली है।
ऐसे कर्म-ग्रंथ के सार्वजनीन हित में प्रयुक्त होने हेतु उसका प्राधारभूत ग्रन्थ भी तिलोयपण्णत्ती रूप में रचा। इस ग्रन्थ में नौ अधिकार हैं : सामान्य लोक स्वरूप, नारकलोक, भवनवासीलोक, मनुष्यलोक, तिर्यग्लोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिर्लोक, देवलोक और सिद्धलोक । इसप्रकार गणितीय, सुव्यवस्थित, संख्यात्मक विवरण संकेत एवं संदृष्टियों सहित इस सरल, लोकोपयोगी तथा लोकोत्तरोपयोगी अन्य की रचना अधिकांशरूप से पद्यात्मक तथा कहीं कहीं गद्य स्खण्ड, स्फुट शब्द या वाक्य रूप भी है। इसमें छन्दों का भी उपयोग हुआ है जो इन्द्रवज्रा, स्वागता, उपजाति, दोधक, शार्दूलविक्रीडित, बसन्ततिलका, गाथा, मालिनी नाम से ज्ञात हैं ।
इस ग्रन्थ में ग्रंथकार ने कहीं प्राचार्य परम्परा से प्राप्त और कहीं गुरुपदेश से प्राप्त ज्ञान का उल्लेख किया है । जिन ग्रंथों का उन्होंने उल्लेख किया है : आग्रायणी, परिकर्म, लोक विभाग, लोक विनिश्चय : वे अभी उपलब्ध नहीं हैं 1 इन ग्रन्थों में भी तिलोयपण्णत्ती के समान करणानुयोग की सामग्री रही होगी । कररणानुयोग-सम्बन्धी सामग्री जिसमें गरिणत सूत्रों का बाहुल्य होता है अर्धमागधी आगम विषयक सूर्यप्रज्ञप्ति (बम्बई १६१६ ), चन्द्रप्रज्ञप्ति और जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ( बम्बई १९२०) में भी मिलती है । साथ ही अन्य ग्रन्थों : लोक विभाग, तत्वार्थराजवातिक, धवला जयधवला टीका, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति संग्रह, त्रिलोकसार, त्रिलोकदीपिका ( सिद्धांतसार दीपक ) में भी करणानुयोग विषयकगणितीय सामग्री उपलब्ध है । सिद्धान्तसार दीपक ग्रंथ तथा त्रिलोकसार ग्रन्थ का अभिनवावधि में सम्पादन श्री आर्यिका विशुद्धमतीमाताजी ने अपार परिश्रम के पश्चात् विशुद्धरूप में किया है । डा० किरफेल द्वारा रचित डाइ कास्मोग्राफी देर इंडेर ( बान, लाइयजिग, १९२०) भी इस संबंध में दृष्टव्य है।
यतिवृषभाचार्य के ग्रन्थ का रचनाकाल निर्णय विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग ढंग से अलग अलग किया है । डा. होरालाल जैन तथा डा० ए० एन० उपाध्ये ने उन का काल ईस्वी सन् ४७३ से लेकर ६०६ के मध्य निर्णीत किया है । यही काल निर्णय डेविड पिंगरी ने माना है। फिर भी इन