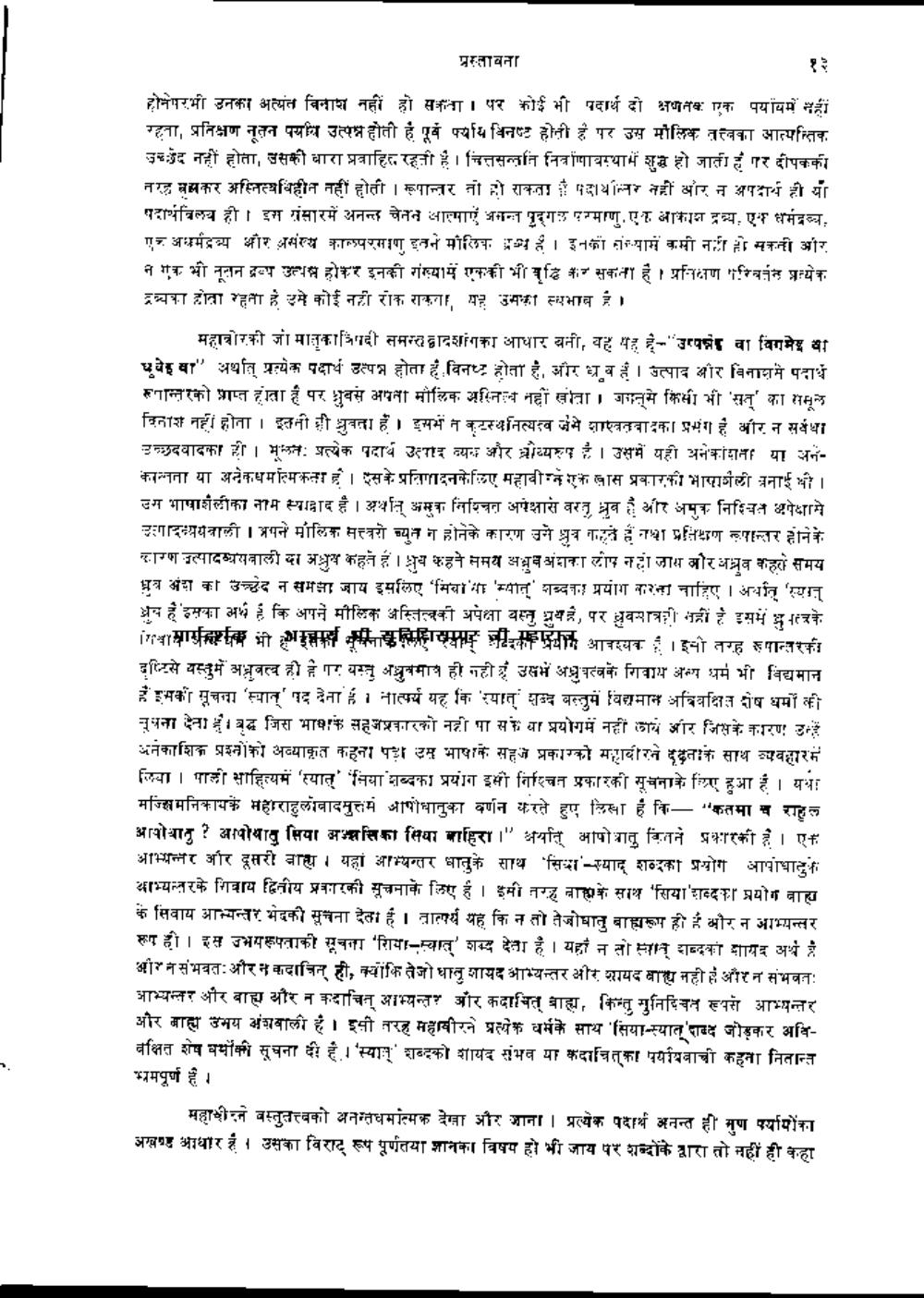________________
प्रस्तावना
होनेपर भी उनका अत्यंत विनाश नहीं हो सकता। पर कोई भी पदार्थ दो अपनः एक पर्याय में नहीं रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्याय उत्पन्न होती है पूर्व पर्याय विनष्ट होती है पर उस मौलिक तत्वका आत्यन्तिक इच्छेद नहीं होता, उसकी धारा प्रवाहित रहती है। चित्तसन्तति निर्वाणावस्थामें शुद्ध हो जाती है पर दीपककी नरहवाकर अस्तित्वविहीन नहीं होती । रूपान्तर तो हो सकता पदाला नहीं और न अपदार्थ ही या पदार्थविलय ही। इस गंसारमें अनन्त चेनन आत्माएं अगन्न पुद्गर परमाणु. एक आकाश द्रव्य, एम धर्मद्रब्ब, एक अधर्मद्रव्य और असंख्य कालपरमाण इतने मालिब यहै। इनका सयाम कमी नही मानी और नगक भी नुतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी गंण्याम एककी भी यदि सकता है। प्रतिक्षण परिवर्तन प्रत्येक द्रव्यत्रा होता रहता है इसे कोई नहीं रोक राकगा, यह उसका स्वभाव है।
महानोरकी जो मालकात्रिपदी समन्स द्वादशांगका आधार बनी, वह यह है-"उत्पन्न वा विगमेन का घवेहवा' अर्थात प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है विनष्ट होता है, और ध्र व है । उत्पाद और विनाशमे पदार्थ रूपान्तरको प्राप्त होता है पर भुवस अपना मौलिक अस्तित्व नहीं खाता। जगन्मे किसी भी 'सत्' का समूल विनाश नहीं होता। इतनीधी ध्रुवता हैं। इसमें न कुटनित्यत्व जैसे शास्त्रतवादका प्रमंग है और न सर्वथा उन्छदवादका ही। मलन: प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्या और धीच्यरूप है। उसमें यही अनेकांना या अनकान्नता या अनेकधर्मात्मकता है। इसके प्रतिपादनकलिए महावीन्न एक खास प्रकारको भाराशैली बनाई थी। उस भाषाशैलीका नाम स्यावाद है। अर्थात अमत्र निश्चित अपेशास वरत भ्रूव है और अमत्र निश्चित अपेक्षामे उल्गादत्ययवाली । अपने मालिक मत्त्तरो न्युन न होनेके कारण उने प्रव नाहते हैं नया प्रतिक्षण रूपान्तर होने के कारण उत्पादध्ययनाली वा अध्रप कहते हैं। श्रवकहने समय अनव अंगाका लोप नही जाय और अन्नव कहते समय ध्रुव अंदा का उच्छेद न समझा जाय इसलिए "मिया या 'म्यात् शब्दका प्रयोग नारना नाहिए । अर्थात् 'स्मन् ध्रुव है इसका अर्थ है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा बस्तु प्रय है, पर प्रवरात्री नहीं है इसमपत्रके iगवायाबाहक भी इसका नाइलाहारका जादका प्रयोग आवश्यक । इसी तरह रूपान्तरकी दृष्टि से यस्तु में अध्रुवत्त्व ही है पर यम्त अध्रुवमात्र ही नही उसमें अध्रुवत्वके गिवाय अन्य धर्म भी विद्यमान है इसकी सूचना 'स्यान्' पद देना है। नात्पर्य यह कि स्यात् शब्द बस्तुम विद्यमान अविवक्षित शेष धमों की नुमना देनाईबद्ध जिस भाषा सहजप्रकारको नहीं पा सके या प्रयोगमं नहीं लाये और जिसके कारण उन्हें अनेकाशिक प्रश्नों को अव्याकृत कहना पड़ा उस भाषाके सहजै प्रकारको महावीरने दृढताके साथ व्यवहार लिया । पाली साहित्यम 'स्यात् निया शब्दका प्रयोग इसौं निश्चित प्रकारकी सुचनाके लिए हुआ है। यथा मज्झिमनिकायके महाराहुलोबादमुत्तमं आपोधानुका वर्णन करते हुए लिखा है कि- "कतमा च राहुल आपोवानु? अपोयातु सिया अससिका सिया बाहिरा।" अर्यात आपोत्रातु जिनन प्रकारकी है। एक आभ्यन्तर और दूसरी बाय । यहां आभ्यन्तर धातुके साथ 'सिया'-याद् शब्दका प्रयोग आपाधादुर याभ्यन्तरके गिवाय द्वितीय प्रनारकी सुचनाके लिए है । इमी तरह नाम के साथ 'सिया'शब्दका प्रयोग बाह्य के सिवाय आभ्यन्तर भेदकी सूचना देता है। तात्पर्य यह कि न तो तेजोधात बाह्यरूप ही है और न आभ्यन्तर हाही। इस उभयरूपताकी सूचना "शिया-स्यात्' शब्द देता है। यहाँ न तो स्मात् शब्दका वायद अर्थ में औरन संभवतःऔर न कदाचित् ही, क्योंकि तेजोधालु शायद आभ्यन्तर और शायद बाघ नही हैं और न संभवतः आभ्यन्तर और बाह्य और न कदाचित आभ्यन्तर और कदाचित् बाह्य, किन्तु मुनिदिचत रूपस आभ्यन्तर और बाह्य उभय अंग्रवाली है। इसी तरह महावीरने प्रत्येक धर्मके साथ 'सिया-स्यात् दाब्द जोड़कर अविबक्षित शेष बाँकी सूचना दी है । 'स्याम' शब्दको शायद संभव या कदाचितका पर्यायवाची कहना नितान्त भ्रमपूर्ण है।
महावीरने वस्तुतत्त्वको अनन्तधात्मक देखा और जाना। प्रत्येक पदार्थ अनन्त ही मण पर्यायोंका अखण्ड आधार है। उसका विराट रूप पूर्णतया शानका विषय हो भी जाय पर शब्दोंके वारा तो नहीं ही कहा