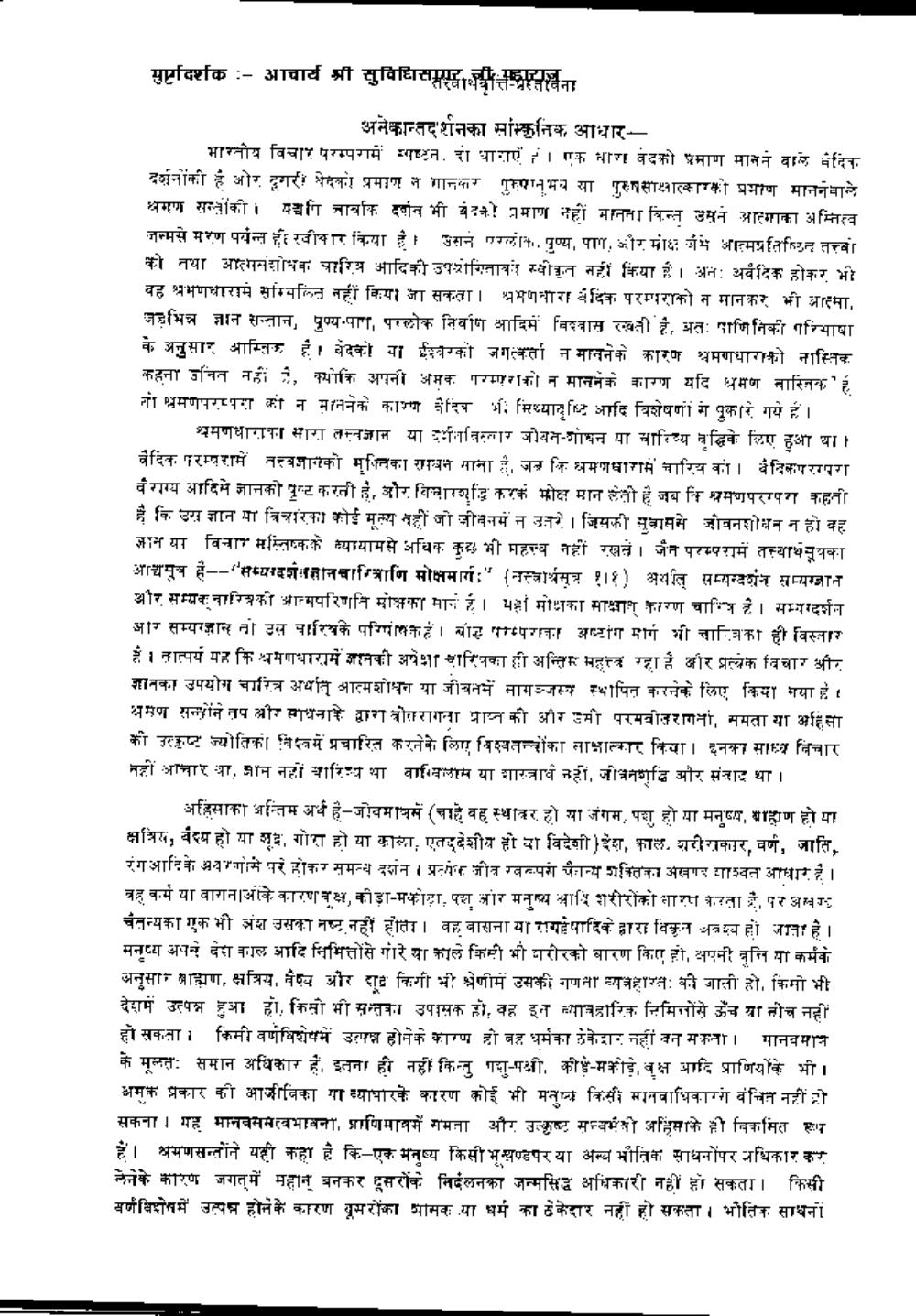________________
मुष्टादर्शक :- आचार्य श्री सुविधिसमता महाराजा
अनेकान्तदर्शनका सांस्कृतिक आधारभारतीय विचार परम्पगमें स्पष्टन. दो धागाएँ। एक भाग बंदको प्रमाण मानने वाले दिन दर्शनोंकी है ओर दुगरी वेदो प्रमाण ने गानकार गुरुपान मात्र या पुरुषसाक्षात्कारको प्रमाण माननेवाले श्रमण सन्त की। यद्यपि नार्वाक दर्शन भी बंद! माण नहीं मानना बिन्त उमन आत्माका अस्तित्व जन्मसे मरण पर्यन्त ही रवीकार किया है। उसन परलोक, पुण्य, पाण, और मोक्ष में आत्मप्रतिष्ठित तत्त्वा को तथा आत्मनंशोधन पारित्र आदिको उपगिताव स्वीकृत नहीं किया है। अन: अवैदिक होकर भी वह श्रमणधारामं सम्मिलित नहीं किया जा सकता। श्रमणवारा वैदिक परम्पराको न मानकर भी आत्मा, जभित्र ज्ञान सन्तान, पुण्य-पा, परलोक निर्वाण आदिम विश्वास रखती है, अतः पाणिनिकी ग्यिाषा के अनुसार आम्निा है। वेदको या ईश्वरको जगत्वा न मानने के कारण श्रमणधागको नास्तिक कहना उचित नहीं, क्योकि अपनी अमक. गरमागको न मानन के कारण यदि श्रमण नास्निक' है, नो श्रमणपराम्पमा को न मानने के कारण वैदित्र न मिथ्यावृष्टि आदि विशेषणों में पुकारे गये हैं।
थमणधागका सारा लन्नज्ञान या विस्तार जोबन-गोधन या चारित्र्य वृद्धिवे लिए हुआ था। वैदिक परम्परामें तत्त्वमानको मस्तिका साधन माना है, जब कि धमधारगमचारिय का। वैदिकप पग वैराग्य आदिमे जानको पृष्ट करती है, और विचारद्धि करकं मोक्ष मान लेती है जब कि श्रमणपरम्पग कहती है कि उस ज्ञान या विचारका कोई मूल्य नहीं जो जीवनम न सरे । जिसकी मुत्रासमे जोवनशोधन न हो वह जाम या विचार मस्तिष्कके न्यायामसे अधिक कुट भी महत्व नहीं रखते। जैन परम्परामं तस्यायका आद्यसुत्र है--सम्यादर्शनसानचाग्त्रिाणि मोक्षमार्ग:" निस्वार्थत्र ११) अयाल सम्यग्दर्शन सम्यग्जान और सम्यक् नारित्रकी आत्मपरिणति मोक्षका मान है। यह मोक्षका माक्षान् कारण चात्रि है। सम्यग्दर्शन आर सम्यग्ज़ाद ना उस पारिबके पगियापनहे। बाद पाम्पगना अष्टांग मार्ग भी तान्त्रिका ही विस्तार हैं। तात्पर्य यह कि श्रमणधारामें शानकी अशा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्व रहा है और प्रत्यक विचार और ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात् आत्मशोधन या जीवनमें नामञ्जस्य स्थापित करनेके लिए किया गया है। श्रमण सन्मोंने नप और साधनाके द्वारा त्रोत रागना प्राप्त की और उमी परमवीतरागनी, ममता या अहिंसा की उत्कृष्ट ज्योतिको विश्वमें प्रचारित करने के लिए विश्वतन्नोंका नाक्षात्कार किया। इनका साहब विचार नहीं आचार बा. मान नहीं वारिप था वाग्विालाम या शास्त्रार्थ नहीं, जीवनद्धि और संबाद था।
अहिंसाका अन्तिम अर्थ है-जोवमात्र (चाहे वह स्थावर हो या जंगम, पशु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, बंदय हो या शुद, गोरा हो या काला, एतद्देशीय हो या विदेशी देश, काल. शरीराकार, वर्ण, जाति, रंगआदि के प्रयागामे पर होकर ममन्य दर्शन । प्रतीक जीत्र ग्वन्पग चैतन्य शक्तिका अखगड गाश्वत आधार है। वह वर्म या वागनाओंके कारण वक्ष, कीड़ा-मकोटा, पश और मनुष्य आदि शरीरोंको धारण करता श्रे, पर अश्वगः चंतन्यका एक भी अंश उसका नष्ट नहीं होता। वह वासना या रागपादिके द्वारा विकृन अवश्य हो जाता है। मनुष्य अपने देशवाल आदि निमित्तोंसे गोरे या काले किसी भी वारीरको बारण किए हो, अपनी बुनि मा कर्मक अनूसा बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दा किगीभी श्रेणीमं उसकी गणना मयनहारतः बी जाती हो. किमो भी देदाम उत्पन्न हुआ हो, किसी भी सन्तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमिनोंसे ऊँच या नोच नहीं हो सकता। किमी वर्णविशेषमें उत्पन्न होने के कारण हो बह धर्मका ठेकेदार नहीं बन सकता। मानवमात्र के मूलत: समान अधिकार है, इतना ही नहीं किन्नु गदा-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियोंके भी। अमर प्रकार की आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिवाग्ग वंचित नहीं हो सकना । यह मानवसमत्वभावना, प्राणिमात्रमें गमता और उत्कृष्ट मन्यमंत्री अहिंसाके ही विक्रमित रूप हैं। श्रमणसन्तोंने यही कहा है कि-एक मनष्य किसीभन्यण्डपर या अन्य भौतिक साधनोंपर अधिकार कर लेने के कारण जगत में महान बनकर दूसरोंके निदंलनका जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता। किसी वर्णविदोष में उत्पन्न होने के कारण अमरोंका भामक या धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। भौतिक साधनों