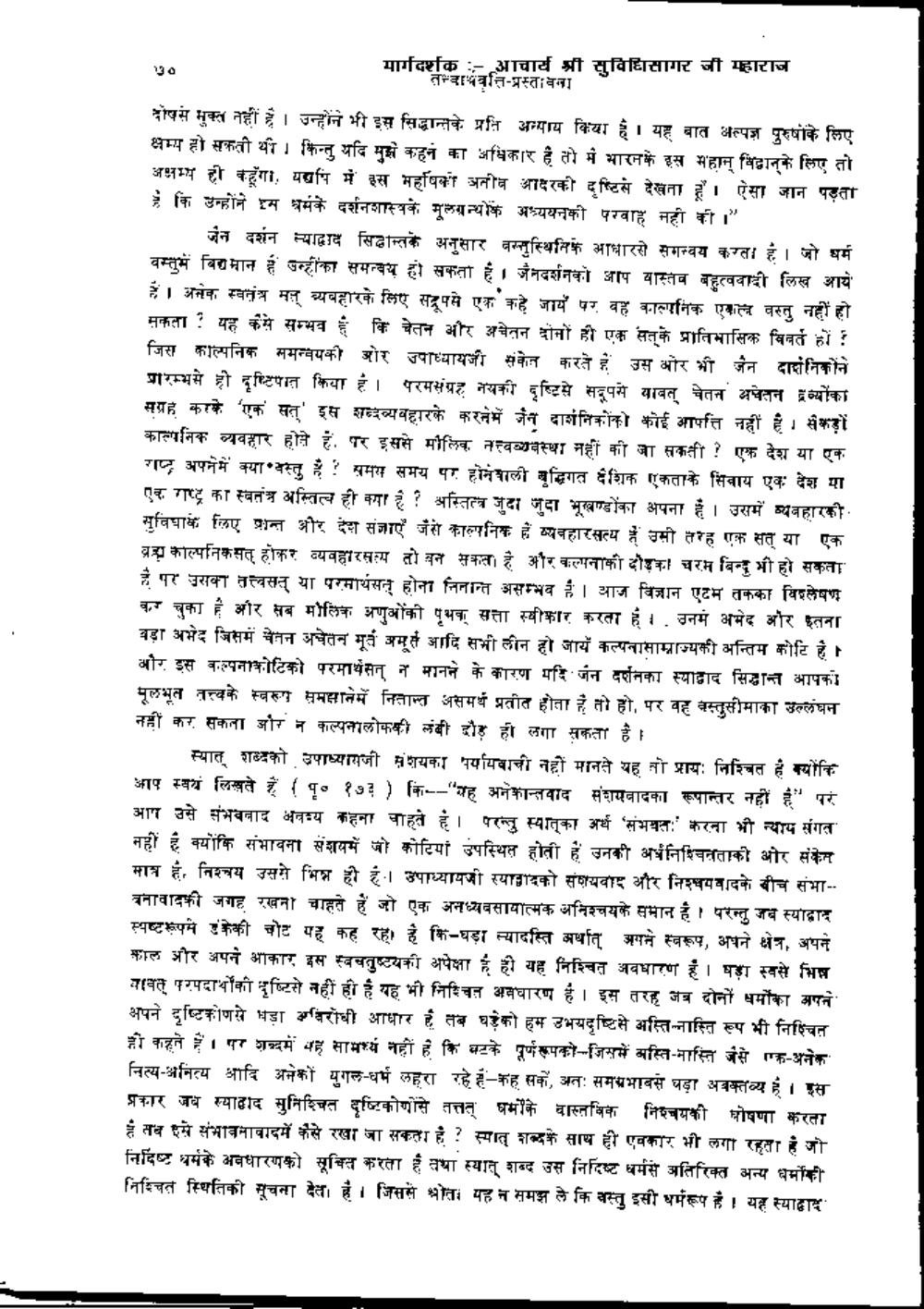________________
30
दोष मुक्त नहीं है। क्षम्य हो सकती थी। असभ्य ही कहूँगा है कि उन्होंने इस
मार्गदर्शक :- आचार्य श्री सुविधिसागर जी महाराज सदावृति प्रस्तावना
उन्होंने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पज्ञ पुरुषोंके लिए किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो में भारत के इस महान् विद्वानके लिए तो यद्यपि में इस महर्षिको अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ ऐसा जान पड़ता धर्मके दर्शनशास्त्र मूल अध्ययनकी परवाह नहीं की।"
I
जैन दर्शन स्याद्वाद सिद्धान्तके अनुसार वस्तुस्थिति आधारसे समन्वय करता है जो धर्म वस्तु विद्यमान है उन्हींना समत्यय हो सकता है। जैनदर्शनको आप वास्तव बहुत्ववादी लिख आये है। अनेक स्वतंत्र मत् व्यवहारके लिए सदूपये एक कहे जाये पर यह काल्पनिक एकल्व वस्तु नहीं हो सकता ? यह कैसे सम्भव है कि वेतन और अपेतन दोनों ही एक संत्के प्रातिभासिक विवह जिस काल्पनिक समयको शेर उपाध्यायजी संकेत करते हैं उस ओर भी जैन दाद निकोन प्रारम्भ से ही दृष्टिपात किया है। परमसंग्रह नयी दृष्टिसे सदूपसे यावत् चेतन अवेतन द्रव्योंका सह करके एक यत् इस व्यवहार करनेमें जैन दार्शनिकको कोई आपत्ति नहीं है। काल्पनिक व्यवहार होते है. पर इससे मौलिक तत्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक राष्ट्र अपने में क्या वस्तु समय समय पर होनेवाली वृद्धिगत वैशिक एकताके सिवाय एक देश एक राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व ही क्या है ? अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डोंका अपना है। उसमें व्यवहारकीसुविधा लिए शन्त और देश सभाएँ जैसे काल्पनिक व्यवहारखत्य में उसी तरह एक सत् या एक ब्रह्म काल्पनिक होकर व्यवहारसत्य तो बन सकता है और कल्पनाको दौड़का चरम बिन्दु भी हो सकता है पर उसका या परमार्थस होना नितान्त असम्भव है। आज विज्ञान एटम तरुका विश्लेषण कर चुका है और सब मौलिक अणुओंकी पृथक् सत्ता स्वीकार करता है उनमें अनेद और इतना बड़ा अभेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जायें कल्पनासाम्राज्यकी अन्तिम कोटि है। और इस कल्पनाकोटिको परमार्थसत् न मानने के कारण मदि जैन दर्शनका स्वाद्वाय सिद्धान्त आपक मूलभूत तत्वके स्वरूप समझाने में नितान्त असमर्थ प्रतीत होता है तो हो, पर वह वस्तुसीमाका उल्लंघन नहीं कर सकता और न कल्पनालोककी लंबी दौड़ ही लगा सकता है।
।
स्थात् शब्दको उपाध्यागी संजयका पर्यायवाची नहीं मानते यह तो प्रायः निश्चित है क्योंकि आप स्वयं लिखते हैं ( पृ० १०३) कि "यह अनेकान्तवाद संवादका रुपान्तर नहीं हूँ" परं आप उसे संभववाद अवश्य कहना चाहते है परन्तु स्वात्का अर्थ 'संभवतः' करना भी न्याय संगत नहीं है क्योंकि संभावना संयमें जो कोटियां उपस्थित होती है उनकी अनिश्चितताकी ओर संकेत मात्र है, निश्चय उससे भिन्न हो है । उपाध्यायजी स्याद्वादको संशयवाद और निश्चयवादके बीच संभा-चनावादी जगह रखना चाहते हैं जो एक अनध्यवसायात्मक अनिश्चयके समान है। परन्तु जब स्याद्वाद स्पष्टरूपये की चोट यह कह रहा है कि पड़ा ज्यादस्ति अर्थात् जगने स्वरूप, अपने क्षेत्र अपने काल और अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है। मड़ा वसे भ वात् परपदार्थों की दृष्टिसे नहीं ही है यह भी निश्चित अवधारण है। इस तरह जब दोनों धर्मोका अपने अपने दृष्टिकोण से घड़ा विरोधी आधार है तब घटेको हम उभयदृष्टि से अस्ति नास्ति रूप भी निश्चित ही कहते हैं। पर शब्दमें यह सामर्थ्य नहीं है कि मटके पूर्णरूपको जिसमें बस्ति नास्ति जैसे एक-अनेक नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगल-धर्म लहरा रहे हैं- कह सकें, अतः समग्रभावसे घड़ा अवक्तव्य हूँ। इस प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित दृष्टिकोणोंसे तत्तत् धर्मोके वास्तविक निश्चयको घोषणा करता संभावनावादमें कैसे रखा जा सकता है ? स्मात् शब्दके साथ ही एवकार भी लगा रहता है जो निर्दिष्ट धर्मके अवधारयको सूचित करता है वषा स्वात् शब्द उस निर्दिष्ट धर्मसे अतिरिक्त अन्य धर्मोकी निश्चित स्थितिको सूचना देता है। जिससे श्रोतः यह न समझ ले कि वस्तु इसी धर्मरूप है। यह स्याद्वाद