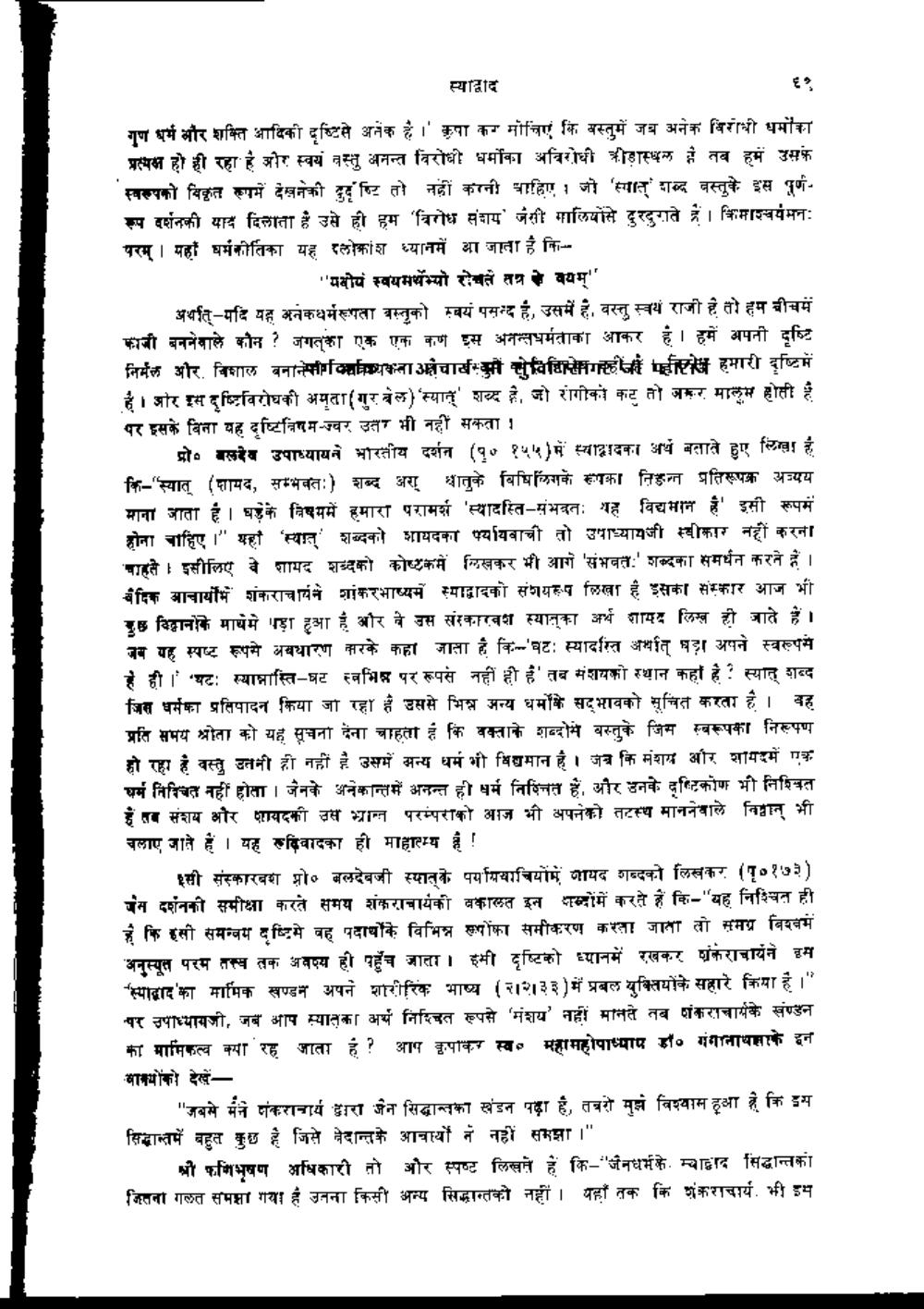________________
६९
स्याद्वाद
गुण धर्म और शक्ति आधिकी दृष्टिसे अनेक है। कृपा कर मोचिए कि वस्तुमें जब अनेक विरोधी धमका प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी तब हमें उसके स्वरूपको विकृत रूपमें देखनेकी दुई ष्टि तो नहीं करनी चाहिए जो 'स्वात्' शब्द वस्तुके इस पूर्णरूप दर्शनकी याद दिलाता है उसे ही हम "विरोध संशय' जंगी गालियोंसे दुरदुराते मनः परम्। यहाँ धर्मकीतिका मह लोकांश ध्यानमें आ जाता है कि
"मीयं स्वयमभ्यो रोचते
वयम्"
अर्थात् यदि यह अनेकधर्मरूपता वस्तुको स्वयं पसन्द है, उसमें है, वस्तु स्वयं राजी है तो हम बीचमें eat बननेवाले कौन ? जगत्का एक एक कम इस अगलधर्मताका आकर है। हमें अपनी दृष्टि निर्मल और विशाल बनाया अचार्यः सुविधिशेषगरी परेज हमारी दृष्टिमें है ओर इस दृष्टिविरोध की अमृता (गुर बेल ) 'स्यात्' शब्द है, जो रोगीको कटु तो जरूर मालूम होती है. पर इसके बिना यह दृष्टिनियम-ज्वर उत्तर भी नहीं सकता ।
प्रो. बलदेव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन (१० १५५) में स्वाद्भावना अर्थ बताते हुए लिखा है कि- "स्वात् ( शायद, सम्भवतः ) शब्द अरा वातुके विधिलिसके रूपका तिङन्त प्रतिरूपक अन्यय माना जाता है। घड़के विषयमें हमारा परामर्श 'स्यादस्ति संभवतः यह विद्यमान है। इसी रूपमें होना चाहिए।" यहाँ 'स्वात्' शब्दको शायद पर्यायवाची तो उपाध्यायणी स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए वे शायद शब्दको कोष्टकमें लिखकर भी आगे 'संभवत' शब्दका समर्थन करते हैं। वैदिक आचार्य शंकराचार्यने शांकरभाष्यमं स्वाद्वादको संगमस्य लिखा है इसका संस्कार आज भी कुछ विद्वानोंके माथेमे पड़ा हुआ है और वे उस संस्कारवश स्यात्का अर्थ शायद लिन हो जाते हैं। जब यह स्पष्ट रूपमे अवधारण करके कहा जाता है कि-'घटः स्यादस्ति अर्थात् घड़ा अपने स्वरूप में हे ही ।' 'घटः स्यान्नास्ति घट स्वभिन पर रूपसे नहीं ही है तब संशयको स्थान कहाँ है ? स्यात् शब्द fae धर्मका प्रतिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य धर्मो के सद्भावको सूचित करता है। वह प्रति समय श्रीता को यह सूचना देना चाहता वस्तुके जिस स्वरूपस्य निरूपण हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं है उसमें अन्य जब कि संशय और शामदमें एक धर्म निश्चित नहीं होता। जैनके अनेकान्त में अनन्त ही धर्म निश्चित है, और उनके दृष्टिकोण भी निश्चित हैं तब संशय और शायदकी उस भ्रान्त परम्पराको आज भी अपनेको तटस्थ माननेवाले विद्वान् भी चलाए जाते हैं। यह रूढ़िवादका ही माहात्म्य है !
कि वक्ता के शब्दोंग धर्म भी विद्यमान है।
इसी संस्कारवश प्रो० बलदेवजी स्यात्के पर्याययाचियोंमें शायद शब्दको लिखकर ( पृ०१७३ ) जैन दर्शनकी समीक्षा करते समय शंकराचार्यको वकालत इन पदों में करते हैं कि "यह निश्चित ही है कि इसी समन्वय दृष्टिसे वह पदार्थोंके विभिन्न रूपोंका समीकरण करता जाता तो समग्र विश्व अनुस्यूत परम तत्व तक अवश्य ही पहुँच जाता हमी दृष्टिको ध्यान में रखकर शंकराचार्य "स्माद्वाद का मार्मिक खण्डन अपने शारीरिक भाष्य ( २२२३३ ) में प्रबल युक्तियों के सहारे किया है।" पर उपाध्यायजी, जब आप स्वातका अर्थ निश्चित रूपसे 'गंशय' नहीं मानते तब शंकराचार्यके संण्डन का माणिकत्व क्या रह जाता है ? आगार स्व
हम
महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथा इन
वाक्योंको देखें
"जब मेने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धान्तका खंडन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ है कि इस सिद्धान्तमें बहुत कुछ है जिसे वेदान्त आचायों ने नहीं समझा।" श्री विभूषण अधिकारी तो
और स्पष्ट लिखने है कि-"जैनधर्म के स्वाद सिद्धान्तका जितना गलत समझा गया है उतना किसी अन्य सिद्धान्तको नहीं यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस