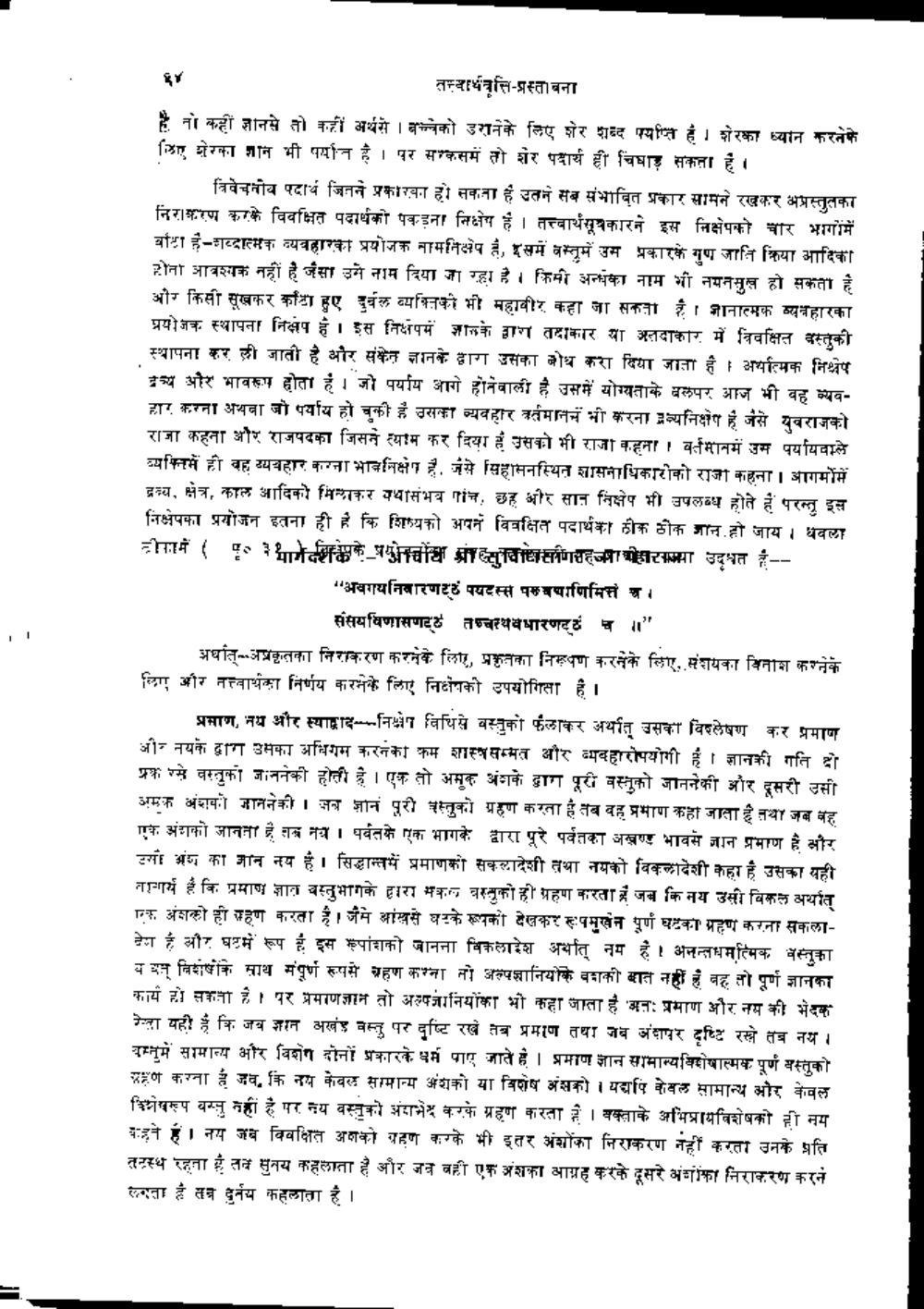________________
तस्वार्थवत्ति-प्रस्ताबना
है तो कहीं ज्ञानसे तो कहीं अर्थसे । बच्चको डराने के लिए शेर शब्द पर्याप्त है। शेरका ध्यान करनेके लिए शेरका शान भी पर्यात है । पर साकसम तो शेर पदार्थ ही चिंघाड़ सकता है।
विवेचनीय पदार्थ जितने प्रकारका हो सकता है उतने सब संभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तुतका निराकरण करके विक्षित पदार्थको पकड़ना निक्षेप है। तत्त्वार्थसूत्रकारने इस निक्षेपको चार भागोंमें बांटा है-गब्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेप है, इसम वस्तुमें उस प्रकारके गुण जाति क्रिया आदिका होना आवश्यक नहीं है जैसा उमे नाम दिया जा रहा है। किमी अन्धका नाम भी नयनसुख हो सकता है और किसी सुखकर काटा हुए दुर्बल व्यक्तिको भी महावीर कहा जा सकता है। ज्ञानात्मक व्यवहारका प्रयोजन स्थापना निक्षप है। इस निक्षपमं ज्ञानके द्वारा तदाकार या अतदाकार में विवक्षित वस्तुकी स्थापना कर ली जाती है और संकेत ज्ञानके द्वारा उसका बोध करा दिया जाता है । अर्थात्मक निक्षेप देव्य और भावरूप होता है। जो पर्याय आगे होनेवाली है उसमें योग्यताके बलपर आज भी वह व्यवहार करना अथवा जो पर्याय हो चुकी है उसका व्यवहार वर्तमान भी करना न्यनिक्षेप है जैसे युवराजको राजा कहना और राजपदका जिसने श्याम कर दिया है उसको भी राजा कहना। वर्तमानम उम पर्यायवाले व्यक्ति ही वह व्यवहार करना भावनिक्षेप है. जसे सिहासनस्थित शासनाधिकारीको राजा कहना । आगोमें द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिको मिलाकर स्थासंभव गांच, छह और सात निक्षेप भी उपलब्ध होते हैं परन्तु इस निक्षेपका प्रयोजन इतना ही है कि शिष्यको अपने विवक्षित पदार्थका ठीक ठोक मान हो जाय । धवला नौगाम ( पृ ३ मार्गशिकाके प्रयोचोंच श्रीवाससगिरहमा चोहाररामया उदृवत है--
"अवगनिवारण पयदस्स परुवाणिमित्त छ।
संसयविणासण? तच्चस्थवधारण8 च ॥" अर्थात्-अप्रकृतका निराकरण करने के लिए, प्रकृतका निरूपण करनेके लिए, संशयका विनाश करने के लिा और नत्त्वार्थका निर्णय करने के लिए निक्षेपको उपयोगिता है।
प्रमाण, नय और स्थावाद-निक्षेप विधिसे वस्तुको फैलाकर अर्थात् उसका विश्लेषण कर प्रमाण और नयके द्वारा उसका अधिगम करनका कम शास्त्रसम्मत और व्यवहारोपयोगी है। ज्ञानकी गति दो प्रा रमे वस्तुको जाननेकी होती है । एक तो अमुक अंगके द्वारा पूरी वस्तुको जानने की और दूसरी उसी अमक अंशवो जानने की । जब ज्ञानं पूरी वस्तुको ग्रहण करता है तब वह प्रमाण कहा जाता है तथा जब वह एक अंगको जानता है नत्र नय । पर्वतके एक भागके द्वारा पूरे पर्वतका अखण्ड भावसे ज्ञान प्रमाण है और उगा अंग का जान नय है। सिद्धान्त प्रमाणको सकलादेशी तथा नयको विकलादेशी कहा है उसका यही नागर्य है कि प्रमाण ज्ञात वस्तुभागके द्वारा मका वस्तुको ही ग्रहण करता है जब कि नय उसी विकल अर्थात कि अंशलो ही रहण करता है। जैसे आस्वसे घटके रूपको देखकर रूपमुखेन पूर्ण घटका ग्रहण करना सकलादेश है और घटमें रूप है इस रूपांशको जानना विकलादेश अर्थात् नम है। अनन्तधत्मिक वस्तुका य या विशेषोंके साथ मंपूर्ण रूपसे ग्रहण करना नो अल्पज्ञानियोंके बाकी बात नहीं हूँ बह तो पूर्ण ज्ञानका कार्य हो सकता है। पर प्रमाणज्ञान तो अल्पजानियोंका भी कहा जाता है अतः प्रमाण और नम की भेदक रेता यही है कि जब ज्ञान अखंड वस्तु पर दृष्टि रखें तब प्रमाण तथा जब अंदापर दृष्टि रस्ने तब नय । वस्तुमें सामान्य और विशेग दोनों प्रकारके धर्म पाए जाते है । प्रमाण ज्ञान सामान्यविशेषात्मक पूर्ण वस्तुको Bण करना है उव, कि नय केवल सामान्य अंशको या विशेष अंशको । यद्यपि केवल सामान्य और केवल किलोखरूप बस्नु नहीं है पर नय वस्तुको अंदाद करके ग्रहण करता है । वक्ताके अभिप्रायविशेषको ही नम कहते हैं। नय जब विवक्षित अशको ग्रहण करके भी इतर अंशोंका निराकरण नहीं करता उनके प्रति तटस्थ रहता है त सुनय कहलाता है और जब वही एक अंशका आग्रह करके दूसरे अंगोका निराकरण करने लगता है तब दुर्नय कहलाता है ।