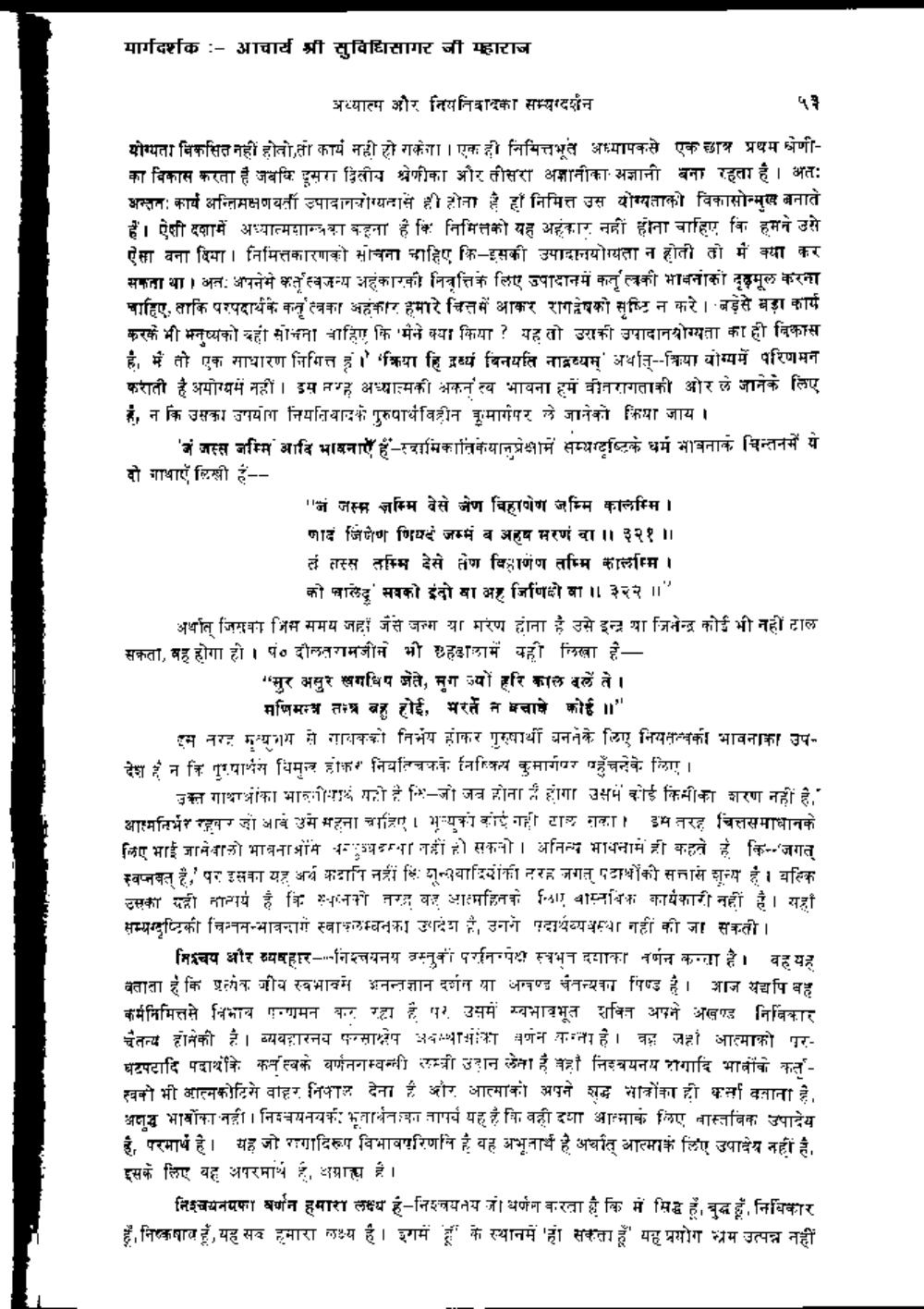________________
मार्गदर्शक :- आचार्य श्री सुविधिसागर जी महाराज
अध्यात्म और नियतिवादका सम्यग्दर्शन
योग्यता विकसित नहीं होतो,ता कार्य नहीं होगकेगा । एकही निमित्तभूत अध्यापकसे एक छात्र प्रथम श्रेणीका विकास करता है जबकि दूसरा द्वितीय श्रेणीका और तीसरा अज्ञानीका अज्ञानी बना रहता है। अत: अन्ततः कार्य अन्तिमक्षणवर्ती उपादानोग्यदास ही होता है हाँ निमित्त उस योग्यताको विकासोन्मुख बनाते हैं। ऐशी दशामें अध्यात्मशास्त्र का कहना है कि निमित्तको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने उसे ऐसा बना दिया। निमित्तकारणको सोचना चाहिए कि इसकी उपादानयोग्यता न होती तो मैं क्या कर सकता था। अत: अपनेमे कर्तृत्वजन्य अहंकारकी निवृत्ति के लिए उपादानम कर्तृलकी भावनाको दृढमूल करना चाहिए, ताकि परपदार्थ के कर्तृत्वका अहंकार हमारे चित्त में आकर रागद्वेषको सष्टि न करे। बड़े से बड़ा कार्य करके भी मनुष्यको यही सोचना चाहिए कि 'मैने क्या किया? यह तो उराकी उपादानयोग्यता का ही विकास है, मैं तो एक साधारण निमित्त है। क्रिया हि द्रव्य बिनयति नाव्यम्' अर्थात्--त्रिया योग्यमें परिणमन कराती है अयोग्यमं नहीं। इस तरह अध्यात्मकी अकनत्व भावना हम वीतरागताकी ओर ले जानेके लिए है, न कि उसका उपयोग नियतिवाद के पुरुषार्थविहीन बूमार्गपर ले जानेको किया जाय ।
'जं जस्स जम्मि आदि भावनाएँ हैं-स्वामिकानिकयानप्रेक्षाम सम्यग्दृष्टिकं धर्म भावनाकं चिन्तनमें ये दो गाथाएँ लिखी है--
" जस्म जम्मि वेसे जेण चिहाणेण जम्मि कालम्मि । कादं जिण णियदं जम्म ब अहष मरणं वा ।। ३२१ ॥ लं तस्स तम्मि देसे तण विहाणंण तम्मि कास्मि ।
को पालेद सबको इंदो या अह.जिणिो वा ॥ ३२२ ।।" अर्थात् जिसमा जिम ममय जहाँ जैसे जन्म या मरण होना है उसे इन्द्र या जिनेन्द्र कोई भी नहीं टाल सकता, वह होगा ही। पं० दौलतगमजीन भी छहवालामें कही लिखा है
"सुर असुर खगधिप जेते, मग ज्यों हरि काल बले ते ।
मणिमन्त्र तन्त्रबह होई, भरते न बचा कोई॥" हम तरह मन्याय की गावकको निर्भय होकर गुरुषार्थी बनने के लिए नियनत्वको भावनाका उपदेश है न कि पायंस चिमुन्न होकर नियतिचक्रवः निष्क्रिय कुमार्गपर पहुँचदेवे लिए।
उक्त गाथाओंका भारुती यही है कि जो जव होना होगा उसमें कोई किमीका कारण नहीं है। आत्मनिर्भर रहबर हा आवं उम महना चाहिए। मृत्युको डाई नही टाल गला। इस तरह चित्तसमाधानके लिए भाई जाने वालो भावनाओम कायदम्बा नहीं हो सकती। अनिन्य भावनामही कहते कि जान स्वप्नवत है. पर इसका यह अब कदापि नहीं कियान्मयादिशंकी दरह जगत् पढाथों की सत्तास शून्य है। बल्कि उसका बही नात्पर्य है कि वनको तरङ्ग व आत्महिनो ला वास्तविक कार्यकारी नहीं है। यहाँ सम्यग्दष्टिकी चिनन-भावनाग स्वालम्चनका उपदंदा है, उगगे पदार्थव्यवस्था नहीं की जा सकती।
मिचय और व्यवहार-..-निश्तयनन तमनुका पर्गन पक्ष स्त्रभन दयाका वर्णन करता है। वह यह वताता है कि प्रत्यंच. गीच स्वभावमे अनन्त ज्ञान दर्शन या अरण्ड चतन्यवर पिण्ड है। आज यद्यपि बह कर्मनिमित्तसे निभाव मिन बर रहा है, पर उसमें स्वभावभूत शक्ति अपने अखण्ड निविकार चैतन्य होनेकी है। व्यवहारनय कामाक्षेप यस्याका वर्णन यन्ना है। वह जहाँ आत्माको पुरघटपटादि पदार्थोके कर्मस्वके वर्णनगम्वन्धी सम्त्री उड़ान लेना है वहाँ निश्चयनयारागादि भावी कर्मस्वको भी आत्मकोटिमे बाहर निकाल देना है, और आत्माको अपने शुद्ध पात्रोंका ही कार्मा बनाना है. अनच भावोंका नहीं। निश्चयनवर्कः भतार्थताका तापर्य यह है कि वही दया आत्माकं लिए वास्तविक उपादेय ई. परमार्थ है। यह जो गगादिरूप विभावपरिणलि है वह अभूतार्थ है अर्थात् आत्माकं लिए उपादेय नहीं है, इसके लिए वह अपरमार्थ है, अग्राह्य है।
निश्चयनयका वर्णन हमारा लक्ष्य है-निश्चयनय जो वर्णन करता है कि में सिद्ध है। बद्ध हैं, निर्विकार है निस्कषाव हूँ, यह सर हमारा लक्ष्य है। इगम हूँ' के स्थानम 'हो सकता हूँ' यह प्रयोग भ्रम उत्पन्न नहीं