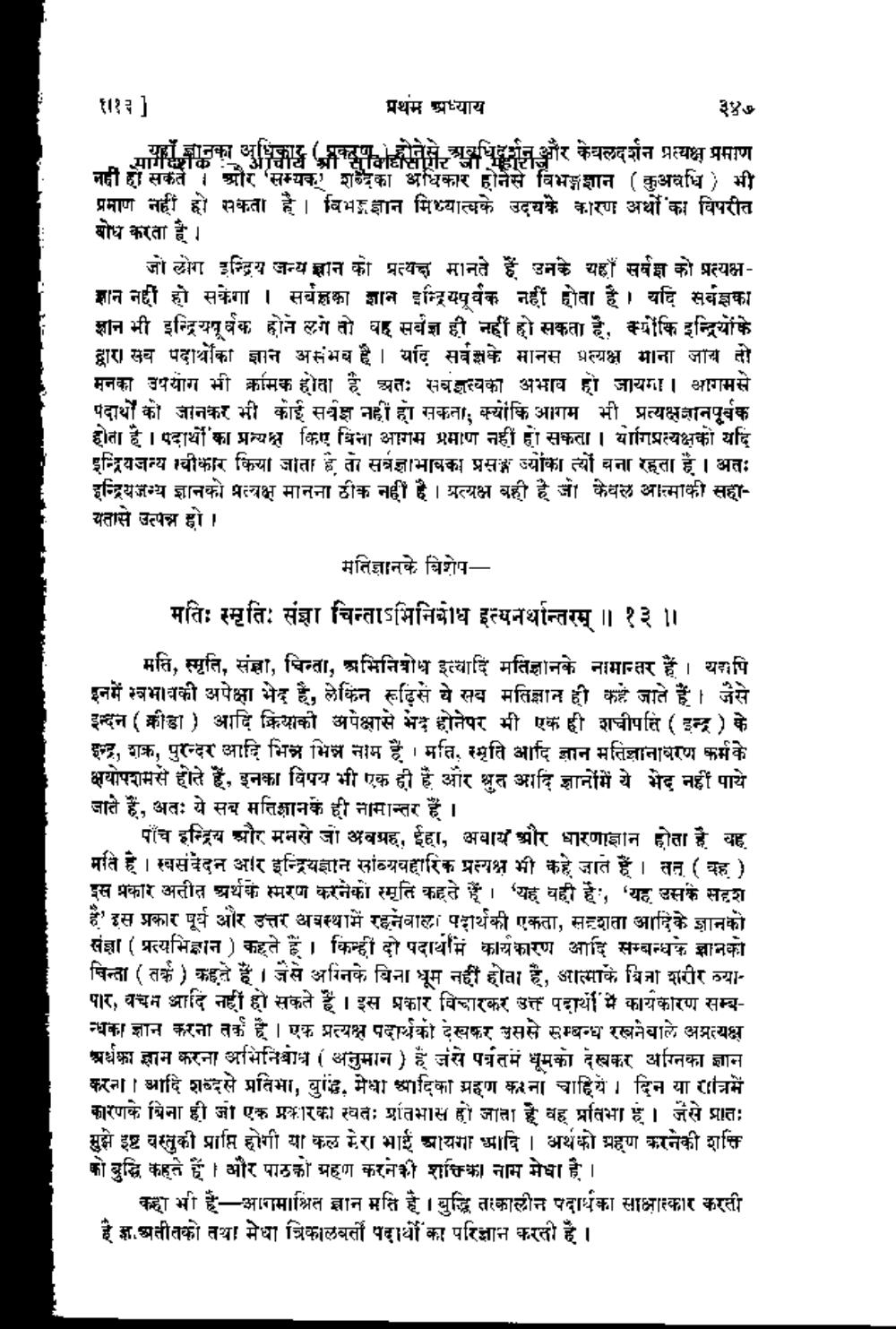________________
प्रथम अध्याय सामाज्ञानका अधिकार असावा होने से अधिशिऔर केवलदर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकते । और 'सम्यक शब्दका अधिकार होनेसे विभङ्गज्ञान (कुअवधि भी प्रमाण नहीं हो सकता है। विभज्ञान मिथ्यात्वके उदयके कारण अर्थो का विपरीत बोध करता है।
___ जो लोग इन्द्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं उनके यहाँ सर्वज्ञ को प्रत्यक्षज्ञान नहीं हो सकेगा । सर्वनका ज्ञान इन्द्रियपूर्वक नहीं होता है। यदि सर्वज्ञका झान भी इन्द्रियपूर्वक होने लगे तो वह सर्वज्ञ ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्द्रियों के द्वार। सब पदाओंका ज्ञान असंभव है । यदि सर्वशके मानस प्रत्यक्ष माना जाच तो मनका उपयोग भी क्रामक होता है अतः सबज्ञत्यका अभाव हो जायगा। आगमसे पदार्थों को जानकर भी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि आगम भी प्रत्यक्षज्ञानपूर्वक होता है । पदार्थों का प्रत्यक्ष किए बिना आगम प्रमाण नहीं हो सकता । योगप्रत्यक्षको यदि इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाता है तो सत्रज्ञाभावका प्रसङ्ग ज्योका त्यों बना रहता है। अतः इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष बही है जो केवल आत्माकी सहायतासे उत्पन्न हो।
मतिज्ञानके विशेषमतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनियोध इत्यनर्थान्तरम् ।। १३ ॥
मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनित्रोध इत्यादि मतिज्ञानके नामान्तर हैं। यदापि इनमें स्वभावकी अपेक्षा भेद हैं, लेकिन रूढ़िस ये सब मतिज्ञान ही कह जाते हैं। जैसे इन्दन ( क्रीडा) आदि क्रियाको अपेक्षासे भंद होनेपर भी एक ही शचीपति ( इन्द्र) के इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम है । मति. स्मृति आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशमसे होते हैं, इनका विषय भी एक ही है और श्रुत आदि ज्ञानों में ये भेद नहीं पाये जाते हैं, अतः ये सब मतिझानक ही नामान्तर है।।
पाँच इन्द्रिय और मनसे जो अवग्रह, ईहा, अवार्य और धारणाज्ञान होता है यह मति है । स्वसंवेदन आर इन्द्रियज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यश्न भी कहे जाते हैं। तत ( वह ) इस प्रकार अतीत अर्थक स्मरण करनेको स्मृति कहते हैं। 'यह वही है, 'यह उसके सदृश है। इस प्रकार पूर्व और उत्तर अवस्थामें रहनेवाला पदार्थकी एकता, सशता आदिके ज्ञानको संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान ) कहते हैं। किन्हीं दो पदार्थों में कार्यकारण आदि सम्बन्धक ज्ञानको चिन्ता ( तर्क ) कहते हैं । जैसे अग्निके बिना धूम नहीं होता है, आत्माके बिना शारीर व्यापार, वचन आदि नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार विचारकर उक्त पदार्थों में कायकारण सम्बन्धका ज्ञान करना तर्क है । एक प्रत्यक्ष पदार्थको देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले अप्रत्यक्ष अर्थका ज्ञान करना अभिनिवांत्र ( अनुमान ) है जैसे पर्वतमं धूमको देखकर अग्निका ज्ञान करना। आदि शब्दसे प्रतिभा, बुद्धि. मेधा आदिका ग्रहण करना चाहिये । दिन या सत्रमें कारणके बिना ही जो एक प्रकारका स्वतः प्रांतभास हो जाता है वह प्रतिभा हूं। जैसे प्रातः मुझे इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होगी या कल मेरा भाई आयगा आदि । अर्थको ग्रहण करनेकी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। और पाठको ग्रहण करने की शक्तिका नाम मेधा है।
कहा भी है-आगमाश्रित ज्ञान मति है । बुद्धि तत्कालीन पदार्थका साक्षात्कार करती है श.अतीतको तथा मेधा त्रिकालवी पदार्थों का परिज्ञान करती है ।