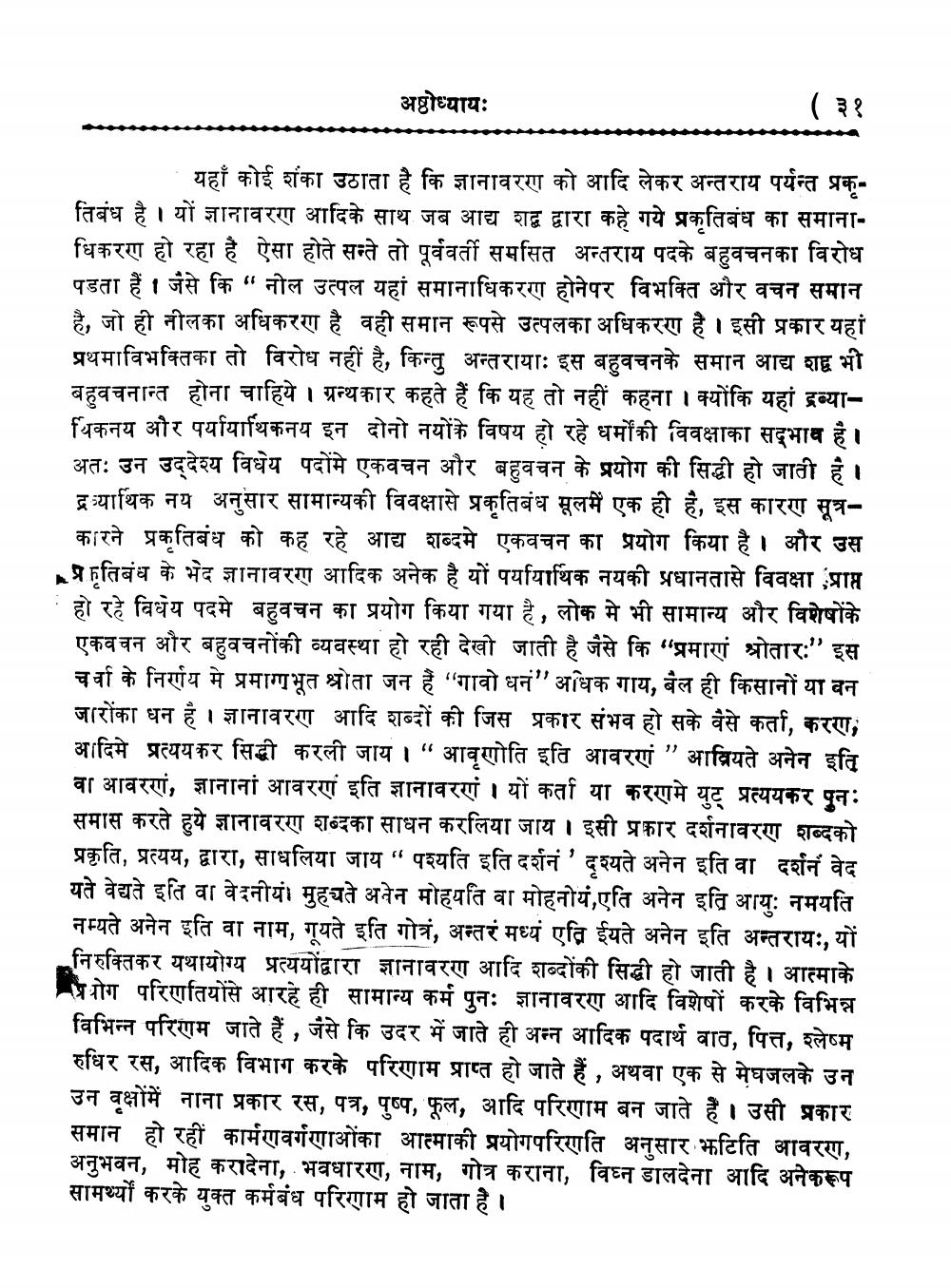________________
अष्ठोध्यायः
( ३१
यहाँ कोई शंका उठाता है कि ज्ञानावरण को आदि लेकर अन्तराय पर्यन्त प्रकृतिबंध है । यो ज्ञानावरण आदिके साथ जब आद्य शब्द द्वारा कहे गये प्रकृतिबंध का समानाधिकरण हो रहा है ऐसा होते सन्ते तो पूर्ववर्ती समसित अन्तराय पदके बहुवचनका विरोध पडता हैं । जैसे कि " नोल उत्पल यहां समानाधिकरण होनेपर विभक्ति और वचन समान है, जो ही नीलका अधिकरण है वही समान रूपसे उत्पलका अधिकरण है। इसी प्रकार यहां प्रथमाविभक्तिका तो विरोध नहीं है, किन्तु अन्तरायाः इस बहुवचनके समान आद्य शह भी बहुवचनान्त होना चाहिये । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि यहां द्रव्याथिकनय और पर्यायाथिकनय इन दोनो नयोंके विषय हो रहे धर्मों की विवक्षाका सद्भाव है। अतः उन उद्देश्य विधेय पदोंमे एकवचन और बहुवचन के प्रयोग की सिद्धी हो जाती है। द्रव्याथिक नय अनुसार सामान्यकी विवक्षासे प्रकृतिबंध मूलमें एक ही है, इस कारण सूत्रकारने प्रकृतिबंध को कह रहे आद्य शब्दमे एकवचन का प्रयोग किया है। और उस प्रतिबंध के भेद ज्ञानावरण आदिक अनेक है यों पर्यायार्थिक नयकी प्रधानतासे विवक्षा प्राप्त हो रहे विधेय पदमे बहुवचन का प्रयोग किया गया है , लोक मे भी सामान्य और विशेषोंके एकवचन और बहुवचनोंकी व्यवस्था हो रही देखो जाती है जैसे कि "प्रमाणं श्रोतारः" इस चर्चा के निर्णय मे प्रमाणभूत श्रोता जन हैं “गावो धनं" अधिक गाय, बैल ही किसानों या वन जारोंका धन है । ज्ञानावरण आदि शब्दों की जिस प्रकार संभव हो सके वैसे कर्ता, करण, आदिमे प्रत्ययकर सिद्धी करली जाय । " आवृणोति इति आवरणं " आवियते अनेन इति वा आवरणं, ज्ञानानां आवरणं इति ज्ञानावरणं । यों कर्ता या करणमे युट् प्रत्ययकर पुनः समास करते हुये ज्ञानावरण शब्दका साधन करलिया जाय । इसी प्रकार दर्शनावरण शब्दको प्रकृति, प्रत्यय, द्वारा, साधलिया जाय " पश्यति इति दर्शनं ' दृश्यते अनेन इति वा दर्शनं वेद यते वेद्यते इति वा वेदनीय। मुह्यते अनेन मोहयति वा मोहनोयं,एति अनेन इति आयु: नमयति नम्यते अनेन इति वा नाम, गूयते इति गोत्रं, अन्तरं मध्यं एति ईयते अनेन इति अन्तरायः, यों निरुक्तिकर यथायोग्य प्रत्ययोंद्वारा ज्ञानावरण आदि शब्दोंकी सिद्धी हो जाती है। आत्माके प्रयोग परिणतियोंसे आरहे ही सामान्य कर्म पुनः ज्ञानावरण आदि विशेषों करके विभिन्न विभिन्न परिणम जाते हैं , जैसे कि उदर में जाते ही अन्न आदिक पदार्थ वात, पित्त, श्लेष्म रुधिर रस, आदिक विभाग करके परिणाम प्राप्त हो जाते हैं , अथवा एक से मेघजलके उन उन वृक्षोंमें नाना प्रकार रस, पत्र, पुष्प, फूल, आदि परिणाम बन जाते हैं। उसी प्रकार समान हो रहीं कार्मणवर्गणाओंका आत्माकी प्रयोगपरिणति अनुसार झटिति आवरण, अनुभवन, मोह करादेना, भवधारण, नाम, गोत्र कराना, विघ्न डालदेना आदि अनेकरूप सामर्यों करके युक्त कर्मबंध परिणाम हो जाता है।