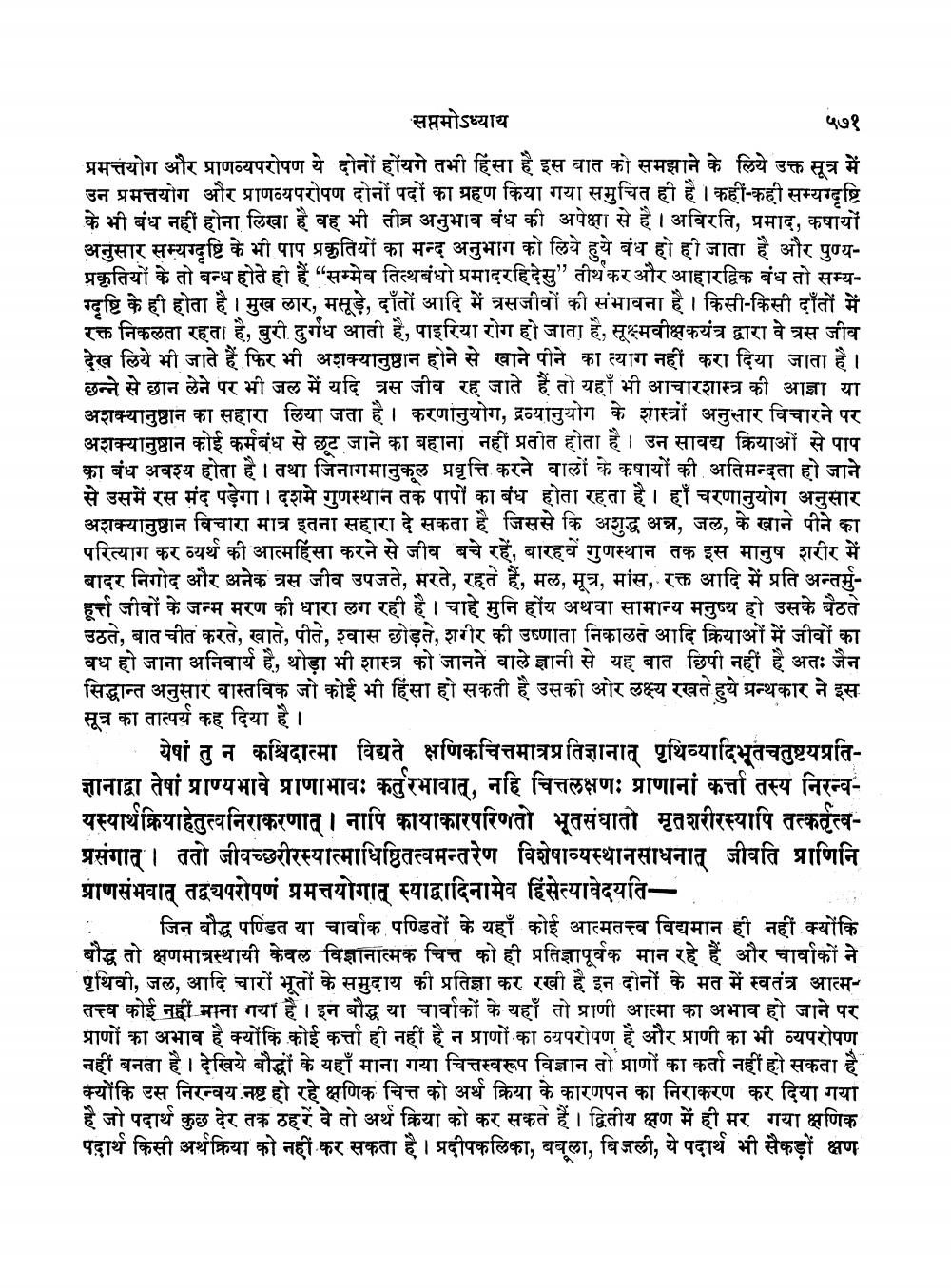________________
सप्तमोऽध्याय
५७१
प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण ये दोनों होंगे तभी हिंसा है इस बात को समझाने के लिये उक्त सूत्र में उन प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण दोनों पदों का ग्रहण किया गया समुचित ही है । कहीं-कही सम्यग्दृष्टि के भी बंध नहीं होना लिखा है वह भी तीव्र अनुभाव बंध की अपेक्षा से है । अविरति, प्रमाद, कषायों अनुसार सम्यग्दृष्टि के भी पाप प्रकृतियों का मन्द अनुभाग को लिये हुये बंध हो ही जाता है और पुण्यप्रकृतियों के तो बन्ध होते ही हैं "सम्मेव तित्थबंधो प्रमादरहिदेसु” तीर्थंकर और आहारद्विक बंध तो सम्यदृष्टि के ही होता है । मुख लार, मसूड़े, दाँतों आदि में त्रसजीवों की संभावना है। किसी-किसी दाँतों में रक्त निकलता रहता है, बुरी दुर्गंध आती है, पाइरिया रोग हो जाता है, सूक्ष्मवीक्षकयंत्र द्वारा वे त्रस जीव देख लिये भी जाते हैं फिर भी अशक्यानुष्ठान होने से खाने पीने का त्याग नहीं करा दिया जाता है । छन्ने से छान लेने पर भी जल में यदि त्रस जीव रह जाते हैं तो यहाँ भी आचारशास्त्र की आज्ञा या अशक्यानुष्ठान का सहारा लिया जता है । करणानुयोग, द्रव्यानुयोग के शास्त्रों अनुसार विचारने पर अशक्यानुष्ठान कोई कर्मबंध से छूट जाने का बहाना नहीं प्रतीत होता है । उन सावद्य क्रियाओं से पाप का बंध अवश्य होता है । तथा जिनागमानुकूल प्रवृत्ति करने वालों के कषायों की अतिमन्दता हो जाने से उसमें रस मंद पड़ेगा । दशमे गुणस्थान तक पापों का बंध होता रहता है। हाँ चरणानुयोग अनुसार अशक्यानुष्ठान विचारा मात्र इतना सहारा दे सकता है जिससे कि अशुद्ध अन्न, जल, के खाने पीने का परित्याग कर व्यर्थ की आत्महिंसा करने से जीव बचे रहें, बारहवें गुणस्थान तक इस मानुष शरीर में बादर निगोद और अनेक त्रस जीव उपजते, मरते, रहते हैं, मल, मूत्र, मांस, रक्त आदि में प्रति अन्तर्मुहूर्त्त जीवों के जन्म मरण की धारा लग रही है। चाहे मुनि होंय अथवा सामान्य मनुष्य हो उसके बैठते उठते, बात चीत करते, खाते, पीते, श्वास छोड़ते, शरीर की उष्णाता निकालते आदि क्रियाओं में जीवों का ध हो जाना अनिवार्य है, थोड़ा भी शास्त्र को जानने वाले ज्ञानी से यह बात छिपी नहीं है अतः जैन सिद्धान्त अनुसार वास्तविक जो कोई भी हिंसा हो सकती है उसकी ओर लक्ष्य रखते हुये प्रन्थकार ने इस सूत्र का तात्पर्य कह दिया है ।
येषां तु न कश्चिदात्मा विद्यते क्षणिकचित्तमात्रप्रतिज्ञानात् पृथिव्यादिभूतचतुष्टयप्रति - ज्ञानाद्वा तेषां प्राण्यभावे प्राणाभावः कर्तुरभावात्, नहि चित्तलक्षणः प्राणानां कर्त्ता तस्य निरन्वयस्यार्थक्रिया हेतुत्वनिराकरणात् । नापि कायाकारपरिणतो भूतसंघातो मृतशरीरस्यापि तत्कर्तृत्वप्रसंगात् । ततो जीवच्छरीरस्यात्माधिष्ठितत्वमन्तरेण विशेषाव्यस्थानसाधनात् जीवति प्राणिनि प्राणसंभवात् तद्वयपरोपणं प्रमत्तयोगात् स्याद्वादिनामेव हिंसेत्यावेदयति —
जिन बौद्ध पण्डित या चार्वाक पण्डितों के यहाँ कोई आत्मतत्त्व विद्यमान ही नहीं क्योंकि बौद्ध तो क्षणमा स्थायी केवल विज्ञानात्मक चित्त को ही प्रतिज्ञापूर्वक मान रहे हैं और चार्वाकों ने पृथिवी, जल, आदि चारों भूतों के समुदाय की प्रतिज्ञा कर रखी है इन दोनों के मत में स्वतंत्र आत्मतत्व कोई नहीं माना गया है। इन बौद्ध या चार्वाकों के यहाँ तो प्राणी आत्मा का अभाव हो जाने पर प्राणों का अभाव है क्योंकि कोई कर्त्ता ही नहीं है न प्राणों का व्यपरोपण है और प्राणी का भी व्यपरोपण नहीं बनता है | देखिये बौद्धों के यहाँ माना गया चित्तस्वरूप विज्ञान तो प्राणों का कर्ता नहीं हो सकता हैं क्योंकि उस निरन्वय नष्ट हो रहे क्षणिक चित्त को अर्थ क्रिया के कारणपन का निराकरण कर दिया गया पदार्थ कुछ देर तक ठहरें वे तो अर्थ क्रिया को कर सकते हैं । द्वितीय क्षण में ही मर गया क्षणिक पदार्थ किसी अर्थक्रिया को नहीं कर सकता है। प्रदीपकलिका, बबूला, बिजली, ये पदार्थ भी सैकड़ों क्षण
I