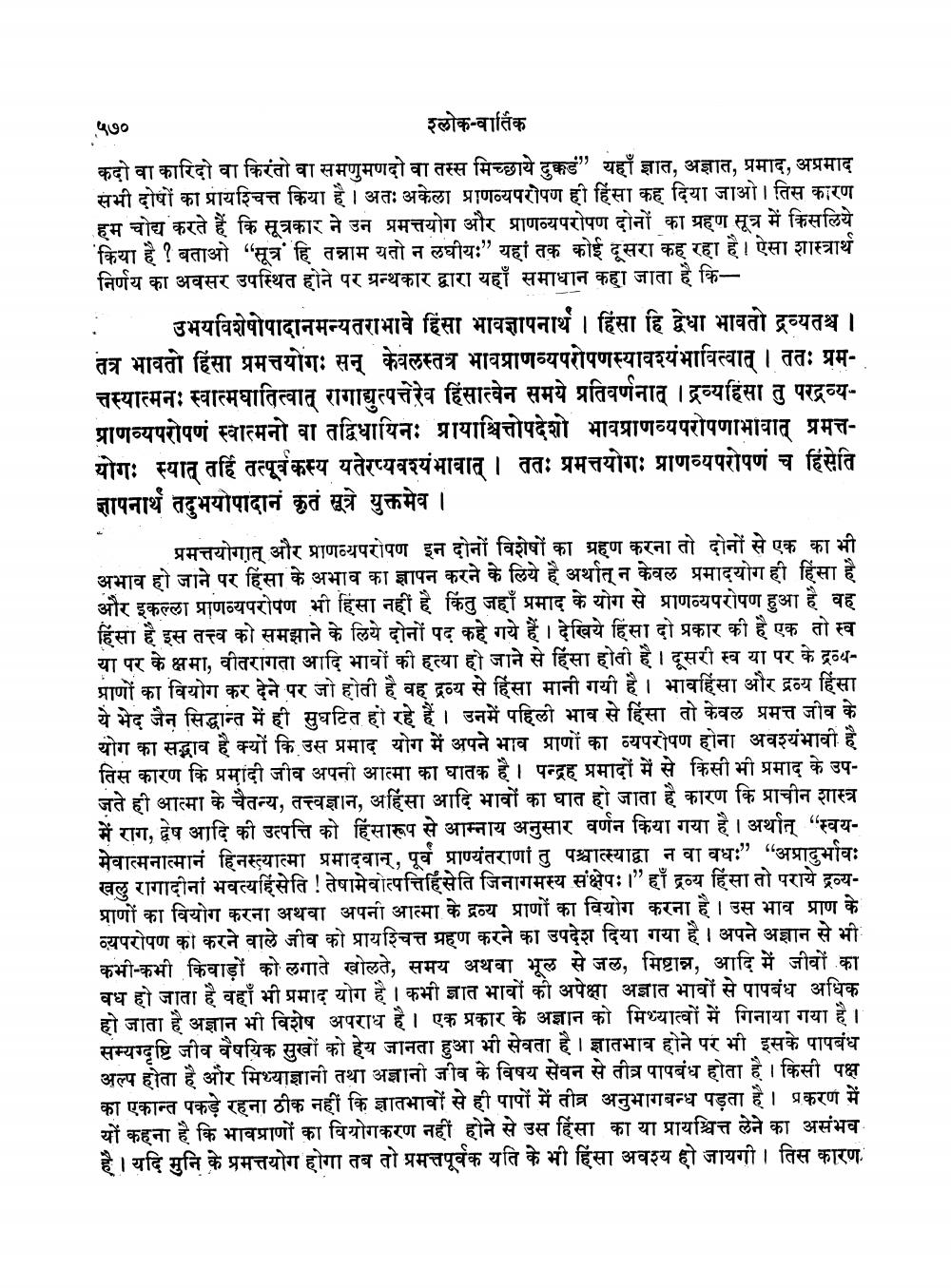________________
५७०
श्लोक-वार्तिक कदो वा कारिदो वा किरंतो वा समणुमणदो वा तस्स मिच्छाये दुक्कड" यहाँ ज्ञात, अज्ञात, प्रमाद, अप्रमाद सभी दोषों का प्रायश्चित्त किया है । अतः अकेला प्राणव्यपरोपण ही हिंसा कह दिया जाओ। तिस कारण हम चोद्य करते हैं कि सूत्रकार ने उन प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण दोनों का ग्रहण सूत्र में किसलिये किया है ? बताओ "सूत्र हि तन्नाम यतो न लघीयः” यहां तक कोई दूसरा कह रहा है। ऐसा शास्त्रार्थ निर्णय का अवसर उपस्थित होने पर ग्रन्थकार द्वारा यहाँ समाधान कहा जाता है कि. उभयविशेषोपादानमन्यतराभावे हिंसा भावज्ञापनार्थ । हिंसा हि द्वेधा भावतो द्रव्यतश्च । तत्र भावतो हिंसा प्रमत्तयोगः सन् केवलस्तत्र भावप्राणव्यपरोपणस्यावश्यंभावित्वात् । ततः प्रमत्तस्यात्मनः स्वात्मघातित्वात् रागाद्युत्पत्तेरेव हिंसात्वेन समये प्रतिवर्णनात् । द्रव्यहिंसा तु परद्रव्यप्राणव्यपरोपणं स्वात्मनो वा तद्विधायिनः प्रायाश्चित्तोपदेशो भावप्राणव्यपरोपणाभावात् प्रमत्तयोगः स्यात् तर्हि तत्पूर्वकस्य यतेरप्यवश्यंभावात् । ततः प्रमत्तयोगः प्राणव्यपरोपणं च हिंसेति ज्ञापनार्थ तदुभयोपादानं कृतं सूत्रे युक्तमेव ।
प्रमत्तयोगात् और प्राणव्यपरोपण इन दोनों विशेषों का ग्रहण करना तो दोनों से एक का भी अभाव हो जाने पर हिंसा के अभाव का ज्ञापन करने के लिये है अर्थात् न केवल प्रमादयोग ही हिंसा है
और इकल्ला प्राणव्यपरोपण भी हिंसा नहीं है किंतु जहाँ प्रमाद के योग से प्राणव्यपरोपण हुआ है वह हिंसा है इस तत्त्व को समझाने के लिये दोनों पद कहे गये हैं । देखिये हिंसा दो प्रकार की है एक तो स्व या पर के क्षमा, वीतरागता आदि भावों की हत्या हो जाने से हिंसा होती है। दूसरी स्व या पर के द्रव्यप्राणों का वियोग कर देने पर जो होती है वह द्रव्य से हिंसा मानी गयी है। भावहिंसा और द्रव्य हिंसा ये भेद जैन सिद्धान्त में ही सुघटित हो रहे हैं। उनमें पहिली भाव से हिंसा तो केवल प्रमत्त जीव के योग का सद्भाव है क्यों कि उस प्रमाद योग में अपने भाव प्राणों का व्यपरोपण होना अवश्यंभावी है तिस कारण कि प्रमादी जीव अपनी आत्मा का घातक है। पन्द्रह प्रमादों में से किसी भी प्रमाद के उपजते ही आत्मा के चैतन्य, तत्त्वज्ञान, अहिंसा आदि भावों का घात हो जाता है कारण कि प्राचीन शास्त्र में राग, द्वेष आदि की उत्पत्ति को हिंसारूप से आम्नाय अनुसार वर्णन किया गया है । अर्थात् "स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् , पूर्व प्राण्यंतराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः" "अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ! तेषामेवोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः।" हाँ द्रव्य हिंसा तो पराये द्रव्यप्राणों का वियोग करना अथवा अपनी आत्मा के द्रव्य प्राणों का वियोग करना है । उस भाव प्राण के व्यपरोपण को करने वाले जीव को प्रायश्चित्त ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। अपने अज्ञान से भी कभी-कभी किवाड़ों को लगाते खोलते, समय अथवा भूल से जल, मिष्टान्न, आदि में जीवों का वध हो जाता है वहाँ भी प्रमाद योग है । कभी ज्ञात भावों की अपेक्षा अज्ञात भावों से पापबंध अधिक हो जाता है अज्ञान भी विशेष अपराध है। एक प्रकार के अज्ञान को मिथ्यात्वों में गिनाया गया है। सम्यग्दृष्टि जीव वैषयिक सुखों को हेय जानता हुआ भी सेवता है । ज्ञातभाव होने पर भी इसके पापबंध अल्प होता है और मिथ्याज्ञानी तथा अज्ञानी जीव के विषय सेवन से तीव्र पापबंध होता है । किसी पक्ष का एकान्त पकडे रहना ठीक नहीं कि ज्ञातभावों से ही पापों में तीव्र अनुभागबन्ध पडता है। प्रकरण में यों कहना है कि भावप्राणों का वियोगकरण नहीं होने से उस हिंसा का या प्रायश्चित्त लेने का असंभव है। यदि मुनि के प्रमत्तयोग होगा तब तो प्रमत्तपूर्वक यति के भी हिंसा अवश्य हो जायगी। तिस कारण