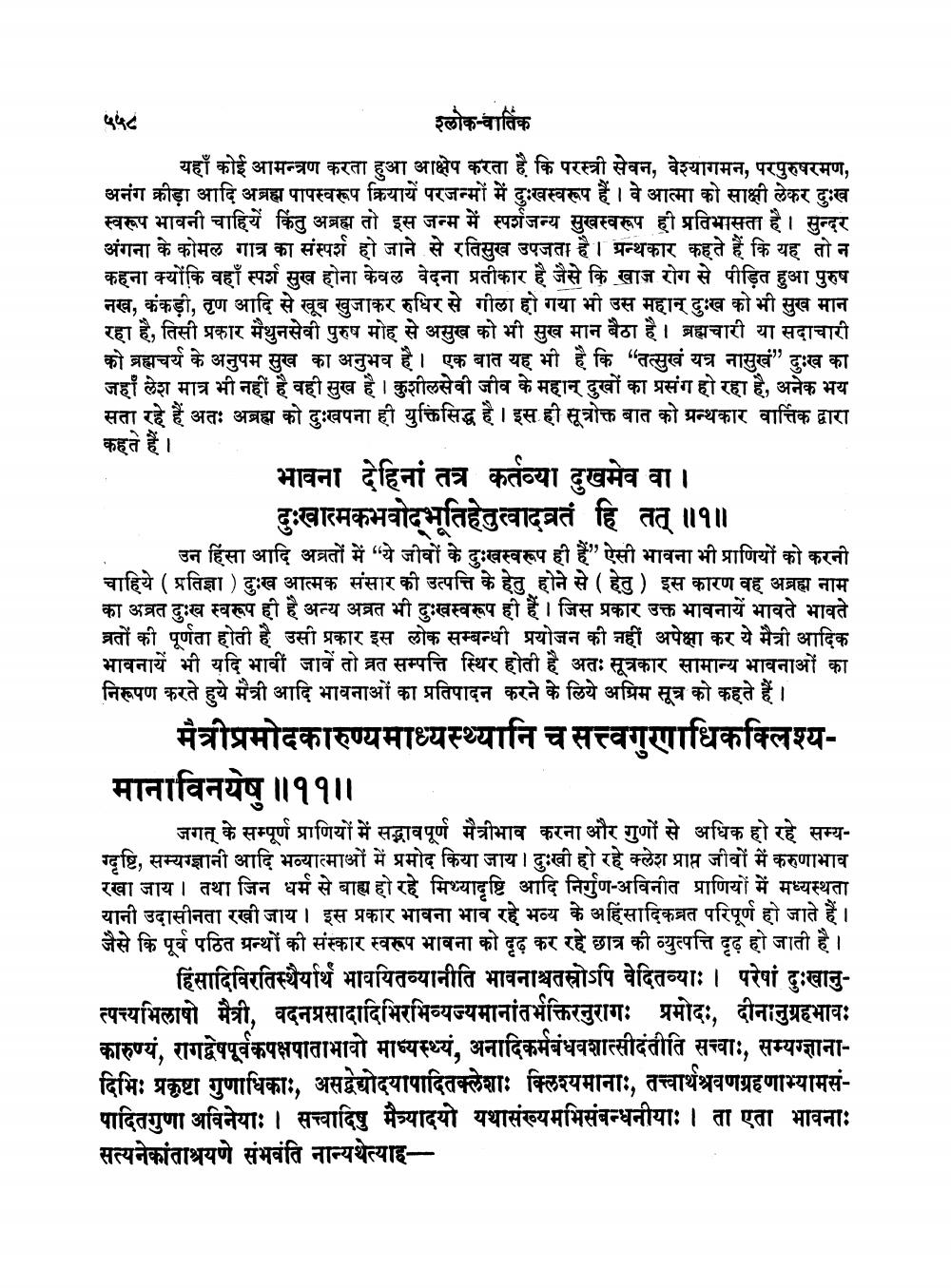________________
५५८
श्लोक वार्तिक यहाँ कोई आमन्त्रण करता हुआ आक्षेप करता है कि परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, परपुरुषरमण, अनंग क्रीड़ा आदि अब्रह्म पापस्वरूप क्रियायें परजन्मों में दुःखस्वरूप हैं । वे आत्मा को साक्षी लेकर दुःख स्वरूप भावनी चाहिये किंतु अब्रह्म तो इस जन्म में स्पर्शजन्य सुखस्वरूप ही प्रतिभासता है। सुन्दर अंगना के कोमल गात्र का संस्पर्श हो जाने से रतिसुख उपजता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि वहाँ स्पर्श सुख होना केवल वेदना प्रतीकार है जैसे कि खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष नख, कंकड़ी, तृण आदि से खूब खुजाकर रुधिर से गीला हो गया भी उस महान दुःख को भी सुख मान रहा है, तिसी प्रकार मैथुनसेवी पुरुष मोह से असुख को भी सुख मान बैठा है। ब्रह्मचारी या सदाचारी को ब्रह्मचर्य के अनुपम सुख का अनुभव है। एक बात यह भी है कि "तत्सुखं यत्र नासुखं" दुःख का जहाँ लेश मात्र भी नहीं है वही सुख है । कुशीलसेवी जीव के महान दुखों का प्रसंग हो रहा है, अनेक भय सता रहे हैं अतः अब्रह्म को दुःखपना ही युक्तिसिद्ध है । इस ही सूत्रोक्त बात को ग्रन्थकार वार्तिक द्वारा कहते हैं।
भावना देहिनां तत्र कर्तव्या दुखमेव वा।
दुःखात्मकभवोद्भुतिहेतुत्वादव्रतं हि तत् ॥१॥ उन हिंसा आदि अव्रतों में “ये जीवों के दुःखस्वरूप ही हैं ऐसी भावना भी प्राणियों को करनी चाहिये (प्रतिज्ञा ) दुःख आत्मक संसार की उत्पत्ति के हेतु होने से ( हेतु ) इस कारण वह अब्रह्म नाम का अव्रत दुःख स्वरूप ही है अत्य अव्रत भी दुःखस्वरूप ही हैं । जिस प्रकार उक्त भावनायें भावते भावते व्रतों की पूर्णता होती है उसी प्रकार इस लोक सम्बन्धी प्रयोजन की नहीं अपेक्षा कर ये मैत्री आदिक भावनायें भी यदि भावी जावें तो व्रत सम्पत्ति स्थिर होती है अतः सूत्रकार सामान्य भावनाओं का निरूपण करते हुये मैत्री आदि भावनाओं का प्रतिपादन करने के लिये अग्रिम सूत्र को कहते हैं।
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु ॥११॥
जगत् के सम्पूर्ण प्राणियों में सद्भावपूर्ण मैत्रीभाव करना और गुणों से अधिक हो रहे सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी आदि भव्यात्माओं में प्रमोद किया जाय। दुःखी हो रहे क्लेश प्राप्त जीवों में करुणाभ रखा जाय । तथा जिन धर्म से बाह्य हो रहे मिथ्यादृष्टि आदि निर्गुण-अविनीत प्राणियों में मध्यस्थता यानी उदासीनता रखी जाय । इस प्रकार भावना भाव रहे भव्य के अहिंसादिकव्रत परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि पूर्व पठित ग्रन्थों की संस्कार स्वरूप भावना को दृढ़ कर रहे छात्र की व्युत्पत्ति दृढ़ हो जाती है।
हिंसादिविरतिस्थैर्यार्थ भावयितव्यानीति भावनाश्चतस्रोऽपि वेदितव्याः। परेषां दुःखानुत्पत्यभिलाषो मैत्री, वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यमानांतर्भक्तिरनुरागः प्रमोदः, दीनानुग्रहभावः कारुण्यं, रागद्वेषपूर्वकपक्षपाताभावो माध्यस्थ्यं, अनादिकर्मबंधवशात्सीदंतीति सच्चाः, सम्यग्ज्ञानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधिकाः, असद्वद्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्यमानाः, तत्त्वार्थश्रवणग्रहणाभ्यामसंपादितगुणा अविनेयाः । सवादिषु मैत्र्यादयो यथासंख्यमभिसंबन्धनीयाः। ता एता भावनाः सत्यनेकांताश्रयणे संभवंति नान्यथेत्याह