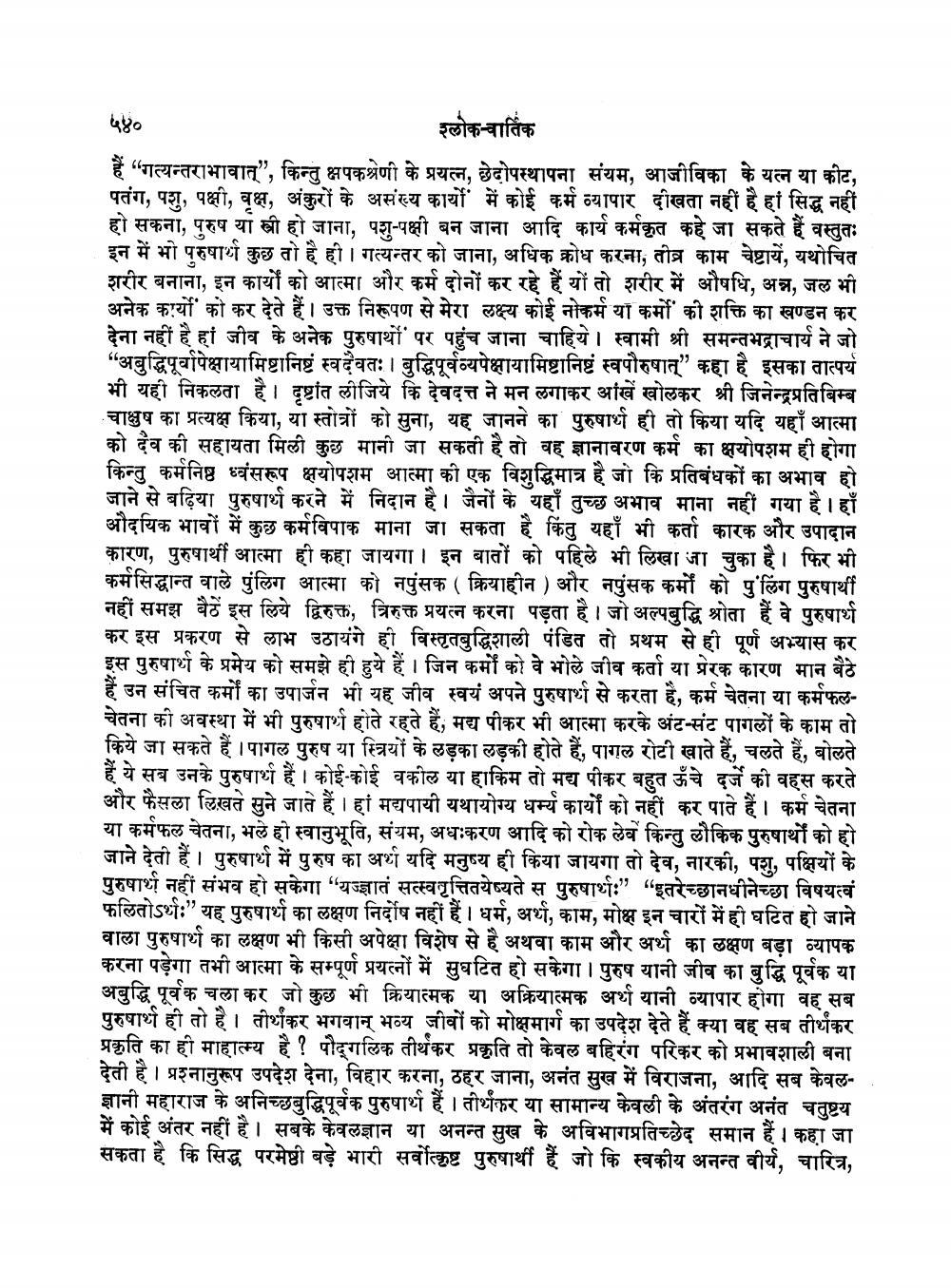________________
५४०
श्लोक-वार्तिक
हैं “गत्यन्तराभावात्”, किन्तु क्षपकश्रेणी के प्रयत्न, छेदोपस्थापना संयम, आजीविका के यत्न या कीट, पतंग, पशु, पक्षी, वृक्ष, अंकुरों के असंख्य कार्यों में कोई कर्म व्यापार दीखता नहीं है हां सिद्ध नहीं हो सकना, पुरुष या स्त्री हो जाना, पशु-पक्षी बन जाना आदि कार्य कर्मकृत कहे जा सकते हैं वस्तुतः इन में भी पुरुषार्थ कुछ तो है ही । गत्यन्तर को जाना, अधिक क्रोध करना, तीव्र काम चेष्टायें, यथोचित शरीर बनाना, इन कार्यों को आत्मा और कर्म दोनों कर रहे हैं यों तो शरीर में औषधि, अन्न, जल भी अनेक कार्यो को कर देते हैं । उक्त निरूपण से मेरा लक्ष्य कोई नोकर्म या कर्मों की शक्ति का खण्डन कर देना नहीं है हां जीव के अनेक पुरुषार्थो पर पहुंच जाना चाहिये । स्वामी श्री समन्तभद्राचार्य ने जो “अबुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः । बुद्धिपूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुषात् " कहा है इसका तात्पर्य भी यही निकलता है । दृष्टांत लीजिये कि देवदत्त ने मन लगाकर आंखें खोलकर श्री जिनेन्द्रप्रतिबिम्ब चाक्षुष का प्रत्यक्ष किया, या स्तोत्रों को सुना, यह जानने का पुरुषार्थ ही तो किया यदि यहाँ आत्मा को देव की सहायता मिली कुछ मानी जा सकती है तो वह ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ही होगा किन्तु कर्मनिष्ठ ध्वंसरूप क्षयोपशम आत्मा की एक विशुद्धिमात्र है जो कि प्रतिबंधकों का अभाव हो जाने से बढ़िया पुरुषार्थ करने में निदान है। जैनों के यहाँ तुच्छ अभाव माना नहीं गया है। हाँ औक भावों में कुछ कर्मविपाक माना जा सकता है किंतु यहाँ भी कर्ता कारक और उपादान कारण, पुरुषार्थी आत्मा ही कहा जायगा । इन बातों को पहिले भी लिखा जा चुका है। फिर भी कर्मसिद्धान्त वाले पुंलिंग आत्मा को नपुंसक ( क्रियाहीन ) और नपुंसक कर्मों को पुलिंग पुरुषार्थी नहीं समझ बैठें इसलिये द्विरुक्त, त्रिरुक्त प्रयत्न करना पड़ता है । जो अल्पबुद्धि श्रोता हैं वे पुरुषार्थ कर इस प्रकरण से लाभ उठायेंगे ही विस्तृतबुद्धिशाली पंडित तो प्रथम से ही पूर्ण अभ्यास कर इस पुरुषार्थ के प्रमेय को समझे ही हुये हैं। जिन कर्मों को वे भोले जीव कर्ता या प्रेरक कारण मान बैठे हैं उन संचित कर्मों का उपार्जन भी यह जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ से करता है, कर्म चेतना या कर्मफलचेतना की अवस्था में भी पुरुषार्थ होते रहते हैं, मद्य पीकर भी आत्मा करके अंट-संट पागलों के काम तो किये जा सकते हैं | पागल पुरुष या स्त्रियों के लड़का लड़की होते हैं, पागल रोटी खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं ये सब उनके पुरुषार्थ हैं । कोई-कोई वकील या हाकिम तो मद्य पीकर बहुत ऊँचे दर्जे की वहस करते और फैसला लिखते सुने जाते हैं। हां मद्यपायी यथायोग्य धर्म्य कार्यों को नहीं कर पाते हैं। कर्म चेतना या कर्मफल चेतना, भले ही स्वानुभूति, संयम, अधःकरण आदि को रोक लेवें किन्तु लौकिक पुरुषार्थों को हो जाने देती हैं । पुरुषार्थ में पुरुष का अर्थ यदि मनुष्य ही किया जायगा तो देव, नारकी, पशु, पक्षियों के पुरुषार्थ नहीं संभव हो सकेगा " यज्ज्ञातं सत्स्ववृत्तितयेष्यते स पुरुषार्थः” “इतरेच्छानधीनेच्छा विषयत्वं फलितोऽर्थः " यह पुरुषार्थ का लक्षण निर्दोष नहीं हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में ही घटित हो जाने वाला पुरुषार्थ का लक्षण भी किसी अपेक्षा विशेष से है अथवा काम और अर्थ का लक्षण बड़ा व्यापक करना पड़ेगा तभी आत्मा के सम्पूर्ण प्रयत्नों में सुघटित हो सकेगा । पुरुष यानी जीव का बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक चलाकर जो कुछ भी क्रियात्मक या अक्रियात्मक अर्थ यानी व्यापार होगा वह सब पुरुषार्थ ही तो है । तीर्थंकर भगवान् भव्य जीवों को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं क्या वह सब तीर्थंकर प्रकृति का ही माहात्म्य है ? पौद्गलिक तीर्थंकर प्रकृति तो केवल बहिरंग परिकर को प्रभावशाली बना देती है। प्रश्नानुरूप उपदेश देना, बिहार करना, ठहर जाना, अनंत सुख में विराजना, आदि सब केवलज्ञानी महाराज के अनिच्छबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ हैं । तीर्थंकर या सामान्य केवली के अंतरंग अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है। सबके केवलज्ञान या अनन्त सुख के अविभागप्रतिच्छेद समान हैं । कहा जा सकता है कि सिद्ध परमेष्ठी बड़े भारी सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थी हैं जो कि स्वकीय अनन्त वीर्य, चारित्र,