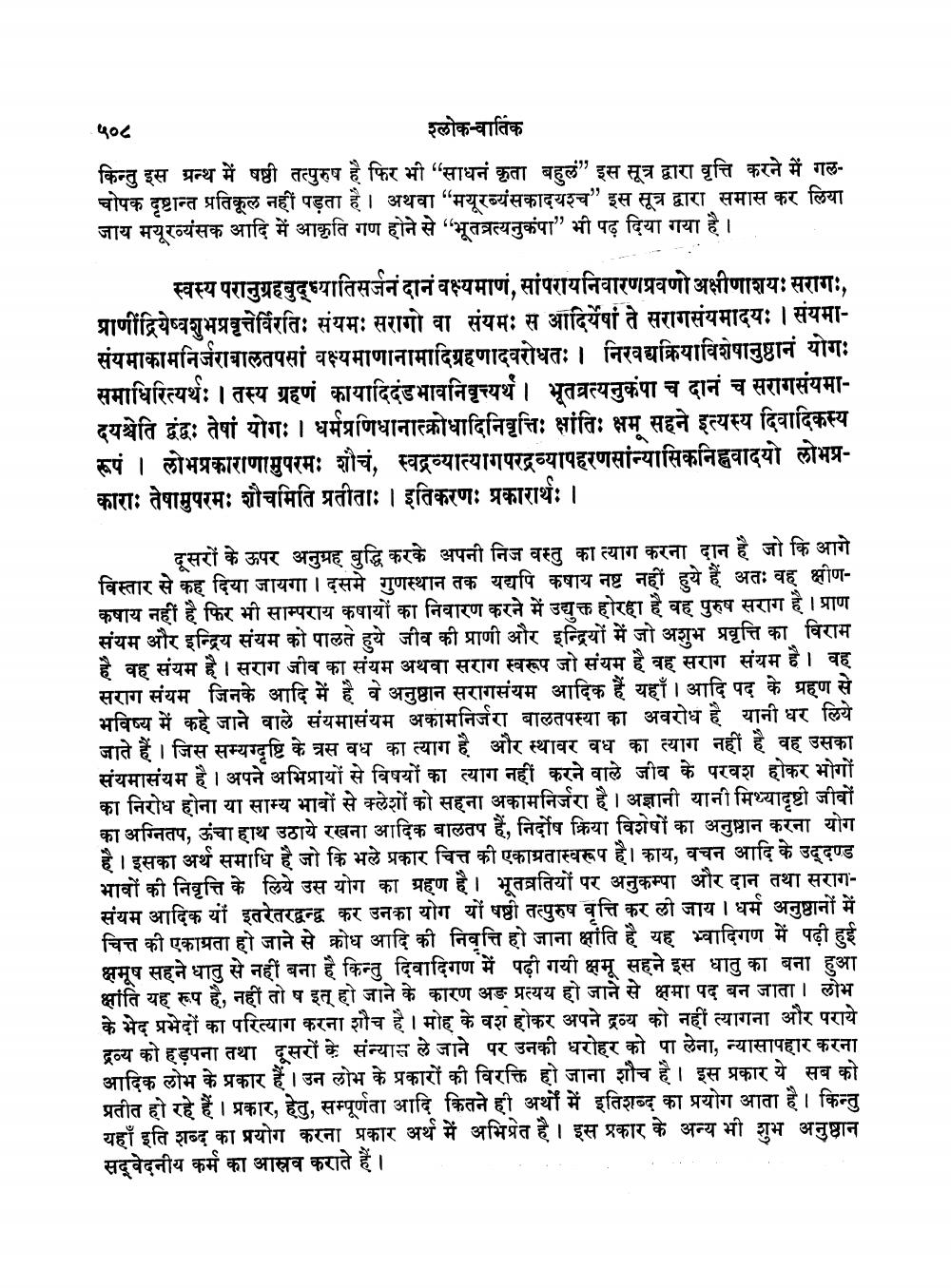________________
५०८
श्लोक-वार्तिक किन्तु इस ग्रन्थ में षष्ठी तत्पुरुष है फिर भी “साधनं कृता बहुलं" इस सूत्र द्वारा वृत्ति करने में गलचोपक दृष्टान्त प्रतिकूल नहीं पड़ता है। अथवा "मयूरब्यसकादयश्च" इस सूत्र द्वारा समास कर लिया जाय मयूरव्यंसक आदि में आकृति गण होने से “भूतव्रत्यनुकंपा" भी पढ़ दिया गया है।
स्वस्य परानुग्रहबुद्ध्यातिसर्जनंदानं वक्ष्यमाणं, सांपरायनिवारणप्रवणो अक्षीणाशयः सरागः, प्राणींद्रियेष्वशुभप्रवृत्तेविरतिः संयमः सरागो वा संयमः स आदिर्येषां ते सरागसंयमादयः । संयमासंयमाकामनिर्जराबालतपसां वक्ष्यमाणानामादिग्रहणादवरोधतः। निरवद्यक्रियाविशेषानुष्ठानं योगः समाधिरित्यर्थः । तस्य ग्रहणं कायादिदंडभावनिवृत्त्यर्थ । भृतव्रत्यनुकंपा च दानं च सरागसंयमादयश्चेति द्वंद्वः तेषां योगः । धर्मप्रणिधानात्क्रोधादिनिवृत्तिः शांतिः सम सहने इत्यस्य दिवादिकस्य रूपं । लोभप्रकाराणामुपरमः शौचं, स्वद्रव्यात्यागपरद्रव्यापहरणसांन्यासिकनिह्नवादयो लोभप्रकाराः तेषामुपरमः शौचमिति प्रतीताः । इतिकरणः प्रकारार्थः ।
दूसरों के ऊपर अनुग्रह बुद्धि करके अपनी निज वस्तु का त्याग करना दान है जो कि आगे विस्तार से कह दिया जायगा । दसमे गुणस्थान तक यद्यपि कषाय नष्ट नहीं हुये हैं अतः वह क्षीणकषाय नहीं है फिर भी साम्पराय कषायों का निवारण करने में उद्युक्त होरहा है वह पुरुष सराग है । प्राण संयम और इन्द्रिय संयम को पालते हुये जीव की प्राणी और इन्द्रियों में जो अशुभ प्रवृत्ति का विराम है वह संयम है। सराग जीव का संयम अथवा सराग स्वरूप जो संयम है वह सराग संयम है। वह सराग संयम जिनके आदि में है वे अनुष्ठान सरागसंयम आदिक हैं यहाँ । आदि पद के ग्रहण से भविष्य में कहे जाने वाले संयमासंयम अकामनिर्जरा बालतपस्या का अवरोध है यानी धर लिये जाते हैं । जिस सम्यग्दृष्टि के त्रस वध का त्याग है और स्थावर वध का त्याग नहीं है वह उसका संयमासंयम है । अपने अभिप्रायों से विषयों का त्याग नहीं करने वाले जीव के परवश होकर भोगों का निरोध होना या साम्य भावों से क्लेशों को सहना अकामनिर्जरा है । अज्ञानी यानी मिथ्यादृष्टी जीवों का अग्नितप, ऊंचा हाथ उठाये रखना आदिक बालतप हैं, निर्दोष क्रिया विशेषों का अनुष्ठान करना योग है। इसका अर्थ समाधि है जो कि भले प्रकार चित्त की एकाग्रतास्वरूप है। काय, वचन आदि के उद्दण्ड भावों की निवृत्ति के लिये उस योग का ग्रहण है। भूतव्रतियों पर अनुकम्पा और दान तथा सरागसंयम आदिक यों इतरेतरद्वन्द्व कर उनका योग यों षष्ठी तत्पुरुष वृत्ति कर ली जाय । धर्म अनुष्ठानों में चित्त की एकाग्रता हो जाने से क्रोध आदि की निवृत्ति हो जाना क्षांति है यह भ्वादिगण में पढ़ी हुई क्षमूष सहने धातु से नहीं बना है किन्तु दिवादिगण में पढ़ी गयी क्षमू सहने इस धातु का बना हुआ क्षांति यह रूप है, नहीं तो ष इत् हो जाने के कारण अङ प्रत्यय हो जाने से क्षमा पद बन जाता। लोभ के भेद प्रभेदों का परित्याग करना शौच है । मोह के वश होकर अपने द्रव्य को नहीं त्यागना और पराये द्रव्य को हड़पना तथा दूसरों के संन्यास ले जाने पर उनकी धरोहर को पा लेना, न्यासापहार करना आदिक लोभ के प्रकार हैं । उन लोभ के प्रकारों की विरक्ति हो जाना शौच है। इस प्रकार ये सब को प्रतीत हो रहे हैं । प्रकार, हेतु, सम्पूर्णता आदि कितने ही अर्थों में इतिशब्द का प्रयोग आता है। किन्तु यहाँ इस
। इति शब्द का प्रयोग करना प्रकार अर्थ में अभिप्रेत है। इस प्रकार के अन्य भी शुभ अनुष्ठान सवेंदनीय कर्म का आस्रव कराते हैं।