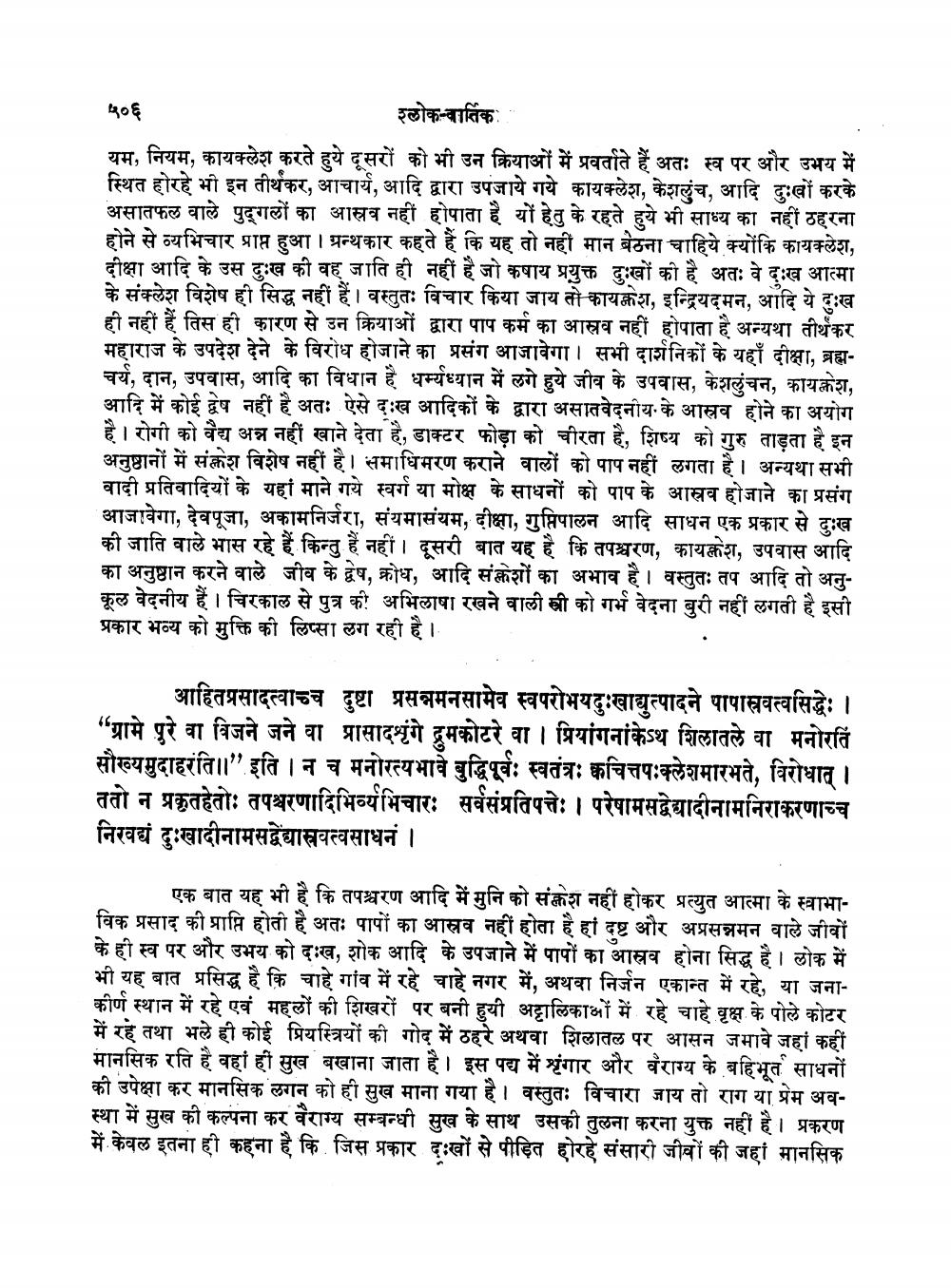________________
५०६
श्लोक- वार्तिक:
यम, नियम, कायक्लेश करते हुये दूसरों को भी उन क्रियाओं में प्रवर्ताते हैं अतः स्व पर और उभय में स्थित होरहे भी इन तीर्थंकर, आचार्य, आदि द्वारा उपजाये गये कायक्लेश, केशलुंच, आदि दुःखों करके असातफल वाले पुद्गलों का आस्रव नहीं होपाता है यों हेतु के रहते हुये भी साध्य का नहीं ठहरना होने से व्यभिचारप्राप्त हुआ । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं मान बैठना चाहिये क्योंकि कायक्लेश, दीक्षा आदि के उस दुःख की वह जाति ही नहीं है जो कषाय प्रयुक्त दुःखों की है अतः वे दुःख आत्मा के संक्लेश विशेष ही सिद्ध नहीं हैं। वस्तुतः विचार किया जाय तो कायक्लेश, इन्द्रियदमन, आदि ये दुःख ही नहीं हैं तिस ही कारण से उन क्रियाओं द्वारा पाप कर्म का आस्रव नहीं होपाता है अन्यथा तीर्थंकर महाराज के उपदेश देने के विरोध होजाने का प्रसंग आजावेगा। सभी दार्शनिकों के यहाँ दीक्षा, ब्रह्म'चर्य, दान, उपवास, आदि का विधान है धर्म्यध्यान में लगे हुये जीव के उपवास, केशलुंचन, कायक्लेश, आदि में कोई द्वेष नहीं है अतः ऐसे दुःख आदिकों के द्वारा असातावेदनीय के आस्रव होने का अयोग है। रोगी को वैद्य अन्न नहीं खाने देता है, डाक्टर फोड़ा को चीरता है, शिष्य को गुरु ताड़ता है इन अनुष्ठानों में संक्लेश विशेष नहीं है। समाधिमरण कराने वालों को पाप नहीं लगता है। अन्यथा सभी वादी प्रतिवादियों के यहां माने गये स्वर्ग या मोक्ष के साधनों को पाप के आस्रव होजाने का प्रसंग आजावेगा, देवपूजा, अकामनिर्जरा, संयमासंयम, दीक्षा, गुप्तिपालन आदि साधन एक प्रकार से दुःख की जाति वाले भास रहे हैं किन्तु हैं नहीं। दूसरी बात यह है कि तपश्चरण, कायक्लेश, उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले जीव के द्वेष, क्रोध, आदि संक्लेशों का अभाव है। वस्तुतः तप आदि तो अनुकूल वेदनीय हैं । चिरकाल से पुत्र की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को गर्भ वेदना बुरी नहीं लगती है इसी प्रकार भव्य को मुक्ति की लिप्सा लग रही है ।
आहितप्रसादत्वाच्च दुष्टा प्रसन्नमनसामेव स्वपरोभयदुः खाद्युत्पादने पापास्रवत्वसिद्धेः । “ग्रामे पुरे वा विजने जने वा प्रासादशृंगे द्रुमकोटरे वा । प्रियांगनांकेऽथ शिलातले वा मनोरतिं सौख्यमुदाहरति।।” इति । न च मनोरत्यभावे बुद्धिपूर्वः स्वतंत्रः क्वचित्तपः क्लेशमारभते, विरोधात् । ततो न प्रकृतहेतोः तपश्चरणादिभिर्व्यभिचारः सर्वसंप्रतिपत्तेः । परेषामसद्वेद्यादीनामनिराकरणाच्च निरवद्यं दुःखादीनामसद्वेद्यास्त्रवत्वसाधनं ।
एक बात यह भी है कि तपश्चरण आदि में मुनि को संक्लेश नहीं होकर प्रत्युत आत्मा के स्वाभा विक प्रसाद की प्राप्ति होती है अतः पापों का आस्रव नहीं होता है हां दुष्ट और अप्रसन्नमन वाले जीवों केही स्व पर और उभय को दःख, शोक आदि के उपजाने में पापों का आस्रव होना सिद्ध है । लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि चाहे गांव में रहे चाहे नगर में, अथवा निर्जन एकान्त में रहे, या जनाकीर्ण स्थान में रहे एवं महलों की शिखरों पर बनी हुयी अट्टालिकाओं में रहे चाहे वृक्ष के पोले कोटर में रहे तथा भले ही कोई प्रियस्त्रियों की गोद में ठहरे अथवा शिलातल पर आसन जमावे जहां कहीं मानसिक रति है वहां हीं सुख बखाना जाता है। इस पद्य में शृंगार और वैराग्य के बहिभूर्त साधनों की उपेक्षा कर मानसिक लगन को ही सुख माना गया है। वस्तुतः विचारा जाय तो राग या प्रेम अवस्था में सुख की कल्पना कर वैराग्य सम्बन्धी सुख के साथ उसकी तुलना करना युक्त नहीं है । प्रकरण में केवल इतना ही कहना है कि जिस प्रकार दुःखों से पीड़ित होरहे संसारी जीवों की जहां मानसिक