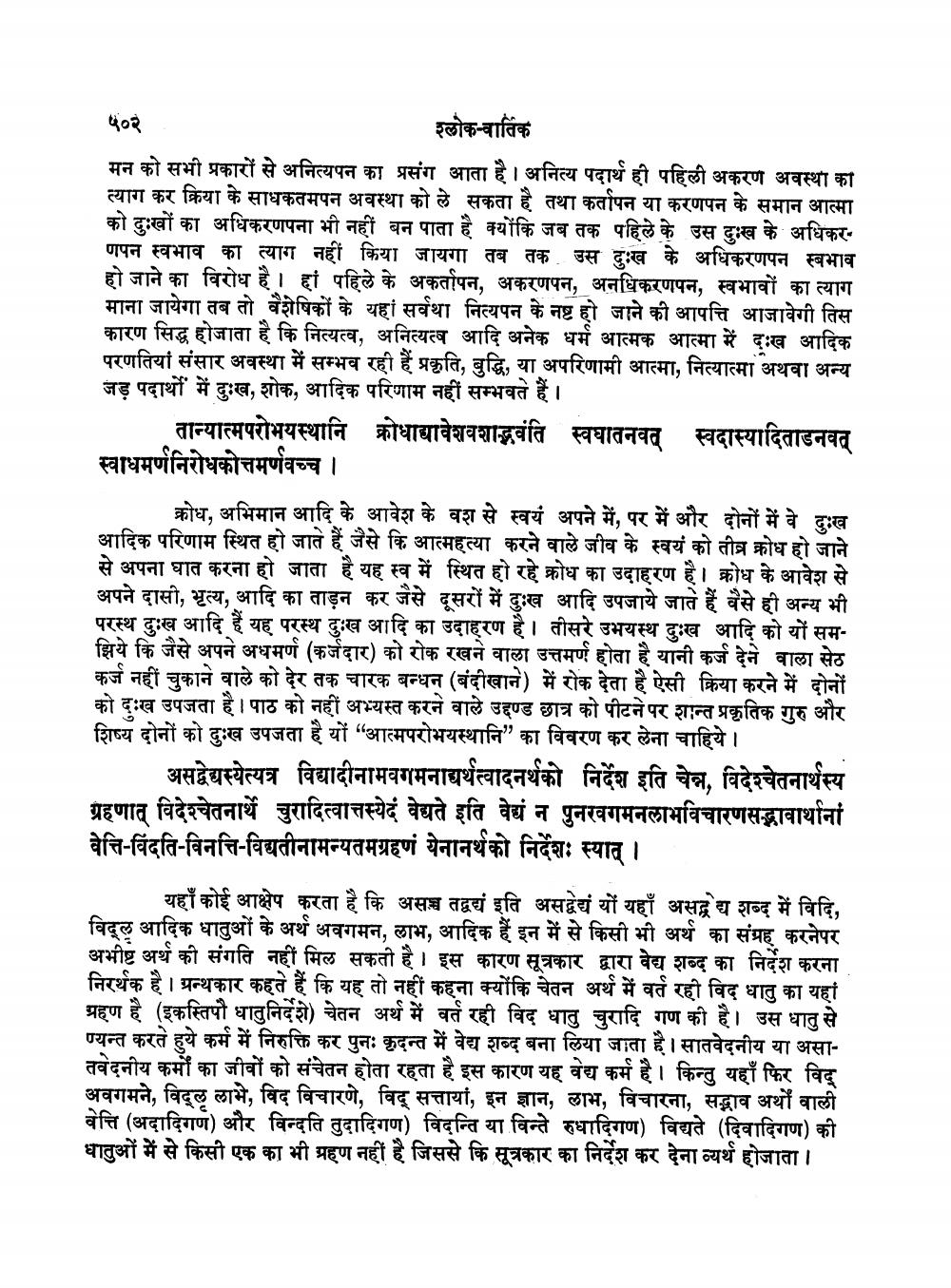________________
५०२
श्लोक-वार्तिक मन को सभी प्रकारों से अनित्यपन का प्रसंग आता है। अनित्य पदार्थ ही पहिली अकरण अवस्था का त्याग कर क्रिया के साधकतमपन अवस्था को ले सकता है तथा कर्तापन या करणपन के समान आत्मा को दुःखों का अधिकरणपना भी नहीं बन पाता है क्योंकि जब तक पहिले के उस दुःख के अधिकरणपन स्वभाव का त्याग नहीं किया जायगा तब तक उस दुःख के अधिकरणपन स्वभाव हो जाने का विरोध है। हां पहिले के अकर्तापन, अकरणपन, अनधिकरणपन, स्वभावों का त्याग माना जायेगा तब तो वैशेषिकों के यहां सर्वथा नित्यपन के नष्ट हो जाने की आपत्ति आजावेगी तिस कारण सिद्ध होजाता है कि नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धर्म आत्मक आत्मा में दःख आदिक परणतियां संसार अवस्था में सम्भव रही हैं प्रकृति, बुद्धि, या अपरिणामी आत्मा, नित्यात्मा अथवा अन्य जड़ पदार्थों में दुःख, शोक, आदिक परिणाम नहीं सम्भवते हैं ।
___तान्यात्मपरोभयस्थानि क्रोधाद्यावेशवशाद्भवंति स्वघातनवत् स्वदास्यादिताडनवत् स्वाधमर्णनिरोधकोत्तमर्णवच्च ।
क्रोध, अभिमान आदि के आवेश के वश से स्वयं अपने में, पर में और दोनों में वे दुःख आदिक परिणाम स्थित हो जाते हैं जैसे कि आत्महत्या करने वाले जीव के स्वयं को तीव्र क्रोध हो जाने से अपना घात करना हो जाता है यह स्व में स्थित हो रहे क्रोध का उदाहरण है। क्रोध के आवेश से अपने दासी, भृत्य, आदि का ताड़न कर जैसे दूसरों में दुःख आदि उपजाये जाते हैं वैसे ही अन्य भी परस्थ दुःख आदि हैं यह परस्थ दुःख आदि का उदाहरण है। तीसरे उभयस्थ दुःख आदि को यों समझिये कि जैसे अपने अधमर्ण (कर्जदार) को रोक रखने वाला उत्तमर्ण होता है यानी कर्ज देने वाला सेठ कर्ज नहीं चुकाने वाले को देर तक चारक बन्धन (बंदीखाने) में रोक देता है ऐसी क्रिया करने में दोनों को दःख उपजता है। पाठ को नहीं अभ्यस्त करने वाले उद्दण्ड छात्र को पीटने पर शान्त प्रकृतिक गुरु और शिष्य दोनों को दुःख उपजता है यों "आत्मपरोभयस्थानि" का विवरण कर लेना चाहिये।
असद्वेद्यस्येत्यत्र विद्यादीनामवगमनाद्यर्थत्वादनर्थको निर्देश इति चेन्न, विदेश्चेतनार्थस्य ग्रहणात् विदेश्चेतनार्थे चुरादित्वात्तस्येदं वेद्यते इति वेद्यं न पुनरवगमनलाभविचारणसद्भावार्थानां वेत्ति-विंदति-विनत्ति-विद्यतीनामन्यतमग्रहणं येनानर्थको निर्देशः स्यात् ।
यहाँ कोई आक्षेप करता है कि असञ्च तद्वद्यं इति असद्वेद्यं यों यहाँ असदुद्य शब्द में विदि, विद्ल आदिक धातुओं के अर्थ अवगमन, लाभ, आदिक हैं इन में से किसी भी अर्थ का संग्रह करनेपर अभीष्ट अर्थ की संगति नहीं मिल सकती है। इस कारण सूत्रकार द्वारा वेद्य शब्द का निर्देश करना निरर्थक है । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि चेतन अर्थ में वर्त रही विद धातु का यहां ग्रहण है (इकस्तिपौ धातुनिदेशे) चेतन अर्थ में वर्त रही विद धातु चुरादि गण की है। उस धातु से ण्यन्त करते हुये कर्म में निरुक्ति कर पुनः कृदन्त में वेद्य शब्द बना लिया जाता है। सातवेदनीय या असातवेदनीय कमों का जीवों को संचेतन होता रहता है इस कारण यह वेद्य कर्म है। किन्तु यहाँ फिर विद् अवगमने, विद्ल लाभे, विद विचारणे, विद् सत्तायां, इन ज्ञान, लाभ, विचारना, सद्भाव अर्थों वाली वेत्ति (अदादिगण) और विन्दति तुदादिगण) विदन्ति या विन्ते रुधादिगण) विद्यते (दिवादिगण) की धातुओं में से किसी एक का भी ग्रहण नहीं है जिससे कि सूत्रकार का निर्देश कर देना व्यर्थ होजाता।