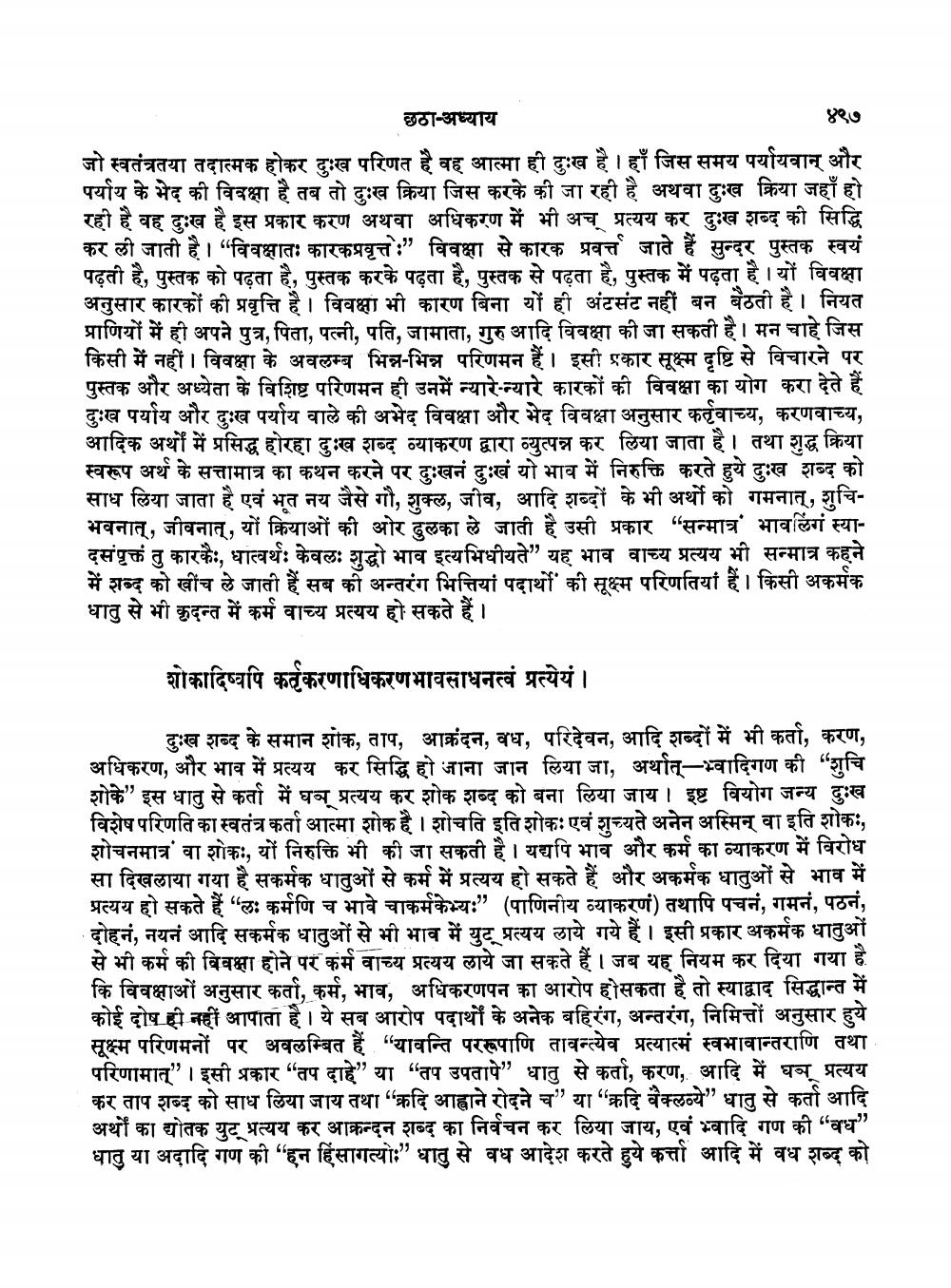________________
छठा अध्याय
४९७
जो स्वतंत्रतया तदात्मक होकर दुःख परिणत है वह आत्मा ही दुःख है । हाँ जिस समय पर्यायवान् और पर्याय के भेद की विवक्षा है तब तो दुःख क्रिया जिस करके की जा रही है अथवा दुःख क्रिया जहाँ हो ही है वह दुःख है इस प्रकार करण अथवा अधिकरण में भी अच् प्रत्यय कर दुःख शब्द की सिद्धि कर ली जाती है। “विवक्षातः कारकप्रवृत्तः” विवक्षा से कारक प्रवर्त्त जाते हैं सुन्दर पुस्तक स्वयं पढ़ती है, पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक करके पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक में 'पढ़ता है । यों विवक्षा अनुसार कारकों की प्रवृत्ति है । विवक्षा भी कारण बिना यों ही अंटसंट नहीं बन बैठती है । नियत प्राणियों में ही अपने पुत्र, पिता, पत्नी, पति, जामाता, गुरु आदि विवक्षा की जा सकती है। मन चाहे जिस किसी में नहीं । विवक्षा के अवलम्ब भिन्न-भिन्न परिणमन हैं । इसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर पुस्तक और अध्येता के विशिष्ट परिणमन ही उनमें न्यारे-न्यारे कारकों की विवक्षा का योग करा देते हैं। दुःख पर्याय और दुःख पर्याय वाले की अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा अनुसार कर्तृवाच्य, करणवाच्य, आदिक अर्थों में प्रसिद्ध होरहा दुःख शब्द व्याकरण द्वारा व्युत्पन्न कर लिया जाता है। तथा शुद्ध क्रिया स्वरूप अर्थ के सत्तामात्र का कथन करने पर दुःखनं दुःखं यो भाव में निरुक्ति करते हुये दुःख शब्द को साध लिया जाता है एवं भूत नय जैसे गौ, शुक्ल, जीव, आदि शब्दों के भी अर्थो को गमनात्, शुचिभवनात्, जीवनात्, यों क्रियाओं की ओर ढुलका ले जाती है उसी प्रकार " सन्मात्र भावलिंगं स्यादसंपृक्तं तु कारकैः, धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते" यह भाव वाच्य प्रत्यय भी सन्मात्र कहने शब्द को खींच ले जाती हैं सब की अन्तरंग भित्तियां पदार्थों की सूक्ष्म परिणतियां हैं। किसी अकर्मक धातु से भी कृदन्त में कर्म वाच्य प्रत्यय हो सकते हैं ।
शोकादिष्वपि कर्तृकरणाधिकरणभावसाधनत्वं प्रत्येयं ।
दुःख शब्द के समान शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, आदि शब्दों में भी कर्ता, करण, अधिकरण, और भाव में प्रत्यय कर सिद्धि हो जाना जान लिया जा, अर्थात् - भ्वादिगण की “शुचि शोके" इस धातु से कर्ता में घन् प्रत्यय कर शोक शब्द को बना लिया जाय । इष्ट वियोग जन्य दुःख विशेष परिणति का स्वतंत्र कर्ता आत्मा शोक है । शोचति इति शोकः एवं शुच्यते अनेन अस्मिन् वा इति शोकः, शोचनमात्र वा शोकः, यों निरुक्ति भी की जा सकती है । यद्यपि भाव और कर्म का व्याकरण में विरोध सा दिखलाया गया है सकर्मक धातुओं से कर्म में प्रत्यय हो सकते हैं और अकर्मक धातुओं से भाव में प्रत्यय हो सकते हैं “लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः” (पाणिनीय व्याकरणं) तथापि पचनं, गमनं, पठनं, दोहनं, नयनं आदि सकर्मक धातुओं से भी भाव में युट् प्रत्यय लाये गये हैं । इसी प्रकार अकर्मक धातुओं से भी कर्म की विवक्षा होने पर कर्म वाच्य प्रत्यय लाये जा सकते हैं । जब यह नियम कर दिया गया है. कि विवक्षाओं अनुसार कर्ता, कर्म, भाव, अधिकरणपन का आरोप होसकता है तो स्याद्वाद सिद्धान्त में कोई दोष ही नहीं आपाता है । ये सब आरोप पदार्थों के अनेक बहिरंग, अन्तरंग, निमित्तों अनुसार हुये सूक्ष्म परिणमनों पर अवलम्बित हैं " यावन्ति पररूपाणि तावन्त्येव प्रत्यात्मं स्वभावान्तराणि तथा परिणामात्” । इसी प्रकार " तप दाहे" या " तप उपतापे" धातु से कर्ता, करण, आदि में घन् प्रत्यय कर ताप शब्द को साध लिया जाय तथा " क्रदि आह्वाने रोदने च" या "क्रदि वैक्लव्ये" धातु से कर्ता आदि अर्थों का द्योतक प्रत्यय कर आक्रन्दन शब्द का निर्वचन कर लिया जाय, एवं भ्वादि गण की " व " धातु या अदादि गण की "हन हिंसागत्योः " धातु से वध आदेश करते हुये कर्त्ता आदि में वध शब्द को