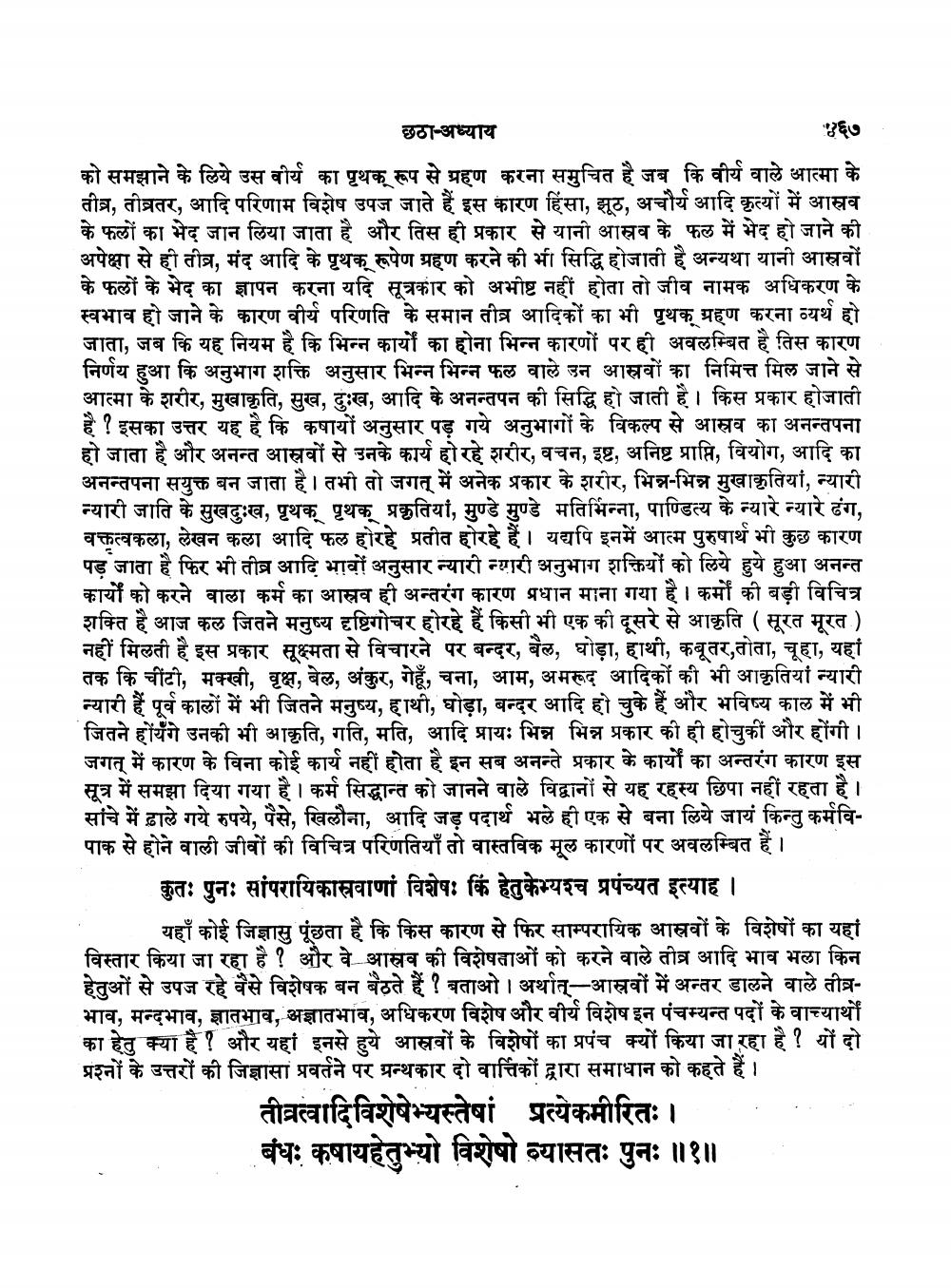________________
छठा अध्याय
४६७
को समझाने के लिये उस बीर्य का पृथक रूप से ग्रहण करना समुचित है जब कि वीर्य वाले आत्मा के तीव्र, तीव्रतर, आदि परिणाम विशेष उपज जाते हैं इस कारण हिंसा, झूठ, अचौर्य आदि कृत्यों में आस्रव के फलों का भेद जान लिया जाता है और तिस ही प्रकार से यानी आस्रव के फल में भेद हो जाने की अपेक्षा से ही तीव्र, मंद आदि के पृथक रूपेण ग्रहण करने की भी सिद्धि होजाती है अन्यथा यानी आस्रवों के फलों के भेद का ज्ञापन करना यदि सूत्रकार को अभीष्ट नहीं होता तो जीव नामक अधिकरण के स्वभाव हो जाने के कारण वीर्य परिणति के समान तीव्र आदिकों का भी पृथक ग्रहण करना व्यर्थ हो जाता, जब कि यह नियम है कि भिन्न कार्यों का होना भिन्न कारणों पर ही अवलम्बित है तिस कारण निर्णय हुआ कि अनुभाग शक्ति अनुसार भिन्न भिन्न फल वाले उन आस्रवों का निमित्त मिल जाने से आत्मा के शरीर, मुखाकृति, सुख, दुःख, आदि के अनन्तपन की सिद्धि हो जाती है । किस प्रकार होजाती है ? इसका उत्तर यह है कि कषायों अनुसार पड़ गये अनुभागों के विकल्प से आस्रव का अनन्तपना हो जाता है और अनन्त आस्रवों से उनके कार्य हो रहे शरीर, वचन, इष्ट, अनिष्ट प्राप्ति, वियोग, आदि का अनन्तपना सयुक्त बन जाता है। तभी तो जगत् में अनेक प्रकार के शरीर, भिन्न-भिन्न मुखाकृतियां, न्यारी न्यारी जाति के सुखदुःख, पृथक् पृथक् प्रकृतियां, मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना, पाण्डित्य के न्यारे न्यारे ढंग, वक्तृत्वकला, लेखन कला आदि फल होरहे प्रतीत होरहे हैं । यद्यपि इनमें आत्म पुरुषार्थ भी कुछ कारण पड़ जाता है फिर भी तीव्र आदि भावों अनुसार न्यारी न्यारी अनुभाग शक्तियों को लिये हुये हुआ अनन्त कार्यों को करने वाला कर्म का आस्रव ही अन्तरंग कारण प्रधान माना गया है । कर्मों की बड़ी विचित्र शक्ति है आज कल जितने मनुष्य दृष्टिगोचर होरहे हैं किसी भी एक की दूसरे से आकृति ( सूरत मूरत ) नहीं मिलती है इस प्रकार सूक्ष्मता से विचारने पर बन्दर, बैल, घोड़ा, हाथी, कबूतर, तोता, चूहा, यहां तक कि चींटी, मक्खी, वृक्ष, बेल, अंकुर, गेहूँ, चना, आम, अमरूद आदिकों की भी आकृतियां न्यारी न्यारी हैं पूर्व कालों में भी जितने मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बन्दर आदि हो चुके हैं और भविष्य काल में भी जितने होंगे उनकी भी आकृति, गति, मति, आदि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की ही होचुकीं और होंगी । जगत् में कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है इन सब अनन्ते प्रकार के कार्यों का अन्तरंग कारण इस सूत्र में समझा दिया गया है । कर्म सिद्धान्त को जानने वाले विद्वानों से यह रहस्य छिपा नहीं रहता है। सांचे में ढाले गये रुपये, पैसे, खिलौना, आदि जड़ पदार्थ भले ही एक से बना लिये जायं किन्तु कर्मविपाक से होने वाली जीवों की विचित्र परिणतियाँ तो वास्तविक मूल कारणों पर अवलम्बित हैं ।
कुतः पुनः सपरायिकास्त्रवाणां विशेषः किं हेतुकेभ्यश्च प्रपंच्यत इत्याह ।
यहाँ कोई जिज्ञासु पूंछता है कि किस कारण से फिर साम्परायिक आस्रवों के विशेषों का यहां विस्तार किया जा रहा है ? और वे आस्रव की विशेषताओं को करने वाले तीव्र आदि भाव भला किन तुओं से उपज रहे वैसे विशेषक बन बैठते हैं ? बताओ । अर्थात् - आस्रवों में अन्तर डालने वाले तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष इन पंचम्यन्त पदों के वाच्यार्थी है ? और यहां इनसे हुये आस्रवों के विशेषों का प्रपंच क्यों किया जा रहा है ? यों दो प्रश्नों के उत्तरों की जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार दो वार्त्तिकों द्वारा समाधान को कहते हैं ।
तीव्रत्वादिविशेषेभ्यस्तेषां प्रत्येकमीरितः । बंधः कषायहेतुभ्यो विशेषो व्यासतः पुनः ॥ १ ॥