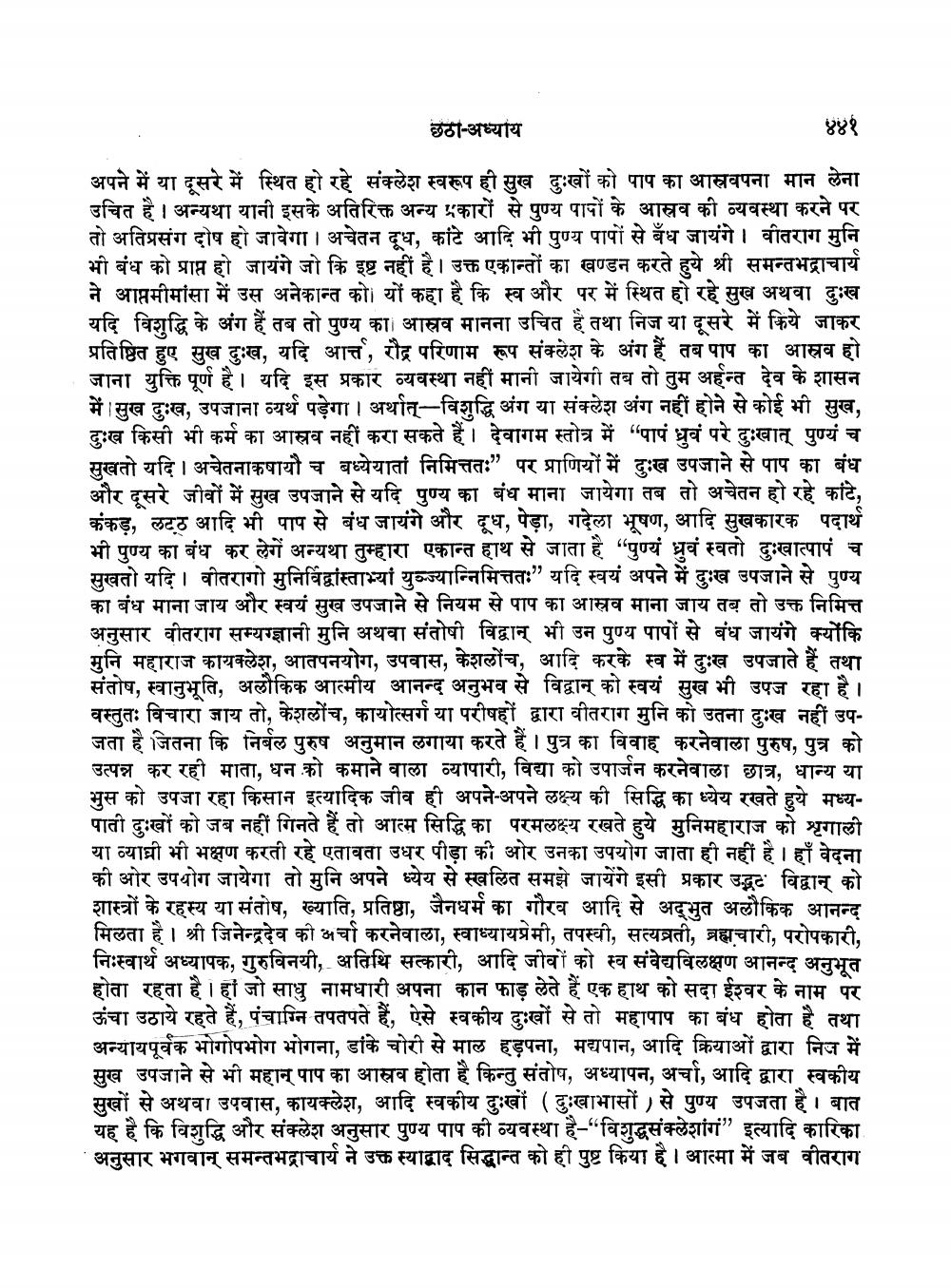________________
छठा-अध्याय
अपने में या दूसरे में स्थित हो रहे संक्लेश स्वरूप ही सुख दुःखों को पाप का आस्रवपना मान लेना उचित है । अन्यथा यानी इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारों से पुण्य पापों के आस्रव की व्यवस्था करने पर तो अतिप्रसंग दोष हो जावेगा। अचेतन दूध, कांटे आदि भी पुण्य पापों से बँध जायंगे। वीतराग मुनि भी बंध को प्राप्त हो जायंगे जो कि इष्ट नहीं है। उक्त एकान्तों का खण्डन करते हये श्री समन्तभद्राचार्य ने आप्तमीमांसा में उस अनेकान्त को यों कहा है कि स्व और पर में स्थित हो रहे सुख अथवा दुःख यदि विशुद्धि के अंग हैं तब तो पुण्य का आस्रव मानना उचित है तथा निज या दूसरे में किये जाकर प्रतिष्ठित हुए सुख दुःख, यदि आत, रौद्र परिणाम रूप संक्लेश के अंग हैं तब पाप का आस्रव हो जाना युक्ति पूर्ण है। यदि इस प्रकार व्यवस्था नहीं मानी जायेगी तब तो तुम अर्हन्त देव के शासन में । सुख दुःख, उपजाना व्यर्थ पड़ेगा। अर्थात्-विशुद्धि अंग या संक्लेश अंग नहीं होने से कोई भी सुख, दुःख किसी भी कर्म का आस्रव नहीं करा सकते हैं। देवागम स्तोत्र में “पापं ध्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सुखतो यदि । अचेतनाकषायौ च बध्येयातां निमित्ततः" पर प्राणियों में दुःख उपजाने से पाप का बंध
और दसरे जीवों में सख उपजाने से यदि पण्य का बंध माना जायेगा तब तो अचेतन हो रहे कांटे. कंकड़, लठ्ठ आदि भी पाप से बंध जायंगे और दूध, पेड़ा, गदेला भूषण, आदि सुखकारक पदार्थ भी पुण्य का बंध कर लेगें अन्यथा तुम्हारा एकान्त हाथ से जाता है "पुण्यं ध्रुवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युञ्ज्यान्निमित्ततः" यदि स्वयं अपने में दुःख उपजाने से पुण्य का बंध माना जाय और स्वयं सुख उपजाने से नियम से पाप का आस्रव माना जाय तब तो उक्त निमित्त अनुसार वीतराग सम्यग्ज्ञानी मुनि अथवा संतोषी विद्वान् भी उन पुण्य पापों से बंध जायंगे क्योंकि मुनि महाराज कायक्लेश, आतपनयोग, उपवास, केशलोंच, आदि करके स्व में दःख उपजाते हैं तथा संतोष, स्वानुभूति, अलौकिक आत्मीय आनन्द अनुभव से विद्वान् को स्वयं सुख भी उपज रहा है। वस्तुतः विचारा जाय तो, केशलोंच, कायोत्सर्ग या परीषहों द्वारा वीतराग मुनि को उतना दुःख नहीं उपजता है जितना कि निर्बल पुरुष अनुमान लगाया करते हैं । पुत्र का विवाह करनेवाला पुरुष, पुत्र को उत्पन्न कर रही माता, धन को कमाने वाला व्यापारी, विद्या को उपार्जन करनेवाला छात्र, धान्य या भुस को उपजा रहा किसान इत्यादिक जीव ही अपने-अपने लक्ष्य की सिद्धि का ध्येय रखते हुये मध्यपाती दुःखों को जब नहीं गिनते हैं तो आत्म सिद्धि का परमलक्ष्य रखते हुये मुनिमहाराज को शृगाली या व्याघ्री भी भक्षण करती रहे एतावता उधर पीड़ा की ओर उनका उपयोग जाता ही नहीं है । हाँ वेदना की ओर उपयोग जायेगा तो मुनि अपने ध्येय से स्खलित समझे जायेंगे इसी प्रकार उद्भट विद्वान् को शास्त्रों के रहस्य या संतोष, ख्याति, प्रतिष्ठा, जैनधर्म का गौरव आदि से अद्भुत अलौकिक आनन्द मिलता है। श्री जिनेन्द्रदेव की अर्चा करनेवाला, स्वाध्यायप्रेमी, तपस्वी, सत्यव्रती. ब्रह्मचारी. परोपकारी निःस्वार्थ अध्यापक, गुरुविनयी, अतिथि सत्कारी, आदि जीवों को स्व संवेद्यविलक्षण आनन्द अनुभूत होता रहता है । हाँ जो साधु नामधारी अपना कान फाड़ लेते हैं एक हाथ को सदा ईश्वर के नाम पर ऊंचा उठाये रहते हैं, पंचाग्नि तपतपते हैं, ऐसे स्वकीय दुःखों से तो महापाप का बंध होता है तथा अन्यायपूर्वक भोगोपभोग भोगना, डांके चोरी से माल हड़पना, मद्यपान, आदि क्रियाओं द्वारा निज में सुख उपजाने से भी महान पाप का आस्रव होता है किन्तु संतोष, अध्यापन, अर्चा, आदि द्वारा स्वकीय सुखों से अथवा उपवास, कायक्लेश, आदि स्वकीय दुःखों ( दुःखाभासों ) से पुण्य उपजता है। बात यह है कि विशुद्धि और संक्लेश अनुसार पुण्य पाप की व्यवस्था है-"विशुद्धसंक्लेशांग" इत्यादि कारिका अनुसार भगवान् समन्तभद्राचार्य ने उक्त स्याद्वाद सिद्धान्त को ही पुष्ट किया है । आत्मा में जब वीतराग