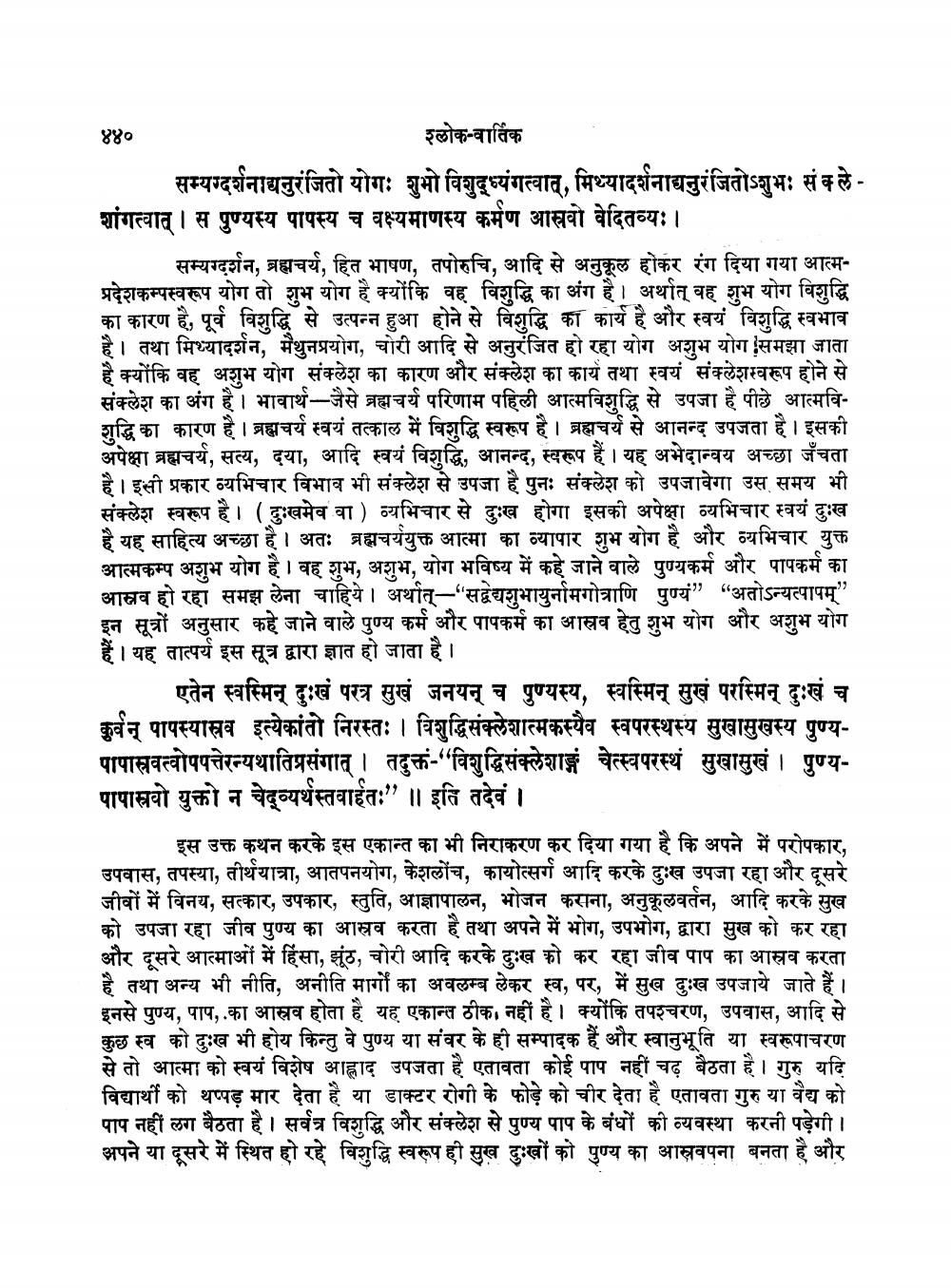________________
४४०
श्लोक-वार्तिक सम्यग्दर्शनाद्यनुरंजितो योगः शुभो विशुद्ध्यंगत्वात्, मिथ्यादर्शनाद्यनुरंजितोऽशुभः संकले - शांगत्वात् । स पुण्यस्य पापस्य च वक्ष्यमाणस्य कर्मण आस्रवो वेदितव्यः।
सम्यग्दर्शन, ब्रह्मचर्य, हित भाषण, तपोरुचि, आदि से अनुकूल होकर रंग दिया गया आत्मप्रदेशकम्पस्वरूप योग तो शुभ योग है क्योंकि वह विशुद्धि का अंग है। अर्थात् वह शुभ योग विशुद्धि का कारण है, पूर्व विशुद्धि से उत्पन्न हुआ होने से विशुद्धि का कार्य है और स्वयं विशुद्धि स्वभाव है। तथा मिथ्यादर्शन, मैथुनप्रयोग, चोरी आदि से अनुरंजित हो रहा योग अशुभ योग समझा जाता है क्योंकि वह अशुभ योग संक्लेश का कारण और संक्लेश का कार्य तथा स्वयं संक्लेशस्वरूप होने से संक्लेश का अंग है। भावार्थ-जैसे ब्रह्मचर्य परिणाम पहिली आत्मविशुद्धि से उपजा है पीछे आत्मविशुद्धि का कारण है । ब्रह्मचर्य स्वयं तत्काल में विशुद्धि स्वरूप है। ब्रह्मचर्य से आनन्द उपजता है। इसकी अपेक्षा ब्रह्मचर्य, सत्य, दया, आदि स्वयं विशुद्धि, आनन्द, स्वरूप हैं । यह अभेदान्वय अच्छा अँचता है। इसी प्रकार व्यभिचार विभाव भी संक्लेश से उपजा है पुनः संक्लेश को उपजावेगा उस समय भी संक्लेश स्वरूप है। ( दुःखमेव वा ) व्यभिचार से दुःख होगा इसकी अपेक्षा व्यभिचार स्वयं दुःख ह यह साहित्य अच्छा है। अतः ब्रह्मचययुक्त आत्मा का व्यापार शुभ योग है और व्यभिचार यक्त आत्मकम्प अशुभ योग है । वह शुभ, अशुभ, योग भविष्य में कहे जाने वाले पुण्यकर्म और पापकर्म का आस्रव हो रहा समझ लेना चाहिये । अर्थात्-"सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यं” “अतोऽन्यत्पापम्" इन सूत्रों अनुसार कहे जाने वाले पुण्य कर्म और पापकर्म का आस्रव हेतु शुभ योग और अशुभ योग हैं । यह तात्पर्य इस सूत्र द्वारा ज्ञात हो जाता है।
एतेन स्वस्मिन् दुःखं परत्र सुखं जनयन् च पुण्यस्य, स्वस्मिन् सुखं परस्मिन् दुःखं च कुर्वन् पापस्यास्रव इत्येकांतो निरस्तः । विशुद्धिसंक्लेशात्मकस्यैव स्वपरस्थस्य सुखासुखस्य पुण्यपापास्रवत्वोपपत्तेरन्यथातिप्रसंगात् । तदुक्तं-"विशुद्धिसंक्लेशाङ्गं चेत्स्वपरस्थं सुखासुखं । पुण्यपापासवो युक्तो न चेद्व्यर्थस्तवार्हतः" ॥ इति तदेवं ।
__ इस उक्त कथन करके इस एकान्त का भी निराकरण कर दिया गया है कि अपने में परोपकार, उपवास, तपस्या, तीर्थयात्रा, आतपनयोग, केशलोंच, कायोत्सर्ग आदि करके दुःख उपजा रहा और दूसरे जीवों में विनय, सत्कार, उपकार, स्तुति, आज्ञापालन, भोजन कराना, अनुकूलवर्तन, आदि करके सुख को उपजा रहा जीव पुण्य का आस्रव करता है तथा अपने में भोग, उपभोग, द्वारा सुख को कर रहा और दूसरे आत्माओं में हिंसा, झूठ, चोरी आदि करके दुःख को कर रहा जीव पाप का आस्रव करता है तथा अन्य भी नीति, अनीति मार्गों का अवलम्ब लेकर स्व, पर, में सुख दुःख उपजाये जाते हैं। इनसे पुण्य, पाप, .का आस्रव होता है यह एकान्त ठीक नहीं है। क्योंकि तपश्चरण, उपवास, आदि से कुछ स्व को दुःख भी होय किन्तु वे पुण्य या संवर के ही सम्पादक हैं और स्वानुभूति या स्वरूपाचरण से तो आत्मा को स्वयं विशेष आह्लाद उपजता है एतावता कोई पाप नहीं चढ़ बैठता है। गुरु यदि विद्यार्थी को थप्पड़ मार देता है या डाक्टर रोगी के फोड़े को चीर देता है एतावता गुरु या वैद्य को पाप नहीं लग बैठता है । सर्वत्र विशुद्धि और संक्लेश से पुण्य पाप के बंधों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने या दूसरे में स्थित हो रहे विशुद्धि स्वरूप ही सुख दुःखों को पुण्य का आस्रवपना बनता है और