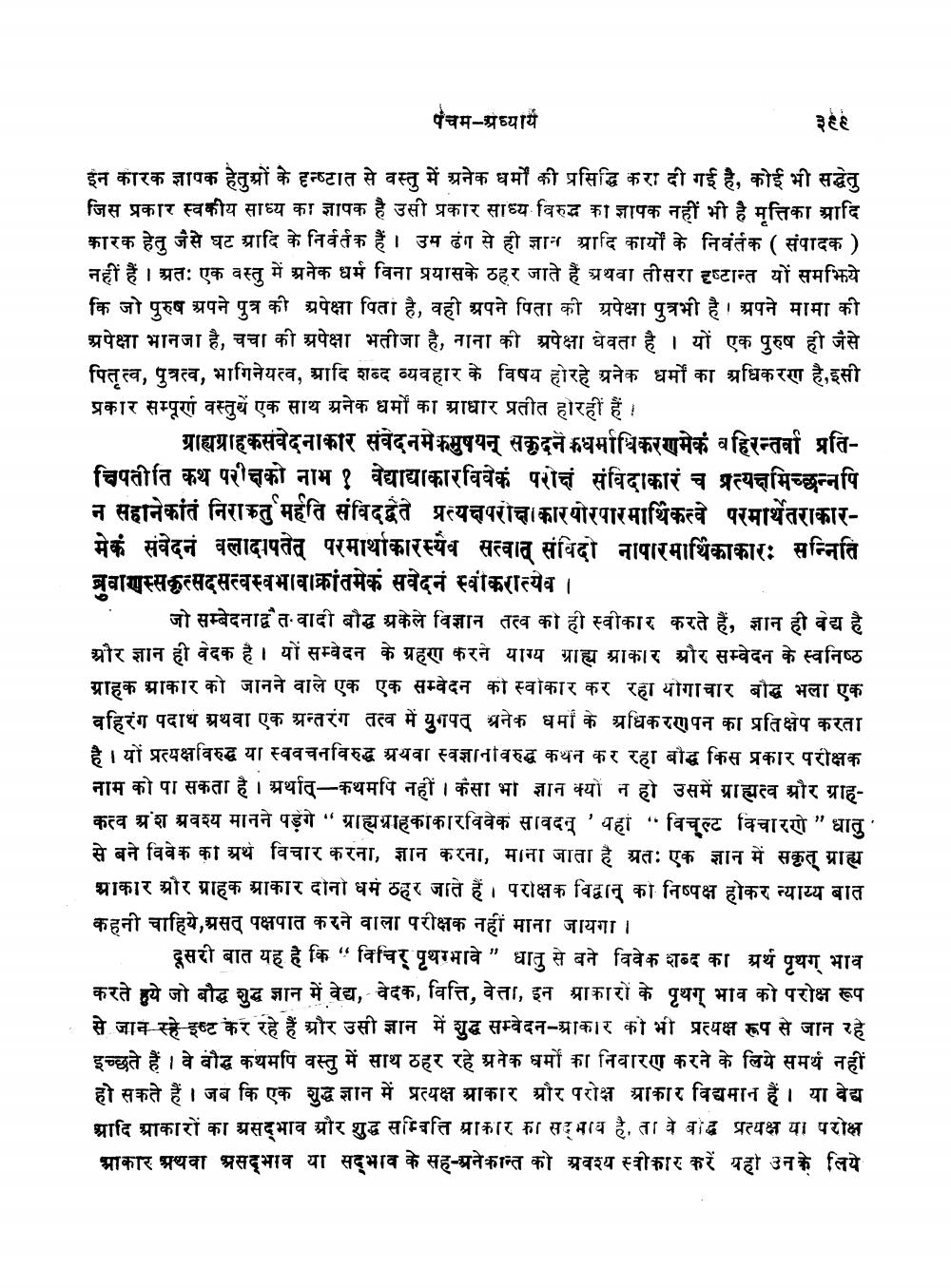________________
पंचम - श्रध्याय
३६६
इन कारक ज्ञापक हैतुओं के इन्ष्टात से वस्तु में अनेक धर्मों की प्रसिद्धि करा दी गई है, कोई भी सद्धे जिस प्रकार स्वकीय साध्य का ज्ञापक है उसी प्रकार साध्य विरुद्ध का ज्ञापक नहीं भी है मृत्तिका आदि कारक हेतु जैसे घट आदि के निर्वर्तक हैं । उस ढंग से ही ज्ञान आदि कार्यों के निवर्तक (संपादक ) नहीं हैं । अत: एक वस्तु में अनेक धर्म विना प्रयासके ठहर जाते हैं अथवा तीसरा दृष्टान्त यों समझिये कि जो पुरुष अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, वही अपने पिता की ग्रपेक्षा पुत्रभी है । अपने मामा की अपेक्षा भानजा है, चचा की अपेक्षा भतीजा है, नाना की अपेक्षा धेवता है । यों एक पुरुष ही जैसे पितृत्व, पुत्रत्व, भागिनेयत्व, आदि शब्द व्यवहार के विषय होरहे अनेक धर्मों का अधिकरण है, इसी प्रकार सम्पूर्ण वस्तुयें एक साथ अनेक धर्मों का आधार प्रतीत होरहीं हैं ।
ग्राह्यग्राहकसंवेदनाकार संवेदन मेकमुषयन् सकृदने कधर्माधिकरणमेकं वहिरन्तर्वा प्रतिचिपतीति कथ परीक्षको नाम ? वेद्याद्याकारविवेकं परोक्षं संविदाकारं च प्रत्यक्षमिच्छन्नपि नहानेकांतं निरातुमर्हति संविदद्वैते प्रत्यक्ष परोक्ष । कारयोरपारमार्थिकत्वे परमार्थेतराकारमेकं संवेदनं वलादापतेत् परमार्थाकारस्यैव सत्वात् संविदो नापारमार्थिकाकारः सन्निति ब्रुवाणस्सकृत्सदसत्वस्वभावाक्रांतमेकं सवेदनं स्वीकरात्येव ।
जो सम्बेदनाद्वैतवादी बौद्ध अकेले विज्ञान
तत्व को ही स्वीकार करते हैं, ज्ञान ही वेद्य है और ज्ञान ही वेदक है । यों सम्वेदन के ग्रहरण करने याग्य ग्राह्य आकार और सम्वेदन के स्वनिष्ठ ग्राहक आकार को जानने वाले एक एक सम्वेदन को स्वीकार कर रहा योगाचार बौद्ध भला एक वहिरंग पदार्थ अथवा एक अन्तरंग तत्व में युगपत् अनेक धर्मां के अधिकरणवन का प्रतिक्षेप करता है । यों प्रत्यक्षविरुद्ध या स्ववचनविरुद्ध अथवा स्वज्ञानविरुद्ध कथन कर रहा बौद्ध किस प्रकार परीक्षक नाम को पा सकता है । अर्थात् कथमपि नहीं । कैसा भी ज्ञान क्यों न हो उसमें ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व अंश अवश्य मानने पड़ेंगे " ग्राह्यग्राहकाकारविवेक सावदन् ' यहां "विचुल्ट विचारणे " धातु' से बने विवेक का अर्थ विचार करना, ज्ञान करना, माना जाता है अतः एक ज्ञान में सकृत् ग्राह्य लाकार और ग्राहक आकार दोनो धर्म ठहर जाते हैं। परोक्षक विद्वान् का निष्पक्ष होकर न्याय्य बात कहनी चाहिये, असत् पक्षपात करने वाला परीक्षक नहीं माना जायगा ।
दूसरी बात यह है कि " विचिर् पृथग्भावे " धातु से बने विवेक शब्द का अर्थ पृथग्भाव करते हुये जो बौद्ध शुद्ध ज्ञान में वेद्य, वेदक, वित्ति, वेत्ता, इन आकारों के पृथग् भाव को परोक्ष रूप से जान रहे इष्ट कर रहे हैं और उसी ज्ञान में शुद्ध सम्वेदन - प्रकार को भी प्रत्यक्ष रूप से जान रहे इच्छते हैं । वे बौद्ध कथमपि वस्तु में साथ ठहर रहे अनेक धर्मों का निवारण करने के लिये समर्थ नहीं हो सकते हैं । जब कि एक शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रकार और परोक्ष आकार विद्यमान हैं। या वेद्य आदि आकारों का असद्भाव और शुद्ध सम्बित्ति प्राकार का सद्भाव है, ता वे बोद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष आकार अथवा असद्भाव या सद्भाव के सह अनेकान्त को अवश्य स्वीकार करें यहां उनके लिये