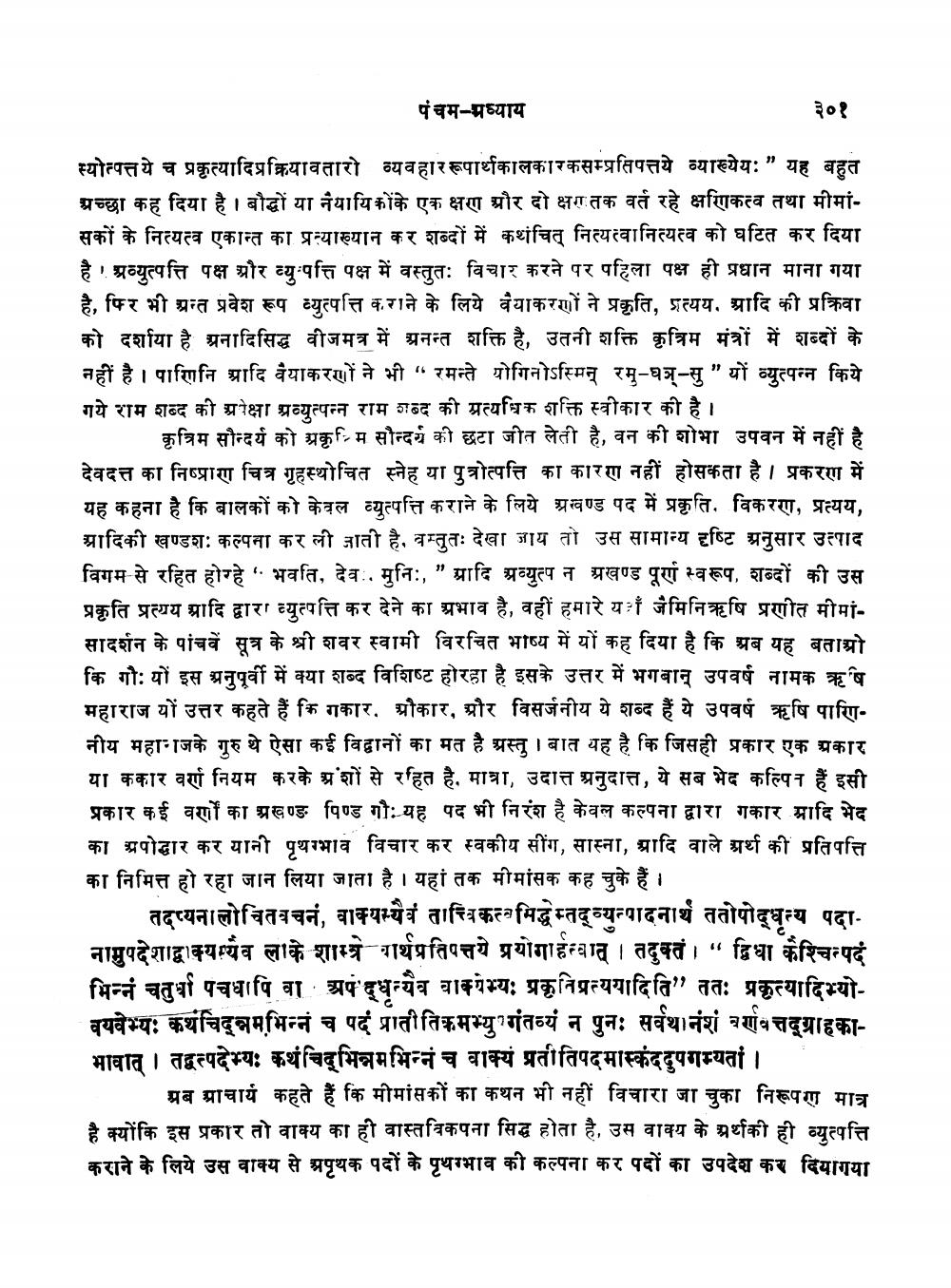________________
पंचम - अध्याय
३०१
19
स्योत्पत्तये च प्रकृत्यादिप्रक्रियावतारो व्यवहार रूपार्थकालकारकसम्प्रतिपत्तये व्याख्येयः यह बहुत अच्छा कह दिया है। बौद्धों या नैयायिकों के एक क्षरण और दो क्षण तक वर्त रहे क्षणिकत्व तथा मीमांसकों के नित्यत्व एकान्त का प्रत्याख्यान कर शब्दों में कथंचित् नित्यत्वानित्यत्व को घटित कर दिया है । व्युत्पत्ति पक्ष और व्युत्पत्ति पक्ष में वस्तुतः विचार करने पर पहिला पक्ष ही प्रधान माना गया है, फिर भी अन्त प्रवेश रूप व्युत्पत्ति कराने के लिये वैयाकरणों ने प्रकृति, प्रत्यय आदि की प्रक्रिवा को दर्शाया है अनादिसिद्ध वीजमंत्र में अनन्त शक्ति है, उतनी शक्ति कृत्रिम मंत्रों में शब्दों के नहीं है । पाणिनि आदि वैयाकरणों ने भी रमन्ते योगिनोऽस्मिन् रमु - घञ् - सु" यों व्युत्पन्न किये गये राम शब्द की अपेक्षा प्रव्युत्पन्न राम शब्द की प्रत्यधिक शक्ति स्वीकार की है ।
66
कृत्रिम सौन्दर्य को प्रकृत्रिम सौन्दर्य की छटा जीत लेती है, वन की शोभा उपवन में नहीं है देवदत्त का निष्प्राण चित्र गृहस्थोचित स्नेह या पुत्रोत्पत्ति का कारण नहीं होसकता है । प्रकरण में यह कहना है कि बालकों को केवल व्युत्पत्ति कराने के लिये प्रखण्ड पद में प्रकृति विकरण, प्रत्यय, आदिकी खण्डशः कल्पना कर ली जाती है, वस्तुतः देखा जाय तो उस सामान्य दृष्टि अनुसार उत्पाद विगम से रहित होरहे " भवति, देव: मुनिः, " प्रादि अव्युत्प न अखण्ड पूर्ण स्वरूप, शब्दों की उस प्रकृति प्रत्यय आदि द्वारा व्युत्पत्ति कर देने का अभाव है, वहीं हमारे यहाँ जैमिनिऋषि प्रणीत मीमांसादर्शन के पांचवें सूत्र के श्री शवर स्वामी विरचित भाष्य में यों कह दिया है कि अब यह बताओ कि गौ: यों इस अनुपूर्वी में क्या शब्द विशिष्ट होरहा है इसके उत्तर में भगवान् उपवर्ष नामक ऋषि महाराज यों उत्तर कहते हैं कि गकार प्रौकार, और विसर्जनीय ये शब्द हैं ये उपवर्ष ऋषि पारिणनीय महाराजके गुरु थे ऐसा कई विद्वानों का मत है अस्तु । बात यह है कि जिसही प्रकार एक प्रकार या ककार वर्ण नियम करके अशों से रहित है, मात्रा, उदात्त अनुदात्त, ये सब भेद कल्पित हैं इसी प्रकार कई वर्णों का अखण्ड पिण्ड गौ: यह पद भी निरंश है केवल कल्पना द्वारा गकार प्रादि भेद का अपोद्धार कर यानी पृथग्भाव विचार कर स्वकीय सींग, सास्ना, श्रादि वाले अर्थ की प्रतिपत्ति का निमित्त हो रहा जान लिया जाता है। यहां तक मीमांसक कह चुके हैं ।
तदप्यनालोचितवचनं, वाक्यस्यैवं तान्त्रिकत्वमिद्धेस्तद्व्युत्पादनार्थं ततोपोद्धृत्य पदानामुपदेशाद्वायैव लाके शास्त्रे वार्थप्रतिपत्तये प्रयोगार्हस्वात् । तदुक्तं । " द्विधा कैश्चित्पदं भिन्नं चतुर्धा पचधापि वा अपं द्धृत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिति” ततः प्रकृत्यादिभ्योवयवेभ्यः कथंचिन्नमभिन्नं च पदं प्रातीतिक्रमभ्यु गंतव्यं न पुनः सर्वथानंशं वर्णव तद्ग्राहकाभावात् । तद्वत्पदेभ्यः कथंचिद्भिन्नमभिन्नं च वाक्यं प्रतीतिपदमास्कंददुपगम्यतां ।
अब प्राचार्य कहते हैं कि मीमांसकों का कथन भी नहीं विचारा जा चुका निरूपण मात्र है क्योंकि इस प्रकार तो वाक्य का ही वास्तविकपना सिद्ध होता है, उस वाक्य के अर्थकी ही व्युत्पत्ति कराने के लिये उस वाक्य से पृथक पदों के पृथग्भाव की कल्पना कर पदों का उपदेश कर दियागया