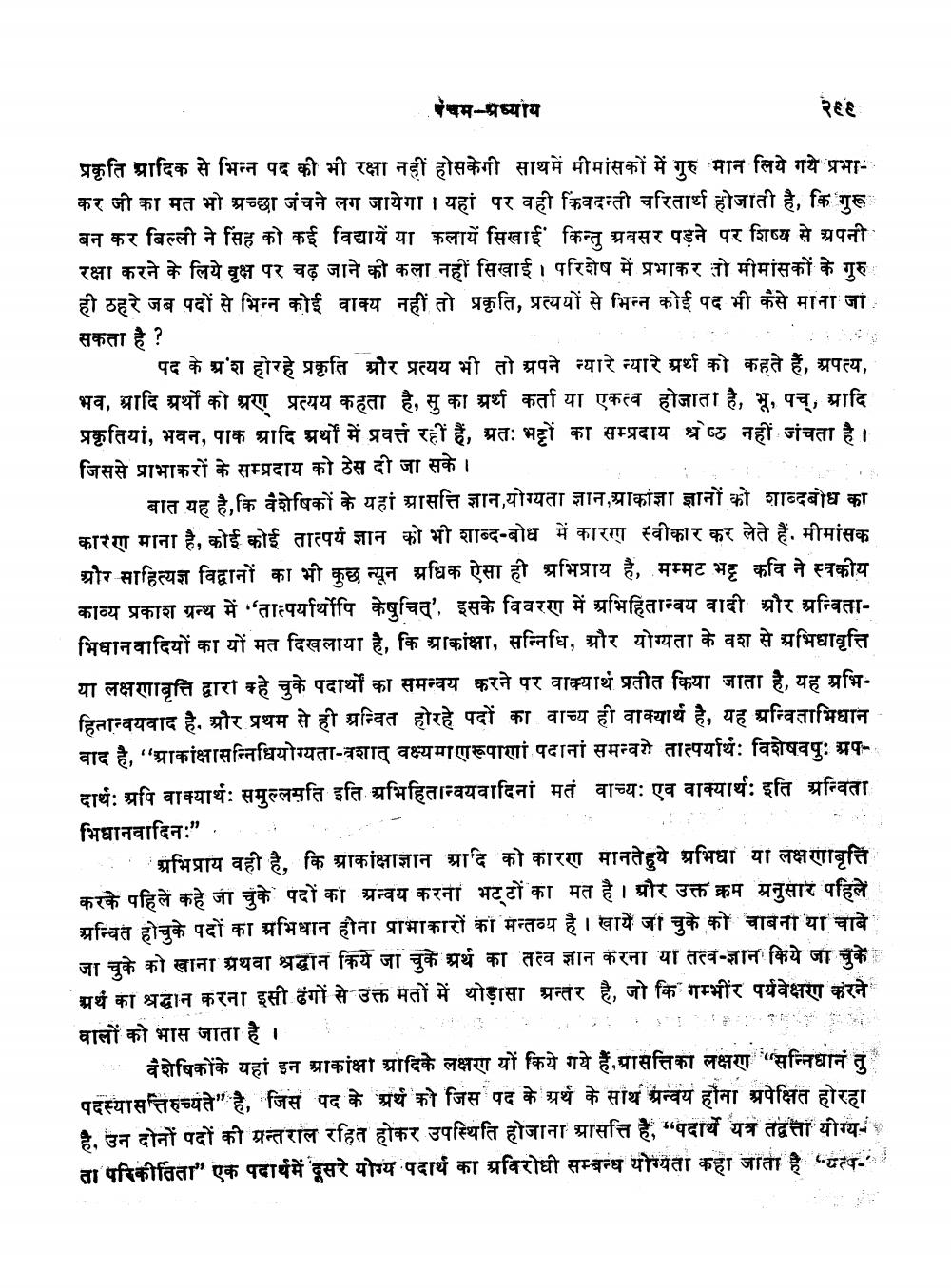________________
चम-अध्याय
२६९
प्रकृति प्रादिक से भिन्न पद की भी रक्षा नहीं होसकेगी साथ में मीमांसकों में गुरु मान लिये गये प्रभाकर जी का मत भो अच्छा जंचने लग जायेगा। यहां पर वही किंवदन्ती चरितार्थ होजाती है, कि 'गुरू बन कर बिल्ली ने सिंह को कई विद्यायें या कलायें सिखाई किन्तु अवसर पड़ने पर शिष्य से अपनी रक्षा करने के लिये वृक्ष पर चढ़ जाने की कला नहीं सिखाई। परिशेष में प्रभाकर तो मीमांसकों के गुरु ही ठहरे जब पदों से भिन्न कोई वाक्य नहीं तो प्रकृति, प्रत्ययों से भिन्न कोई पद भी कैसे माना जा सकता है ?
पद के अंश होरहे प्रकृति और प्रत्यय भी तो अपने न्यारे न्यारे अर्थ को कहते हैं, अपत्य, भव, प्रादि अर्थों को प्ररण प्रत्यय कहता है, सु का अर्थ कर्ता या एकत्व होजाता है, भू, पच्, प्रादि प्रकृतियां, भवन, पाक आदि अर्थों में प्रवत रहीं हैं, अतः भट्टों का सम्प्रदाय श्रेष्ठ नहीं जंचता है। जिससे प्राभाकरों के सम्प्रदाय को ठेस दी जा सके।
बात यह है,कि वैशेषिकों के यहां आसत्ति ज्ञान,योग्यता ज्ञान,आकांज्ञा ज्ञानों को शाब्दबोध का कारण माना है, कोई कोई तात्पर्य ज्ञान को भी शाब्द-बोध में कारण स्वीकार कर लेते हैं. मीमांसक
और साहित्यज्ञ विद्वानों का भी कुछ न्यून अधिक ऐसा ही अभिप्राय है, मम्मट भट्ट कवि ने स्वकीय काव्य प्रकाश ग्रन्थ में "तात्पर्यार्थोपि केषुचित्', इसके विवरण में अभिहितान्वय वादी और अन्विताभिधानवादियों का यों मत दिखलाया है, कि आकांक्षा, सन्निधि, और योग्यता के वश से अभिधावृत्ति या लक्षणावृत्ति द्वारा कहे चुके पदार्थों का समन्वय करने पर वाक्यार्थ प्रतीत किया जाता है, यह अभिहितान्वयवाद है. और प्रथम से ही अन्वित होरहे पदों का वाच्य ही वाक्यार्थ है, यह अन्विताभिधान वाद है, "अाकांक्षासन्निधियोग्यता-वशात् वक्ष्यमाणरूपाणां पदानां समन्वरो तात्पर्यार्थः विशेषवपुः अपदार्थः अपि वाक्यार्थः समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनां मतं वाच्यः एव वाक्यार्थः इति अन्विता भिधानवादिनः"
अभिप्राय वही है, कि आकांक्षाज्ञान आदि को कारण मानतेहुये अभिधा या लक्षणाबृत्ति करके पहिले कहे जा चुके पदों का अन्वय करना भटों का मत है । और उक्त क्रम अनुसार पहिले अन्वित होचुके पदों का अभिधान होना प्राभाकारों का मन्तव्य है । खाये जा चुके को चाबना या चाबे जा चुके को खाना अथवा श्रद्धान किये जा चुके अर्थ का तत्व ज्ञान करना या तत्व-ज्ञान किये जा चुके : अर्थ का श्रद्धान करना इसी ढंगों से उक्त मतों में थोड़ासा अन्तर है, जो कि गम्भीर पर्यवेक्षण करने वालों को भास जाता है।
४. वैशेषिकोंके यहां इन आकांक्षा आदिके लक्षण यों किये गये हैं,प्रासत्तिका लक्षण "सन्निधानं तू पदस्यासतिरुच्यते" है, जिस पद के अर्थ को जिस पद के अर्थ के साथ अन्वय होना अपेक्षित होरहा है, उन दोनों पदों की अन्तराल रहित होकर उपस्थिति होजाना प्रासत्ति है, "पदार्थे यत्र तद्वत्ता योग्य ता परिकीर्तिता" एक पदार्थमें दूसरे योग्य पदार्थ का अविरोधी सम्बन्ध योग्यता कहा जाता है "यत्प