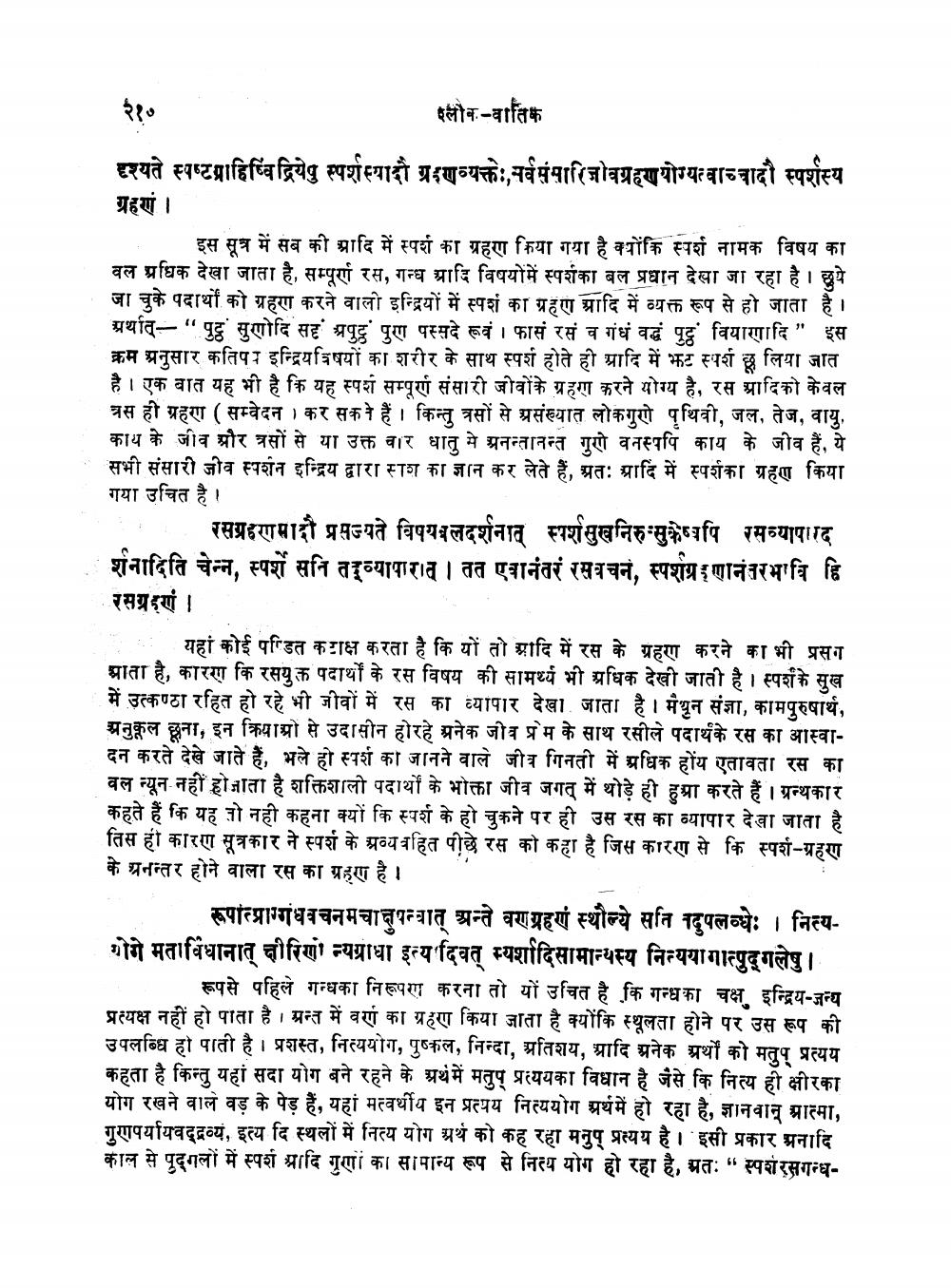________________
श्लोक - वार्तिक
दृश्यते स्पष्टग्राहिष्विद्रियेषु स्पर्शस्यादौ ग्रहणव्यक्तः, सर्व संसारिजोवग्रहण योग्यत्वाच्चादौ स्पर्शस्य
ग्रहणं ।
ܕܪ
इस
इस सूत्र में सब की आदि में स्पर्श का ग्रहण किया गया है क्योंकि स्पर्श नामक विषय का वल अधिक देखा जाता है, सम्पूर्ण रस, गन्ध आदि विषयों में स्पर्शका बल प्रधान देखा जा रहा है । छुये जा चुके पदार्थों को ग्रहण करने वाली इन्द्रियों में स्पर्श का ग्रहण आदि में व्यक्त रूप से हो जाता है । अर्थात् - " पुट्ठ सुगोदि सह पुट्ट पुरण पस्सदे रूवं । फासं रसं व गंधं वद्धं पुट्ठ वियागादि " क्रम अनुसार कतिपन इन्द्रियविषयों का शरीर के साथ स्पर्श होते ही श्रादि में झट स्पर्श छू लिया जात है। एक बात यह भी है कि यह स्पर्श सम्पूर्ण संसारी जीवोंके ग्रहण करने योग्य है, रस आदिको केवल सही ग्रहण ( सम्वेदन कर सकते हैं। किन्तु त्रसों से प्रसंख्यात लोकगुरणे पृथिवी, जल, तेज, वायु, काय के जीव और त्रसों से या उक्त वार धातु से अनन्तानन्त गुणे वनस्पति काय के जीव हैं, ये सभी संसारी जीव स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा सारा का ज्ञान कर लेते हैं, अतः प्रादि में स्पर्शका ग्रहण किया गया उचित 1
रसग्रहणमादौ प्रसज्यते विषयवलदर्शनात् स्पर्शसुखनिरु सुकेष्वपि रसव्यापारद र्शनादिति चेन्न, स्पर्शे सति तद्व्यापारात् । तत एवानंतरं रसवचनं, स्पर्शग्रहणानंतर भावि हि रसग्रहणं ।
यहां कोई पण्डित कटाक्ष करता है कि यों तो आदि में रस के ग्रहण करने का भी प्रसन ाता है, कारण कि रसयुक्त पदार्थों के रस विषय की सामर्थ्य भी अधिक देखी जाती है । स्पर्श के सुख में उत्कण्ठा रहित हो रहे भी जीवों में रस का व्यापार देखा जाता है । मैथुन संज्ञा, कामपुरुषार्थ, अनुकूलना, इन क्रियाओं से उदासीन होरहे अनेक जीव प्र ेम के साथ रसीले पदार्थंके रस का आस्वादन करते देखे जाते हैं, भले हो स्पर्श का जानने वाले जीव गिनती में अधिक होंय एतावता रस का वल न्यून नहीं हो जाता है शक्तिशाली पदार्थों के भोक्ता जीव जगत् में थोड़े ही हुआ करते हैं । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नही कहना क्यों कि स्पर्श के हो चुकने पर ही उस रस का व्यापार देखा जाता है। तिस ही कारण सूत्रकार ने स्पर्श के अव्यवहित पीछे रस को कहा है जिस कारण से कि स्पर्श - ग्रहण के श्रनन्तर होने वाला रस का ग्रहण है ।
रूपात्प्राग्गंध वचन मचाक्षुपन्वात् अन्ते वणग्रहणं स्थौल्ये सति नदुपलब्धेः । नित्ययोगे मताविधानात् क्षीरिणां न्यग्राधा इत्यादिवत् स्यर्शादिसामान्यस्य नित्ययागात्पुद् गलेषु ।
रूप से पहिले गन्धका निरूपण करना तो यों उचित है कि गन्धका चक्षु इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है । ग्रन्त में वर्ण का ग्रहण किया जाता है क्योंकि स्थूलता होने पर उस रूप की उपलब्धि हो पाती है । प्रशस्त, नित्ययोग, पुष्कल, निन्दा, अतिशय, आदि अनेक अर्थों को मतुप् प्रत्यय कहता है किन्तु यहां सदा योग बने रहने के अर्थ में मतुप् प्रत्ययका विधान है जैसे कि नित्य ही क्षीरका योग रखने वाले वड़ के पेड़ हैं, यहां मत्वर्थीय इन प्रत्यय नित्ययोग अर्थ में हो रहा है, ज्ञानवान् आत्मा,
पर्यावद्द्रव्यं इत्यदि स्थलों में नित्य योग अर्थ को कह रहा मनुप् प्रत्यय है । इसी प्रकार श्रनादि काल से पुद्गलों में स्पर्श आदि गुणों का सामान्य रूप से नित्य योग हो रहा है, अतः " स्पर्शरसगन्ध