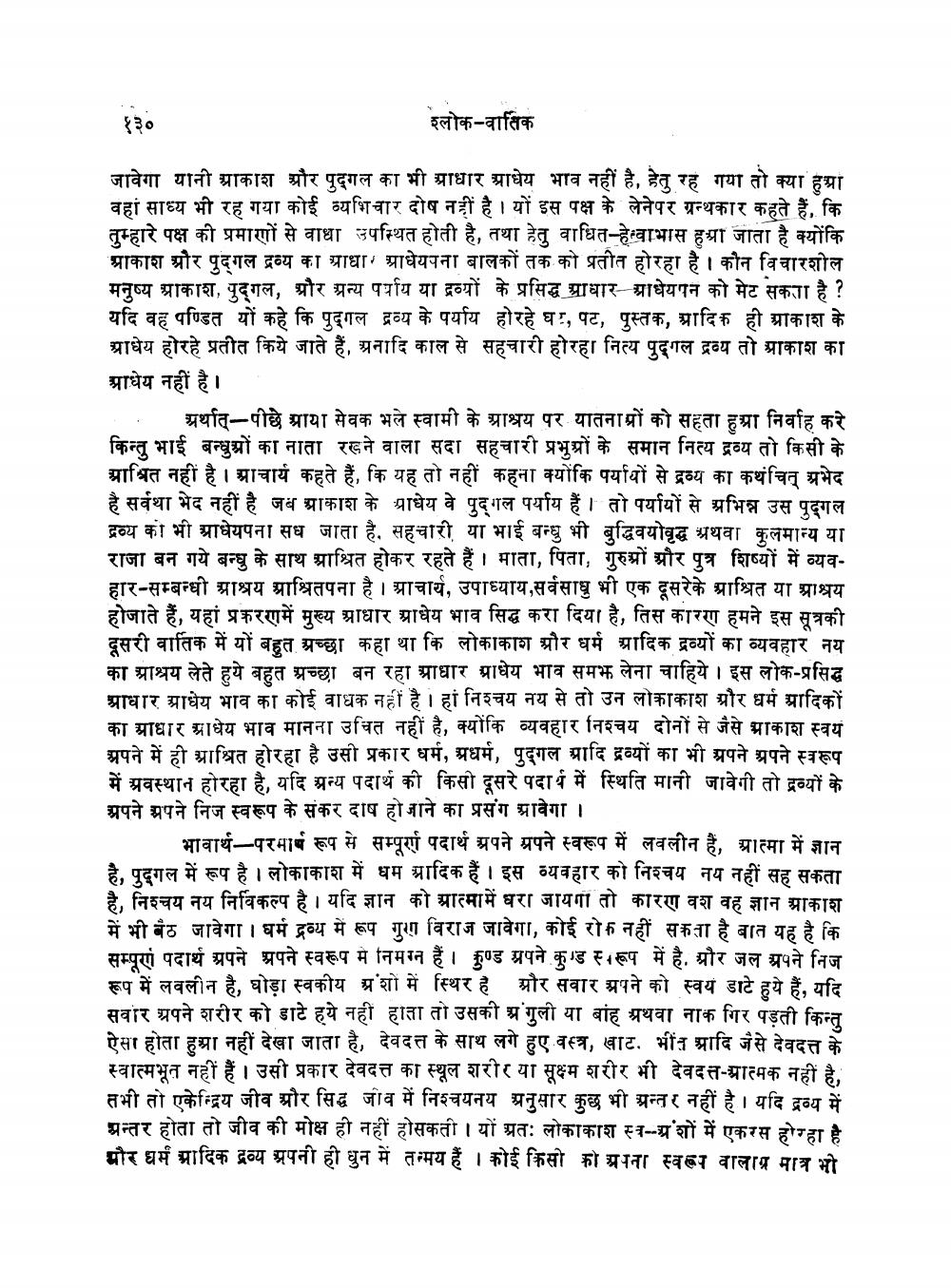________________
१३०
श्लोक - वार्तिक
जावेगा यानी आकाश और पुद्गल का भी आधार प्राधेय भाव नहीं है, हेतु रह गया तो क्या हुआ वहां साध्य भी रह गया कोई व्यभिचार दोष नहीं है । यों इस पक्ष के लेनेपर ग्रन्थकार कहते हैं, कि तुम्हारे पक्ष की प्रमाणों से वाधा उपस्थित होती है, तथा हेतु वाधित हेत्वाभास हुआ जाता है क्योंकि श्राकाश और पुद्गल द्रव्य का आधार आधेयपना बालकों तक को प्रतीत होरहा है। कौन विचारशील मनुष्य आकाश, पुद्गल, और अन्य पर्याय या द्रव्यों के प्रसिद्ध आधार - आधेयवन को मेट सकता है ? यदि वह पण्डित यों कहे कि पुद्गल द्रव्य के पर्याय हो रहे घर, पट, पुस्तक, आादिक ही प्रकाश के आधेय होरहे प्रतीत किये जाते हैं, अनादि काल से सहचारी होरहा नित्य पुद्गल द्रव्य तो आकाश का आय नहीं है ।
अर्थात् - पीछे श्राया सेवक भले स्वामी के प्रश्रय पर यातनाम्रों को सहता हुआ निर्वाह करे किन्तु भाई बन्धुओं का नाता रखने वाला सदा सहचारी प्रभुनों के समान नित्य द्रव्य तो किसी के श्रित नहीं है। आचार्य कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्योंकि पर्यायों से द्रव्य का कथंचित् प्रभेद है सर्वथा भेद नहीं है जब आकाश के प्राधेय वे पुद्गल पर्याय हैं। तो पर्यायों से भिन्न उस पुद्गल द्रव्य को भी आधेयपना सध जाता है, सहचारी या भाई बन्धु भी बुद्धिवयोवृद्ध अथवा कुलमान्य या राजा बन गये बन्धु के साथ श्राश्रित होकर रहते हैं । माता, पिता, गुरुनों और पुत्र शिष्यों में व्यव - हार-सम्बन्धी प्रश्रय श्राश्रितपना है । प्राचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु भी एक दूसरेके प्राश्रित या श्राश्रय होजाते हैं, यहां प्रकररणमें मुख्य आधार प्राधेय भाव सिद्ध करा दिया है, तिस कारण हमने इस सूत्र की दूसरी वार्तिक में यों बहुत अच्छा कहा था कि लोकाकाश और धर्म प्रादिक द्रव्यों का व्यवहार नय IT लेते हुये बहुत अच्छा बन रहा आधार प्राधेय भाव समझ लेना चाहिये । इस लोक - प्रसिद्ध आधार आधे भाव का कोई वाधक नहीं है । हां निश्चय नय से तो उन लोकाकाश और धर्म आदिकों का आधार प्रधेय भाव मानना उचित नहीं है, क्योंकि व्यवहार निश्चय दोनों से जैसे प्राकाश स्वयं अपने में ही आश्रित होरहा है उसी प्रकार धर्म, अधर्म, पुद्गल यादि द्रव्यों का भी अपने अपने स्वरूप स्थान होरहा है, यदि अन्य पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ में स्थिति मानी जावेगी तो द्रव्यों के अपने अपने निज स्वरूप के संकर दाष हो जाने का प्रसंग आवेगा ।
भावार्थ- परमार्थ रूप से सम्पूर्ण पदार्थ अपने प्रपने स्वरूप में लवलीन हैं, आत्मा में ज्ञान है, पुद्गल में रूप है । लोकाकाश में धम आदिक हैं । इस व्यवहार को निश्चय नय नहीं सह सकता है, निश्चय न निर्विकल्प है । यदि ज्ञान को आत्मा में घरा जायगा तो कारण वश वह ज्ञान आकाश में भी बैठ जावेगा । धर्म द्रव्य में रूप गुण विराज जावेगा, कोई रोक नहीं सकता है बात यह है कि सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने स्वरूप में निमग्न हैं । कुण्ड अपने कुड स्वरूप में है. और जल अपने निज रूप लवलीन है, घोड़ा स्वकीय अशों में स्थिर है और सवार अपने को स्वयं डाटे हुये हैं, यदि सवार अपने शरीर को डाटे ये नहीं होता तो उसकी अंगुली या बांह अथवा नाक गिर पड़ती किन्तु ऐसा होता हुआ नहीं देखा जाता है, देवदत्त के साथ लगे हुए वस्त्र, खाट भींत आदि जैसे देवदत्त के स्वात्मभूत नहीं हैं । उसी प्रकार देवदत्त का स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर भी देवदत्त - प्रात्मक नहीं है, तभी तो केन्द्रिय जीव और सिद्ध जीव में निश्चयनय अनुसार कुछ भी अन्तर नहीं है । यदि द्रव्य में अन्तर होता तो जीव की मोक्ष ही नहीं हो सकती । यों अतः लोकाकाश स्व-प्रशों में एकरस होरहा है और धर्म आदिक द्रव्य अपनी ही धुन में तन्मय हैं । कोई किसी को अपना स्वरूप वालाग्र मात्र भी