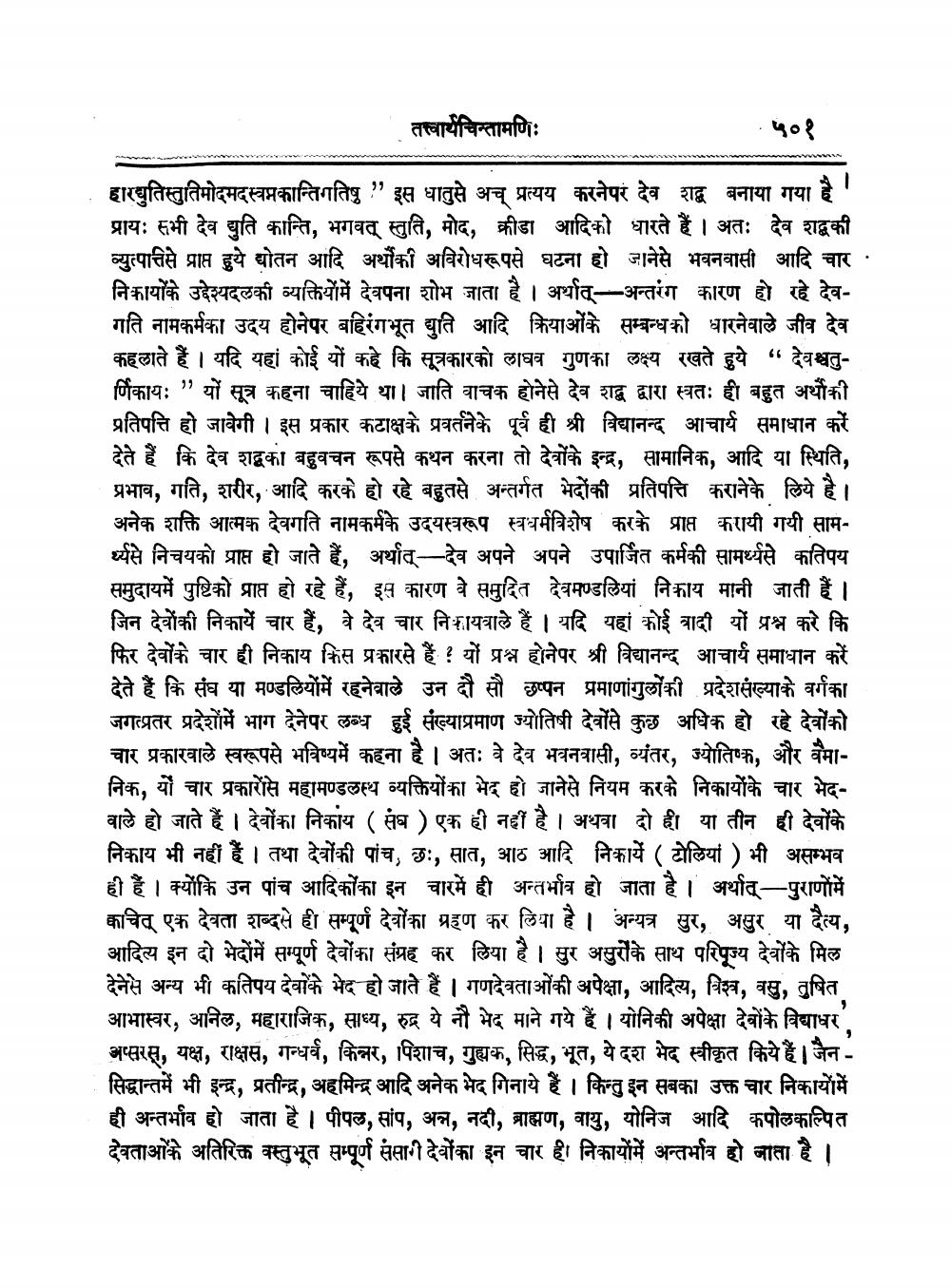________________
तत्त्वार्यचिन्तामणिः
हारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्मकान्तिगतिषु !” इस धातुसे अच् प्रत्यय करनेपर देव शब्द बनाया गया है। प्रायः सभी देव द्युति कान्ति, भगवत् स्तुति, मोद, क्रीडा आदिको धारते हैं । अतः देव शद्वकी व्युत्पत्तिसे प्राप्त हुये द्योतन आदि अर्थोकी अविरोधरूपसे घटना हो जानेसे भवनवासी आदि चार । निकायोंके उद्देश्यदलकी व्यक्तियोंमें देवपना शोभ जाता है । अर्थात् अन्तरंग कारण हो रहे देवगति नामकर्मका उदय होनेपर बहिरंगभूत द्युति आदि क्रियाओंके सम्बन्धको धारनेवाले जीव देव कहलाते हैं । यदि यहां कोई यों कहे कि सूत्रकारको लाघव गुणका लक्ष्य रखते हुये " देवश्चतुर्णिकायः " यों सूत्र कहना चाहिये था। जाति वाचक होनेसे देव शब्द द्वारा स्वतः ही बहुत अर्थोकी प्रतिपत्ति हो जावेगी । इस प्रकार कटाक्षके प्रवर्तनेके पूर्व ही श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान करें देते हैं कि देव शद्वका बहुवचन रूपसे कथन करना तो देवोंके इन्द्र, सामानिक, आदि या स्थिति, प्रभाव, गति, शरीर, आदि करके हो रहे बहुतसे अन्तर्गत भेदोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये है। अनेक शक्ति आत्मक देवगति नामकर्मके उदयस्वरूप स्वधर्मविशेष करके प्राप्त करायी गयी सामyसे निचयको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात्-देव अपने अपने उपार्जित कर्मकी सामर्थ्यसे कतिपय समुदायमें पुष्टिको प्राप्त हो रहे हैं, इस कारण वे समुदित देवमण्डलियां निकाय मानी जाती हैं। जिन देवोंकी निकायें चार हैं, वे देव चार निकायवाले हैं । यदि यहां कोई वादी यो प्रश्न करे कि फिर देवोंके चार ही निकाय किस प्रकारसे हैं ? यो प्रश्न होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान करें देते हैं कि संघ या मण्डलियोंमें रहनेवाले उन दौ सौ छप्पन प्रमाणांगुलोंकी प्रदेशसंख्याके वर्गका जगत्प्रतर प्रदेशोंमें भाग देनेपर लब्ध हुई संख्याप्रमाण ज्योतिषी देवोंसे कुछ अधिक हो रहे देवोंको चार प्रकारवाले स्वरूपसे भविष्यमें कहना है । अतः वे देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, और वैमानिक, यों चार प्रकारोंसे महामण्डलस्थ व्यक्तियों का भेद हो जानेसे नियम करके निकायोंके चार भेदवाले हो जाते हैं । देवोंका निकाय (संघ) एक ही नहीं है । अथवा दो ही या तीन ही देवोंके निकाय भी नहीं हैं । तथा देवोंकी पांच, छः, सात, आठ आदि निकायें ( टोलियां ) भी असम्भव ही हैं। क्योंकि उन पांच आदिकोंका इन चारमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। अर्थात्-पुराणोंमें कचित् एक देवता शब्दसे ही सम्पूर्ण देवोंका ग्रहण कर लिया है। अन्यत्र सुर, असुर या दैत्य, आदित्य इन दो भेदोंमें सम्पूर्ण देवोंका संग्रह कर लिया है । सुर असुरों के साथ परिपूज्य देवोंके मिल देनेसे अन्य भी कतिपय देवोंके भेद हो जाते हैं । गणदेवताओंकी अपेक्षा, आदित्य, विश्व, वसु, तुषित आभास्वर, अनिल, महाराजिक, साध्य, रुद्र ये नौ भेद माने गये हैं । योनिकी अपेक्षा देवों के विद्याधर अप्सरस्, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, भूत, ये दश भेद स्वीकृत किये हैं। जैन - सिद्धान्तमें भी इन्द्र, प्रतीन्द्र, अहमिन्द्र आदि अनेक भेद गिनाये हैं । किन्तु इन सबका उक्त चार निकायोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । पीपल, सांप, अन्न, नदी, ब्राह्मण, वायु, योनिज आदि कपोलकल्पित देवताओंके अतिरिक्त वस्तुभूत सम्पूर्ण संसारी देवोंका इन चार ही निकायोंमें अन्तर्भाव हो जाता है ।