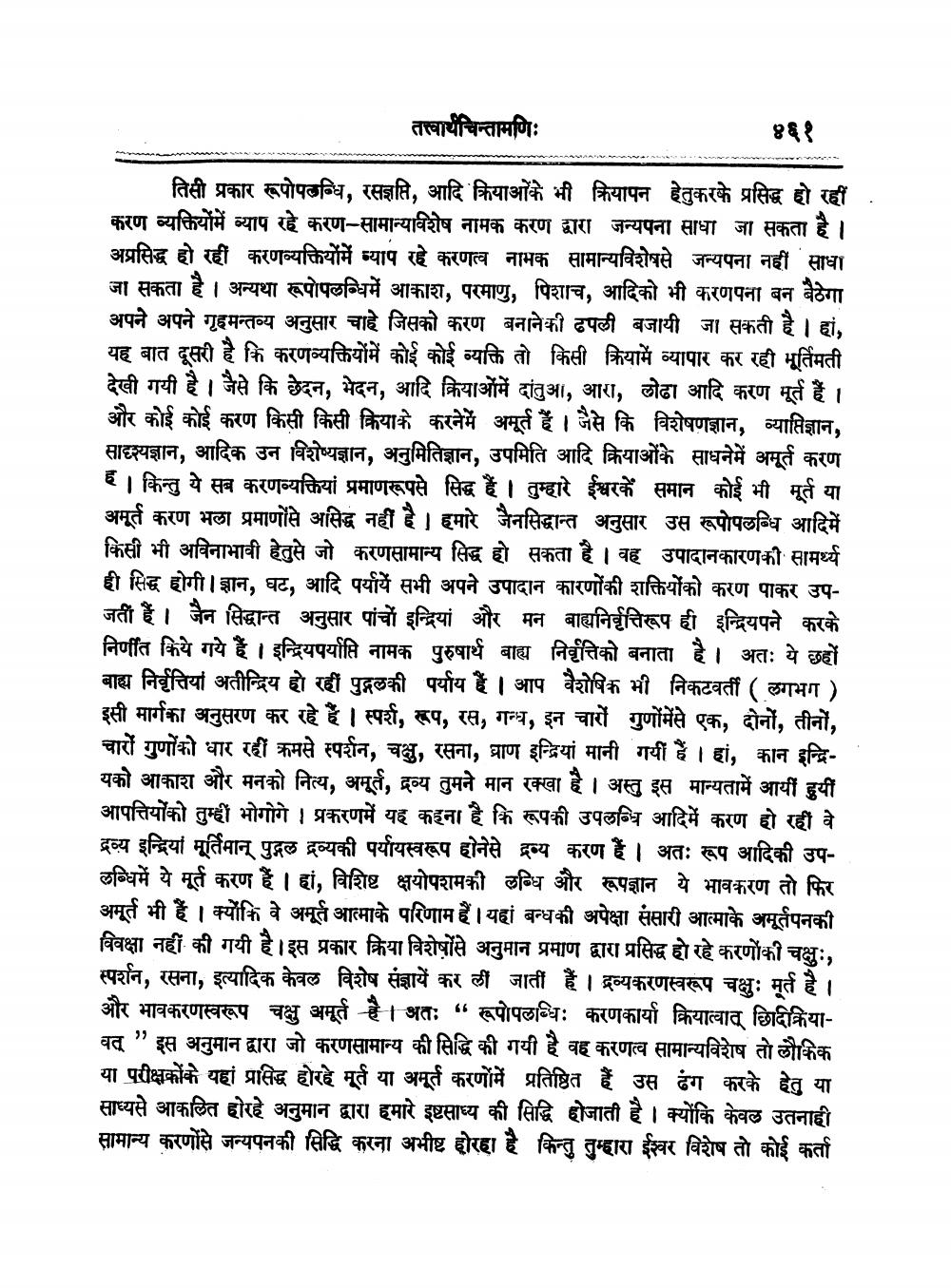________________
तत्त्वार्थचिन्तामणिः
४६१
1
तिसी प्रकार रूपोपलब्धि, रसज्ञप्ति, आदि क्रियाओंके भी क्रियापन हेतुकरके प्रसिद्ध हो रहीं करण व्यक्तियोंमें व्याप रहे करण - सामान्यविशेष नामक करण द्वारा जन्यपना साधा जा सकता है । अप्रसिद्ध हो रहीं करणव्यक्तियोंमें व्याप रहे करणत्व नामक सामान्यविशेषसे जन्यपना नहीं साधा जा सकता है । अन्यथा रूपोपलब्धिमें आकाश, परमाणु, पिशाच, आदिको भी करणपना बन बैठेगा अपने अपने गृहमन्तव्य अनुसार चाहे जिसको करण बनानेकी ढपली बजायी जा सकती है। हां, यह बात दूसरी है कि करणव्यक्तियोंमें कोई कोई व्यक्ति तो किसी क्रियामें व्यापार कर रही मूर्तिमती देखी गयी है । जैसे कि छेदन, भेदन, आदि क्रियाओंमें दांतुआ, आरा, लोढा आदि करण मूर्त हैं । और कोई कोई करण किसी किसी क्रिया के करनेमें अमूर्त हैं । जैसे कि विशेषणज्ञान, व्याप्तिज्ञान, सादृश्यज्ञान, आदिक उन विशेष्यज्ञान, अनुमितिज्ञान, उपमिति आदि क्रियाओंके साधनेमें अमूर्त करण ह | किन्तु ये सब करणव्यक्तियां प्रमाणरूपसे सिद्ध हैं । तुम्हारे ईश्वरकें समान कोई भी मूर्त या अमूर्त करण भला प्रमाणोंसे असिद्ध नहीं है। हमारे जैनसिद्धान्त अनुसार उस रूपोपलब्धि आदि में किसी भी अविनाभावी हेतुसे जो करणसामान्य सिद्ध हो सकता है । वह उपादानकारणकी सामर्थ्य ही सिद्ध होगी । ज्ञान, घट, आदि पर्यायें सभी अपने उपादान कारणोंकी शक्तियोंको करण पाकर उपजतीं हैं । जैन सिद्धान्त अनुसार पांचों इन्द्रियां और मन बाह्यनिर्वृत्तिरूप ही इन्द्रियपने करके निर्णीत किये गये हैं । इन्द्रियपर्याप्ति नामक पुरुषार्थ बाह्य निर्वृत्तिको बनाता है । अतः छहों बाह्य निर्वृत्तियां अतीन्द्रिय हो रहीं पुद्गलकी पर्याय हैं । आप वैशेषिक भी निकटवर्ती ( लगभग ) इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं । स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन चारों गुणोंमेंसे एक, दोनों, तीनों, 1 चारों गुणों को धार रहीं क्रमसे स्पर्शन, चक्षु, रसना, घ्राण इन्द्रियां मानी गयीं हैं। हां, कान इन्द्रियको आकाश और मनको नित्य, अमूर्त, द्रव्य तुमने मान रक्खा है । अस्तु इस मान्यतामें आयीं हुयीं आपत्तियों को तुम्हीं भोगोगे । प्रकरणमें यह कहना है कि रूपकी उपलब्धि आदिमें करण हो रहीं वे द्रव्य इन्द्रियां मूर्तिमान् पुद्गल द्रव्यकी पर्यायस्वरूप होनेसे द्रव्य करण हैं । अतः रूप आदिकी उपलब्धिमें ये मूर्त करण हैं। हां, विशिष्ट क्षयोपशमकी लब्धि और रूपज्ञान ये भावकरण तो फिर अमूर्त भी हैं। क्योंकि वे अमूर्त आत्माके परिणाम हैं। यहां बन्धकी अपेक्षा संसारी आत्माके अमूर्तपनकी विवक्षा नहीं की गयी है। इस प्रकार क्रिया विशेषोंसे अनुमान प्रमाण द्वारा प्रसिद्ध हो रहे करणों की चक्षुः, स्पर्शन, रसना, इत्यादिक केवल विशेष संज्ञायें कर लीं जातीं हैं । द्रव्यकरणस्वरूप चक्षुः मूर्त है । और भावकरणस्वरूप चक्षु अमूर्त है । अतः " रूपोपलब्धिः करणकार्या क्रियात्वात् छिदिक्रियावत् इस अनुमान द्वारा जो करणसामान्य की सिद्धि की गयी है वह करणत्व सामान्यविशेष तो लौकिक या परीक्षकों के यहां प्रसिद्ध होरहे मूर्त या अमूर्त करणोंमें प्रतिष्ठित हैं उस ढंग करके हेतु या साध्यसे आकलित होरहे अनुमान द्वारा हमारे इष्टसाध्य की सिद्धि होजाती है। क्योंकि केवल उतनाही सामान्य करणोंसे जन्यपनकी सिद्धि करना अभीष्ट होरहा है किन्तु तुम्हारा ईश्वर विशेष तो कोई कर्ता
ܙܙ