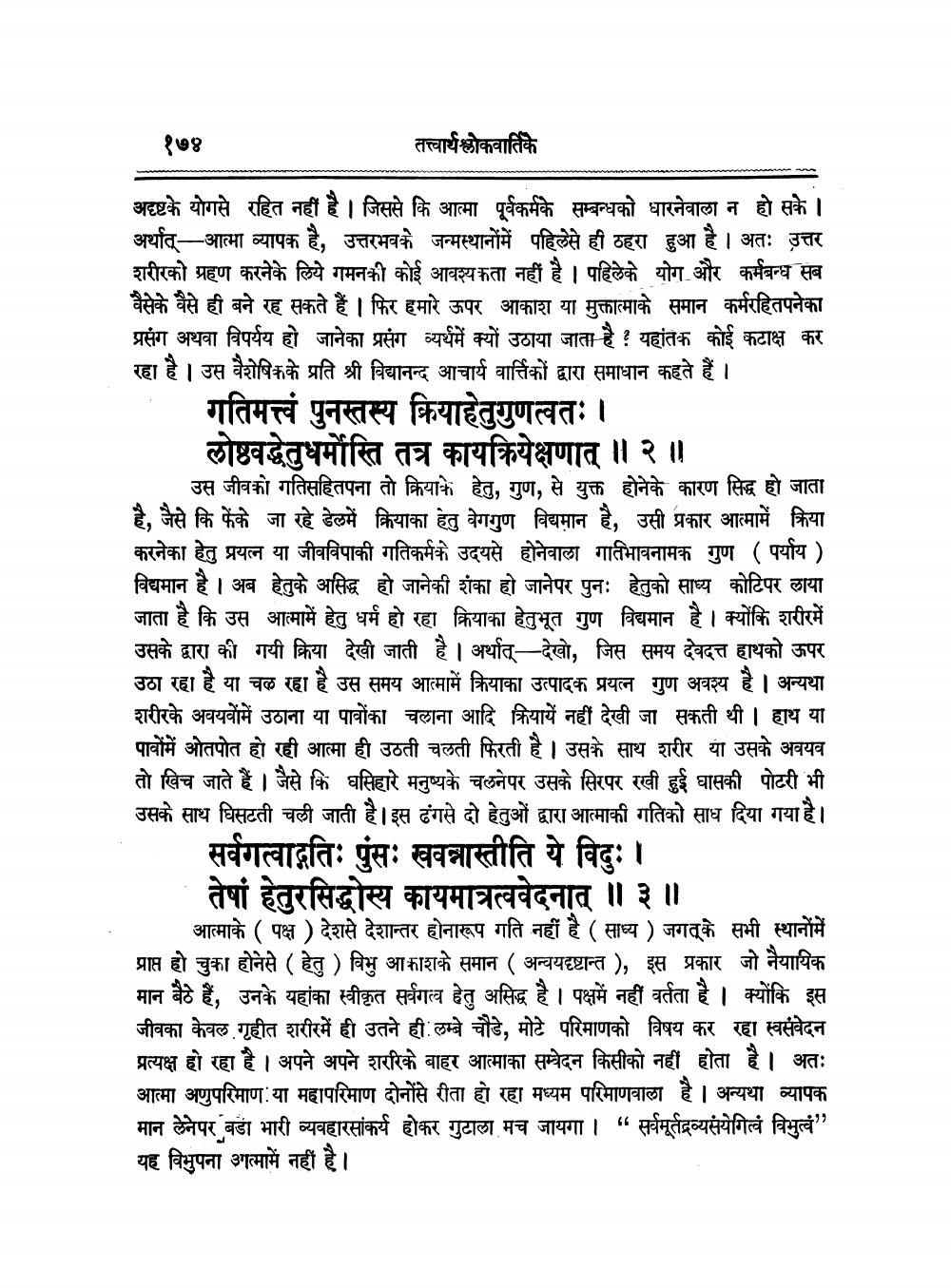________________
तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिके
अष्टके योगसे रहित नहीं है । जिससे कि आत्मा पूर्वकर्मके सम्बन्धको धारनेवाला न हो सके । अर्थात् — आत्मा व्यापक है, उत्तरभव के जन्मस्थानोंमें पहिलेसे ही ठहरा हुआ है । अतः उत्तर शरीरको ग्रहण करनेके लिये गमनकी कोई आवश्यकता नहीं है । पहिलेके योग और कर्मबन्ध सब I वैसे वैसे ही बने रह सकते हैं । फिर हमारे ऊपर आकाश या मुक्तात्मा के समान कर्मरहितपनेका प्रसंग अथवा विपर्यय हो जानेका प्रसंग व्यर्थमें क्यों उठाया जाता है ? यहांतक कोई कटाक्ष कर है । उस वैशेषिक के प्रति श्री विद्यानन्द आचार्य वार्त्तिकों द्वारा समाधान कहते हैं ।
रहा
१७४
गतिमत्त्वं पुनस्तस्य क्रियाहेतुगुणत्वतः । लोष्ठवद्धेतुधर्मोस्ति तत्र कायक्रियेक्षणात् ॥ २ ॥
समय देवदत्त हाथको ऊपर
उस जीवको गतिसहितपना तो क्रियाके हेतु, गुण, से युक्त होनेके कारण सिद्ध हो जाता है, जैसे कि फेंके जा रहे डेलमें क्रियाका हेतु वेगगुण विद्यमान है, उसी प्रकार आत्मामें क्रिया करनेका हेतु प्रयत्न या जीवविपाकी गतिकर्मके उदयसे होनेवाला गार्तभावनामक गुण ( पर्याय ) विद्यमान है । अब हेतुके असिद्ध हो जानेकी शंका हो जानेपर पुनः हेतुको साध्य कोटिपर लाया जाता है कि उस आत्मामें हेतु धर्म हो रहा क्रियाका हेतुभूत गुण विद्यमान है । क्योंकि शरीर में उसके द्वारा की गयी क्रिया देखी जाती है । अर्थात् — देखो, जिस उठा रहा है या चल रहा है उस समय आत्मामें क्रियाका उत्पादक प्रयत्न शरीर के अवयवोंमें उठाना या पावोंका चलाना आदि क्रियायें नहीं देखी जा सकती थी । हाथ या पावोंमें ओतपोत हो रही आत्मा ही उठती चलती फिरती है । उसके साथ शरीर या उसके अवयव तो खिच जाते हैं । जैसे कि घसिहारे मनुष्य के चलनेपर उसके सिरपर रखी हुई घासकी पोटरी भी उसके साथ घिसटती चली जाती है । इस ढंगसे दो हेतुओं द्वारा आत्माकी गतिको साध दिया गया है । सर्वगत्वाद्गतिः पुंसः खवन्नास्तीति ये विदुः ।
गुण अवश्य । अन्यथा
तेषां हेतुरसिद्धोस्य कायमात्रत्ववेदनात् ॥
३ ॥
आत्माके ( पक्ष ) देशसे देशान्तर होनारूप गति नहीं है ( साध्य ) जगत् के सभी स्थानोंमें प्राप्त हो चुका होनेसे ( हेतु ) विभु आकाश के समान ( अन्वयदृष्टान्त ), इस प्रकार जो नैयायिक मान बैठे हैं, उनके यहांका स्वीकृत सर्वगत्व हेतु असिद्ध है । पक्षमें नहीं वर्तता है । क्योंकि इस जीवका केवल गृहीत शरीर में ही उतने ही लम्बे चौडे, मोटे परिमाणको विषय कर रहा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो रहा है । अपने अपने शररिके बाहर आत्माका सम्वेदन किसीको नहीं होता है। अतः आत्मा अणुपरिमाण. या महापरिमाण दोनोंसे रीता हो रहा मध्यम परिमाणवाला है । अन्यथा व्यापक मान लेनेपर बडा भारी व्यवहारसांकर्य होकर गुटाला मच जायगा । "" सर्वमूर्तद्रव्यसंयेगित्वं विभुत्वं" यह विभुपना अगत्मामें नहीं है।