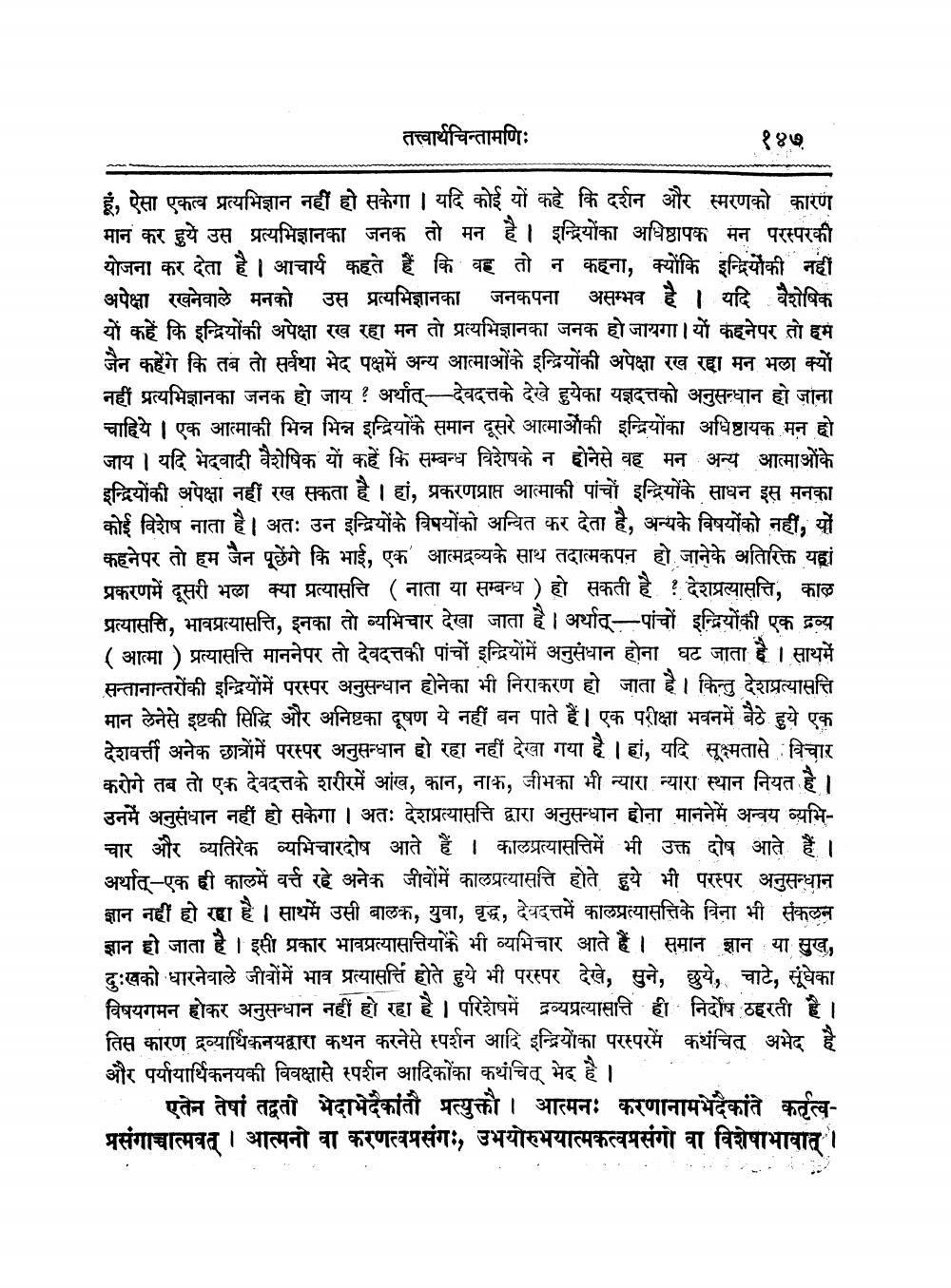________________
तत्त्वार्थचिन्तामणिः
१४७
m-
m
annamom
हूं, ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा । यदि कोई यों कहे कि दर्शन और स्मरणको कारण मान कर हुये उस प्रत्यभिज्ञानका जनक तो मन है। इन्द्रियोंका अधिष्ठापक मन परस्परकी योजना कर देता है । आचार्य कहते हैं कि वह तो न कहना, क्योंकि इन्द्रियोंकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले मनको उस प्रत्यभिज्ञानका जनकपना असम्भव है । यदि वैशेषिक यों कहें कि इन्द्रियोंकी अपेक्षा रख रहा मन तो प्रत्यभिज्ञानका जनक हो जायगा। यों कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि तब तो सर्वथा भेद पक्षमें अन्य आत्माओंके इन्द्रियोंकी अपेक्षा रख रहा मन भला क्यों नहीं प्रत्यभिज्ञानका जनक हो जाय ? अर्थात्-देवदत्तके देखे हुयेका यज्ञदत्तको अनुसन्धान हो जाना चाहिये । एक आत्माकी भिन्न भिन्न इन्द्रियोंके समान दूसरे आत्माओंकी इन्द्रियोंका अधिष्ठायक मन हो जाय । यदि भेदवादी वैशेषिक यों कहें कि सम्बन्ध विशेषके न होनेसे वह मन अन्य आत्माओंके इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रख सकता है । हां, प्रकरणप्राप्त आत्माकी पांचों इन्द्रियोंके साधन इस मनका कोई विशेष नाता है। अतः उन इन्द्रियों के विषयोंको अन्वित कर देता है, अन्यके विषयोंको नहीं, यों कहनेपर तो हम जैन पूठेंगे कि भाई, एक आत्मद्रव्यके साथ तदात्मकपन हो जानेके अतिरिक्त यहां प्रकरणमें दूसरी भला क्या प्रत्यासत्ति ( नाता या सम्बन्ध ) हो सकती है ? देशप्रत्यासत्ति, काल प्रत्यासत्ति, भावप्रत्यासत्ति, इनका तो व्यभिचार देखा जाता है । अर्थात्-पांचों इन्द्रियोंकी एक द्रव्य ( आत्मा ) प्रत्यासत्ति माननेपर तो देवदत्तकी पांचों इन्द्रियोंमें अनुसंधान होना घट जाता है । साथमें सन्तानान्तरोंकी इन्द्रियोंमें परस्पर अनुसन्धान होनेका भी निराकरण हो जाता है। किन्तु देशप्रत्यासत्ति मान लेनेसे इष्टकी सिद्धि और अनिष्टका दूषण ये नहीं बन पाते हैं। एक परीक्षा भवनमें बैठे हुये एक देशवर्ती अनेक छात्रोंमें परस्पर अनुसन्धान हो रहा नहीं देखा गया है । हां, यदि सूक्ष्मतासे विचार करोगे तब तो एक देवदत्तके शरीरमें आंख, कान, नाक, जीभका भी न्यारा न्यारा स्थान नियत है। उनमें अनुसंधान नहीं हो सकेगा । अतः देशप्रत्यासत्ति द्वारा अनुसन्धान होना माननेमें अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचारदोष आते हैं । कालप्रत्यासत्तिमें भी उक्त दोष आते हैं । अर्थात्-एक ही कालमें वर्त्त रहे अनेक जीवोंमें कालप्रत्यासत्ति होते हुये भी परस्पर अनुसन्धान ज्ञान नहीं हो रहा है । साथमें उसी बालक, युवा, वृद्ध, देवदत्तमें कालप्रत्यासत्तिके विना भी संकलन ज्ञान हो जाता है । इसी प्रकार भावप्रत्यासत्तियाके भी व्यभिचार आते हैं। समान ज्ञान या सुख, दुःखको धारनेवाले जीवोंमें भाव प्रत्यासत्तिं होते हुये भी परस्पर देखे, सुने, छुये, चाटे, सूंघेका विषयगमन होकर अनुसन्धान नहीं हो रहा है। परिशेषमें द्रव्यप्रत्यासत्ति ही निर्दोष ठहरती है। तिस कारण द्रव्यार्थिकनयद्वारा कथन करनेसे स्पर्शन आदि इन्द्रियोंका परस्परमें कथंचित् अभेद है और पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे स्पर्शन आदिकोंका कथंचित् भेद है। _____एतेन तेषां तद्वतो भेदाभेदैकांती प्रत्युक्तौ। आत्मनः करणानामभेदैकांते कर्तृत्वप्रसंगाचात्मवत् । आत्मनो वा करणत्वप्रसंगः, उभयोरुभयात्मकत्वासंगो वा विशेषाभावात् ।