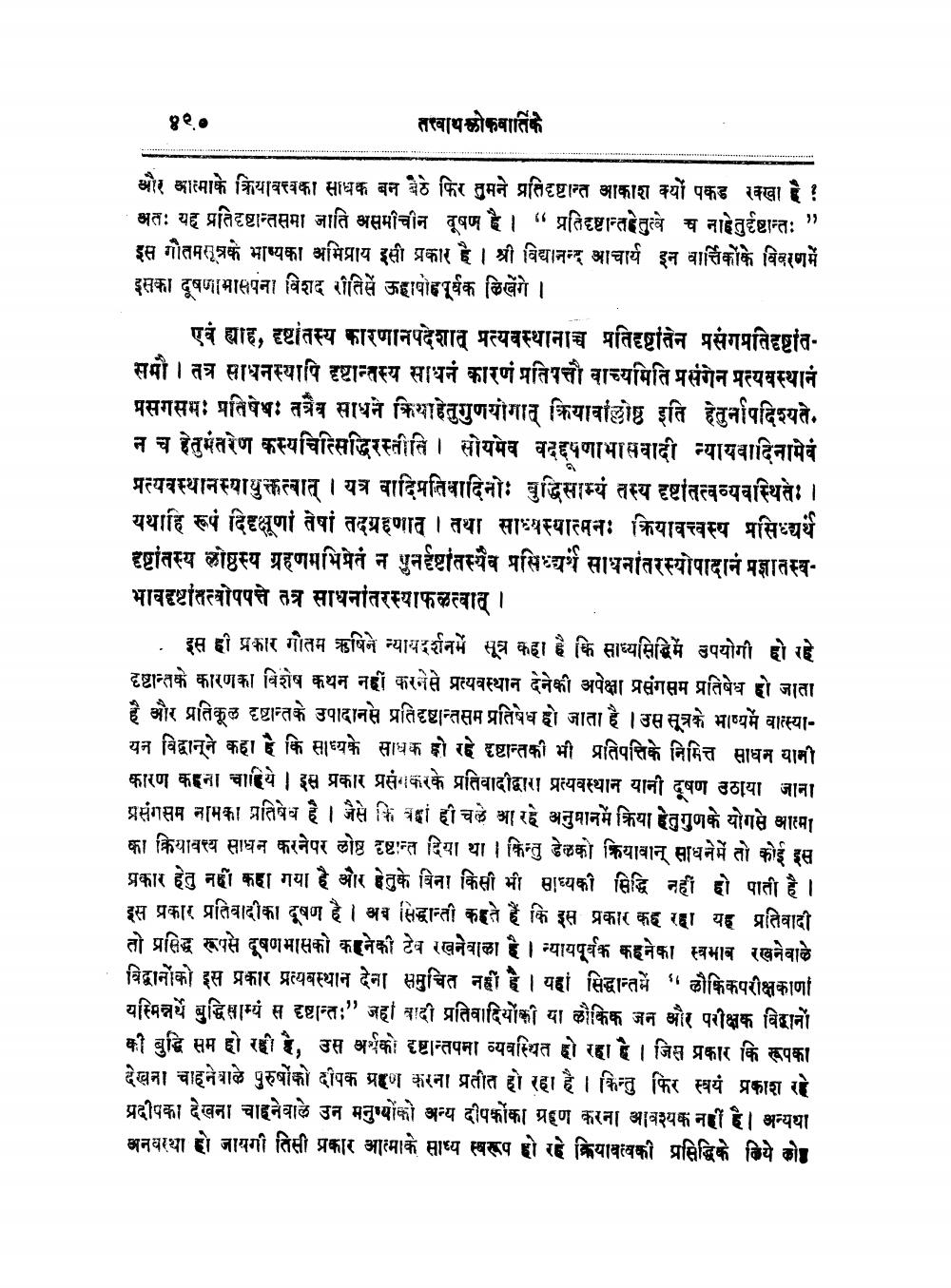________________
४९.
तत्वाथकोकवार्तिके
और आत्माके क्रियावत्वका साधक बन बैठे फिर तुमने प्रतिदृष्टान्त आकाश क्यों पकड रक्खा है ! अतः यह प्रतिदृष्टान्तसमा जाति असमीचीन दूषण है। " प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुर्दृष्टान्तः " इस गौतमसूत्रके भाष्यका अभिप्राय इसी प्रकार है । श्री विद्यानन्द आचार्य इन वार्तिकोंके विवरणमें इसका दूषणामासपना विशद रीतिसें ऊहापोहपूर्वक लिखेंगे ।
एवं ह्याह, दृष्टांतस्य कारणानपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टांतेन प्रसंगप्रतिदृष्टांतसमौ । तत्र साधनस्यापि दृष्टान्तस्य साधनं कारणं प्रतिपत्तौ वाच्यमिति प्रसंगेन प्रत्ययस्थान प्रसगसमः प्रतिषेधः तत्रैव साधने क्रियाहेतुगुणयोगात् क्रियावालोष्ठ इति हेतु पदिश्यते. न च हेतुमंतरेण कस्यचित्सिद्धिरस्तीति । सोयमेव वदद्दपणाभासवादी न्यायवादिनामेवं प्रत्यवस्थानस्यायुक्तत्वात् । यत्र वादिप्रतिवादिनोः बुद्धिसाम्यं तस्य दृष्टांतत्वव्यवस्थितेः । यथाहि रूपं दिदृक्षणां तेषां तदग्रहणात् । तथा साध्यस्यात्मनः क्रियावत्त्वस्य प्रसिध्यर्थ दृष्टांतस्य लोष्ठस्य ग्रहणमभिप्रेतं न पुनदृष्टांतस्यैव प्रसिध्द्यर्थ साधनांतरस्योपादानं प्रज्ञातस्वभावदृष्टांतत्वोपपत्ते तत्र साधनांतरस्याफलत्वात् ।
.. इस ही प्रकार गौतम ऋषिने न्यायदर्शनमें सूत्र कहा है कि साध्यसिद्धिमें उपयोगी हो रहे दृष्टान्तके कारणका विशेष कथन नहीं करनेसे प्रत्यवस्थान देनेकी अपेक्षा प्रसंगसम प्रतिषेध हो जाता है और प्रतिकूल दृष्टान्तके उपादानसे प्रति दृष्टान्तसम प्रतिषेध हो जाता है । उस सूत्रके भाष्यमें वात्स्यायन विद्वान्ने कहा है कि साध्य के साधक हो रहे दृष्टान्तकी भी प्रतिपत्तिके निमित्त साधम यानी कारण कहना चाहिये । इस प्रकार प्रसंगकारके प्रतिवादीद्वारा प्रत्यवस्थान यानी दूषण उठाया जाना प्रसंगसम नामका प्रतिषेध है । जैसे कि वहां ही चले आ रहे अनुमानमें क्रिया हेतुगुणके योगसे आत्मा का क्रियावत्य साधन करनेपर लोष्ठ दृष्टान्त दिया था। किन्तु डेलको क्रियावान् साधनेमें तो कोई इस प्रकार हेतु नहीं कहा गया है और हेतुके बिना किसी भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है । इस प्रकार प्रतिवादीका दूषण है । अब सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार कह रहा यह प्रतिवादी तो प्रसिद्ध रूपसे दूषणमासको कहनेकी टेव रखनेवाला है। न्यायपूर्वक कहनेका स्वभाव रखनेवाले विद्वानोंको इस प्रकार प्रत्यवस्थान देना समुचित नहीं है । यहां सिद्धान्तमें लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः" जहां वादी प्रतिवादियोंकी या लौकिक जन और परीक्षक विद्वानों की बुद्धि सम हो रही है, उस अर्थको दृष्टान्तपमा व्यवस्थित हो रहा है । जिस प्रकार कि रूपका देखना चाहने वाले पुरुषोंको दीपक ग्रहण करना प्रतीत हो रहा है । किन्तु फिर स्वयं प्रकाश रहे प्रदीपका देखना चाहनेवाले उन मनुष्योंको अन्य दीपकोंका ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। अन्यथा अनवस्था हो जायगी तिसी प्रकार आत्माके साध्य स्वरूप हो रहे क्रियावत्वकी प्रसिद्धि के लिये कोई