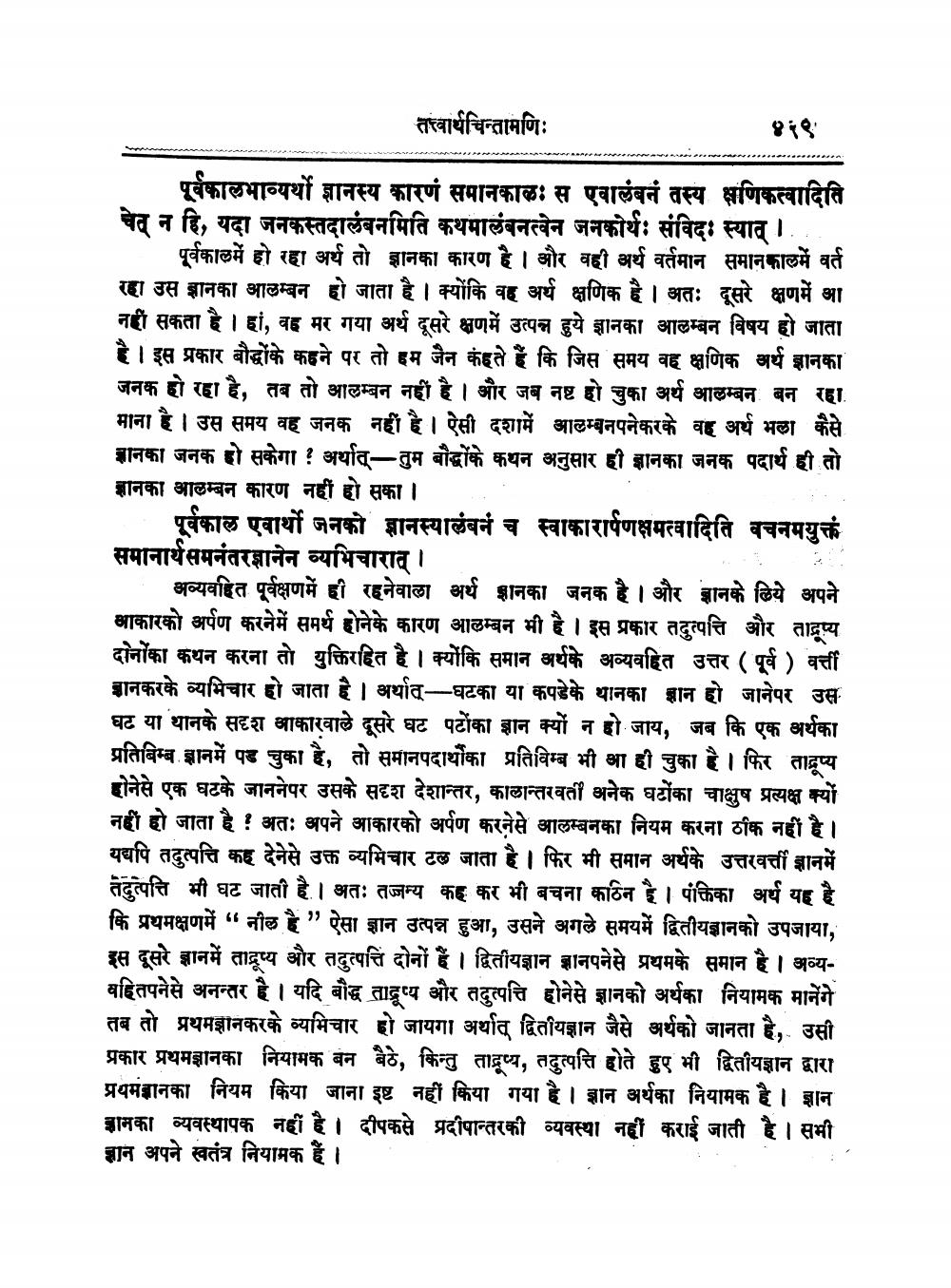________________
तत्त्वार्थचिन्तामणिः
४९९
I
पूर्वकालभाव्यर्थी ज्ञानस्य कारणं समानकालः स एवालंबनं तस्य क्षणिकत्वादिति चेत् न हि यदा जनकस्तदा लंबनमिति कथमालंबनत्वेन जनकोर्थः संविदः स्यात् । पूर्वकालमें हो रहा अर्थ तो ज्ञानका कारण है । और वही अर्थ वर्तमान समानकाल में वर्त I रहा उस ज्ञानका आलम्बन हो जाता है । क्योंकि वह अर्थ क्षणिक है । अतः दूसरे क्षणमें आ नहीं सकता है। हां, वह मर गया अर्थ दूसरे क्षण में उत्पन्न हुये ज्ञानका आलम्बन विषय हो जाता है । इस प्रकार बौद्धोंके कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि जिस समय वह क्षणिक अर्थ ज्ञानका जनक हो रहा है, तब तो आलम्बन नहीं है । और जब नष्ट हो चुका अर्थ आलम्बन बन रहा माना है । उस समय वह जनक नहीं है। ऐसी दशामें आलम्बनपनेकरके वह अर्थ भला कैसे ज्ञानका जनक हो सकेगा ? अर्थात् - तुम बौद्धोंके कथन अनुसार ही ज्ञानका जनक पदार्थ ही तो ज्ञानका आलम्बन कारण नहीं हो सका ।
पूर्वकाल एवार्थो जनको ज्ञानस्यालंबनं च स्वाकारार्पणक्षमत्वादिति वचनमयुक्तं समानार्थसमनंतरज्ञानेन व्यभिचारात् ।
अव्यवहित पूर्वक्षण में ही रहनेवाला अर्थ ज्ञानका जनक है । और ज्ञानके लिये अपने आकारको अर्पण करनेमें समर्थ होनेके कारण आलम्बन भी है । इस प्रकार तदुत्पत्ति और ताद्रूप्य दोनोंका कथन करना तो युक्तिरहित है। क्योंकि समान अर्थके अव्यवहित उत्तर ( पूर्व ) वर्त्ती ज्ञानकरके व्यभिचार हो जाता है । अर्थात्- - घटका या कपडेके थानका ज्ञान हो जानेपर उस घट या थानके सदृश आकारवाले दूसरे घट पटोंका ज्ञान क्यों न हो जाय, जब कि एक अर्थका प्रतिबिम्ब ज्ञानमें पड चुका है, तो समानपदार्थोंका प्रतिविम्ब भी आ ही चुका है । फिर ताद्रूप्य होनेसे एक घटके जाननेपर उसके सदृश देशान्तर, कालान्तरवर्ती अनेक घटोंका चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो जाता है ? अतः अपने आकारको अर्पण करनेसे आलम्बनका नियम करना ठीक नहीं है । यद्यपि तदुत्पत्ति कह देनेसे उक्त व्यभिचार टल जाता है। फिर भी समान अर्थके उत्तरवर्त्ती ज्ञानमें तेदुत्पत्ति भी घट जाती है । अतः तज्जन्य कह कर भी बचना कठिन है । पंक्तिका अर्थ यह है कि प्रथमक्षण में " नील हैं " ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसने अगले समय में द्वितीयज्ञानको उपजाया, इस दूसरे ज्ञानमें ताद्रूप्य और तदुत्पत्ति दोनों हैं । द्वितीयज्ञान ज्ञानपनेसे प्रथमके समान है । अव्यवहितपनेसे अनन्तर है । यदि बौद्ध ताद्रूष्य और तदुत्पत्ति होनेसे ज्ञानको अर्थका नियामक मानेंगे तब तो प्रथमज्ञानकर के व्यभिचार हो जायगा अर्थात् द्वितीयज्ञान जैसे अर्थको जानता है, उसी प्रकार प्रथमज्ञानका नियामक बन बैठे, किन्तु ताद्रूष्य, तदुत्पत्ति होते हुए भी द्वितीयज्ञान द्वारा प्रथमंज्ञानका नियम किया जाना इष्ट नहीं किया गया है। ज्ञान अर्थका नियामक है । ज्ञान ज्ञानका व्यवस्थापक नहीं है । दीपकसे प्रदीपान्तरकी व्यवस्था नहीं कराई जाती है। सभी ज्ञान अपने स्वतंत्र नियामक हैं ।
1