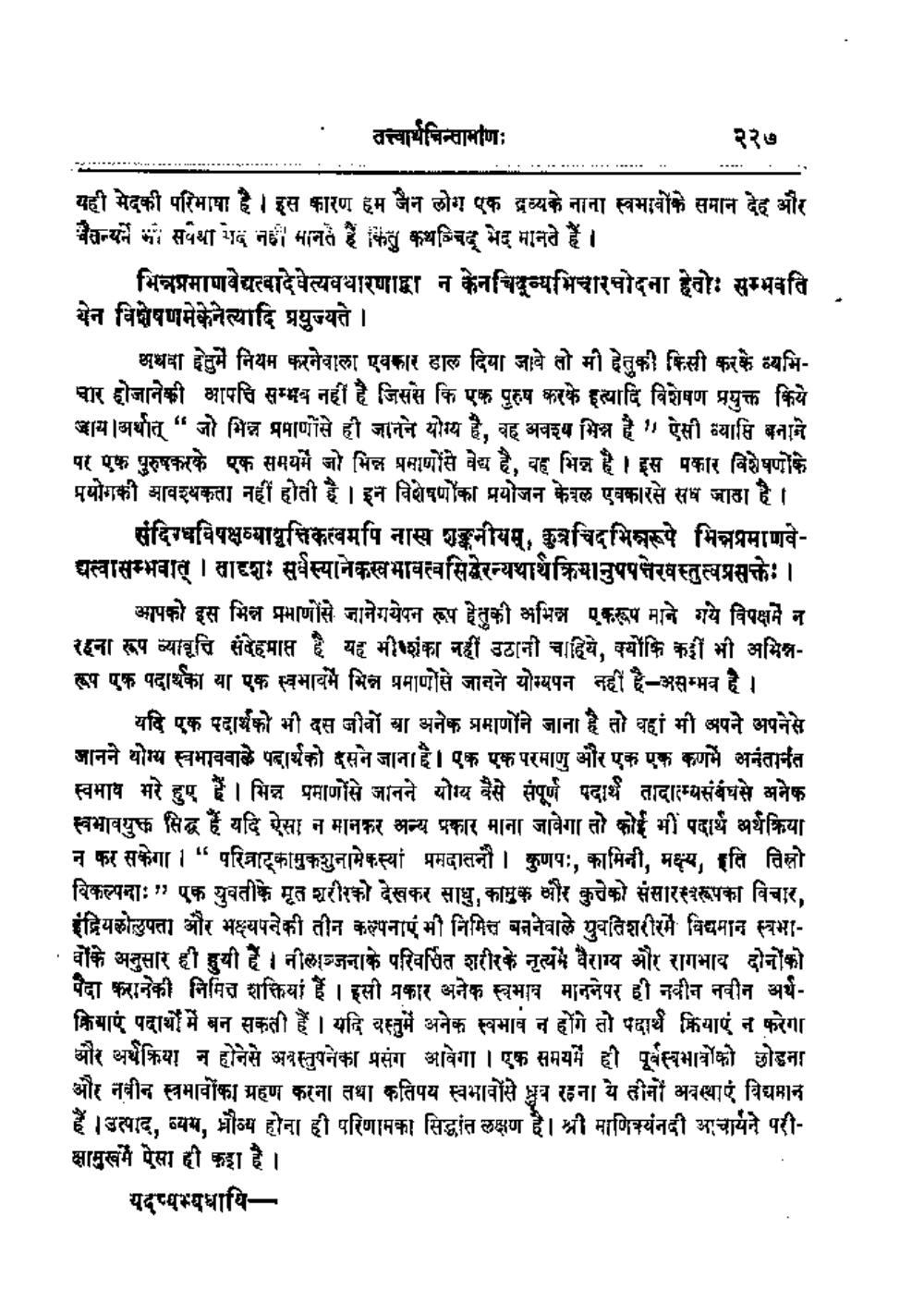________________
- तत्त्वार्थचिन्तामणिः
२२७
यही मेदकी परिभाषा है । इस कारण हम जैन लोग एक द्रव्यके नाना स्वभावोंके समान देह और चैतन्यर्ने भो सर्वथा भेद नही मानते हैं किंतु कथञ्चिद् भेद मानते हैं।
भिन्नप्रमाणवेद्यत्वादेधेत्यवधारणाद्वा न केनचिदन्यभिचारचोदना हेतोः सम्भवति , येन विशेषणमेकेनेत्यादि प्रयुज्यते ।
अथवा इतुमे नियम करनेवाला एवकार डाल दिया जाये तो मी देतुकी किसी करके व्यभिचार होजानेकी आपत्ति सम्भव नहीं है जिससे कि एक पुरुष करके इत्यादि विशेषण प्रयुक्त किये जाय।अर्थात् " जो भिन्न प्रमाणोंसे ही जानने योग्य है, वह अवश्य भिन्न है ।" ऐसी व्याप्ति बनाने पर एक पुरुषकरके एक समयमै जो भिन्न प्रमाणोंसे वेद्य है, वह भिन्न है । इस प्रकार विशेषणों के प्रयोगकी आवश्यकता नहीं होती है । इन विशेषणोंका प्रयोजन केवल एवकारसे सब जाठा है।
संदिग्धविषक्षव्यावृत्तिकत्वमपि नास्य शङ्कनीयम्, कुत्रचिदभिन्नरूपे भिन्नप्रमाणवेचत्वासम्भवात् । सादृशः सर्वस्यानेकखभावत्वसिबेरन्यथार्थक्रियानुपपत्तेरवस्तुवप्रसक्तेः।
आपको इस भिन्न प्रमाणोंसे जानेगयेपन रूप हेतुकी अभिन्न एकरूप माने गये विपक्षमें न रहना रूप ब्यावृत्ति संदेहमाप्त है यह भीशंका नहीं उठानी चाहिये, क्योंकि कहीं भी अभिन्नरूप एक पदार्थका या एक स्वभावमै भिन्न प्रमाणोसे जानने योग्यपन नहीं है-असम्भव है।
___ यदि एक पदार्थको भी दस जीवों या अनेक प्रमाणोंने जाना है तो वहां भी अपने अपनेसे जानने योग्य स्वभाववाले पदार्थको इसने जाना है। एक एक परमाणु और एक एक कण, अनंतानंत स्वभाव भरे हुए हैं। भिन्न प्रमाणोंसे जानने योग्य वैसे संपूर्ण पदार्थ तादात्म्यसंबंघसे अनेक स्वभावयुक्त सिद्ध हैं यदि ऐसा न मानकर अन्य प्रकार माना जावेगा तो कोई भी पदार्थ अर्थक्रिया न कर सकेगा । “ परित्राट्कामुकशुनामेकस्यां प्रमदातनौ । कुणपः, कामिनी, मक्ष्य, इति तिस्रो विकल्पनाः" एक युवतीके मृत शरीरको देखकर साधु, कामुक और कुत्तेको संसारस्वरूपका विचार, इंद्रियलोलुपता और भक्ष्यपनेकी तीन कल्पनाएं भी निमित्त बननेवाले युवतिशरीरमै विद्यमान स्वभावोंके अनुसार ही हुयी हैं। नीलाञ्जनाके परिवर्तित शरीरके नृत्य वैराग्य और रागभाव दोनोंको पैदा करानेकी निमित्त शक्तियां हैं । इसी प्रकार अनेक स्वभाव माननेपर ही नवीन नवीन अर्थक्रियाएं पदार्थों में बन सकती हैं। यदि वस्तुमें अनेक स्वभाव न होंगे तो पदार्थ क्रियाएं न करेगा और अर्थक्रिया न होनेसे अवस्तुपनेका प्रसंग आवेगा । एक समयमें ही पूर्वस्वभावोंको छोड़ना और नवीन स्वभावोंका ग्रहण करना तथा कतिपय स्वभावोंसे ध्रुव रहना ये तीनों अवस्थाएं विद्यमान हैं । उत्पाद, व्यय, भौव्य होना ही परिणामका सिद्धांत लक्षण है। श्री माणिक्यनदी आचार्य ने परीक्षामुखमें ऐसा ही कहा है।
यदप्यभ्यधायि